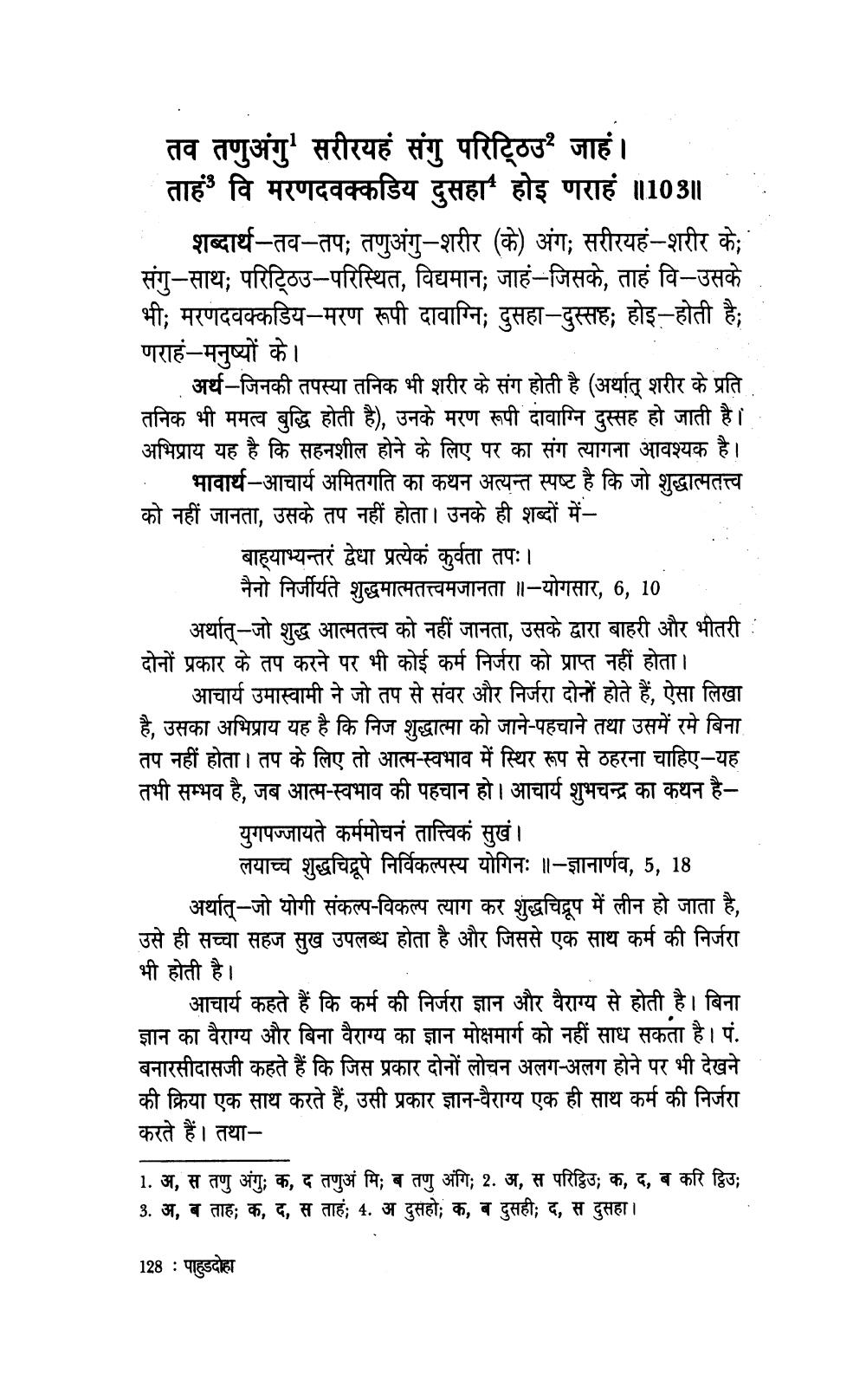________________
तव तणुअंगु सरीरयहं संगु परिट्ठिउ' जाहं । ताह वि मरणदवक्कडिय दुसहा - होइ णराहं ॥10॥
शब्दार्थ-तव-तप; तणुअंगु - शरीर (के) अंग; सरीरयहं - शरीर के; संगु - साथ; परिट्ठिउ-परिस्थित, विद्यमान; जाहं - जिसके , ताहं वि - उसके भी; मरणदवक्कडिय–मरण रूपी दावाग्नि; दुसहा - दुस्सह; होइ - होती है; णराहं - मनुष्यों के ।
अर्थ-जिनकी तपस्या तनिक भी शरीर के संग होती है (अर्थात् शरीर के प्रति तनिक भी ममत्व बुद्धि होती है), उनके मरण रूपी दावाग्नि दुस्सह हो जाती है। अभिप्राय यह है कि सहनशील होने के लिए पर का संग त्यागना आवश्यक है भावार्थ-आचार्य अमितगति का कथन अत्यन्त स्पष्ट है कि जो शुद्धात्मतत्त्व को नहीं जानता, उसके तप नहीं होता। उनके ही शब्दों में
1
बाह्याभ्यन्तरं द्वेधा प्रत्येकं कुर्वता तपः ।
नैनो निर्जीर्यते शुद्धमात्मतत्त्वमजानता ॥ - योगसार, 6, 10 अर्थात् - जो शुद्ध आत्मतत्त्व को नहीं जानता, उसके द्वारा बाहरी और भीतरी : दोनों प्रकार के तप करने पर भी कोई कर्म निर्जरा को प्राप्त नहीं होता ।
आचार्य उमास्वामी ने जो तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं, ऐसा लिखा है, उसका अभिप्राय यह है कि निज शुद्धात्मा को जाने-पहचाने तथा उसमें रमे बिना तप नहीं होता । तप के लिए तो आत्म-स्वभाव में स्थिर रूप से ठहरना चाहिए - यह तभी सम्भव है, जब आत्म-स्वभाव की पहचान हो । आचार्य शुभचन्द्र का कथन है
युगपज्जायते कर्ममोचनं तात्त्विकं सुखं ।
लयाच्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः ॥ - ज्ञानार्णव, 5, 18
अर्थात्-जो योगी संकल्प-विकल्प त्याग कर शुद्धचिद्रूप में लीन हो जाता है, उसे ही सच्चा सहज सुख उपलब्ध होता है और जिससे एक साथ कर्म की निर्जरा भी होती है ।
आचार्य कहते हैं कि कर्म की निर्जरा ज्ञान और वैराग्य से होती है। बिना ज्ञान का वैराग्य और बिना वैराग्य का ज्ञान मोक्षमार्ग को नहीं साध सकता है। पं. बनारसीदासजी कहते हैं कि जिस प्रकार दोनों लोचन अलग-अलग होने पर भी देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान-वैराग्य एक ही साथ कर्म की निर्जरा करते हैं। तथा
1. अ, स तणु अंगु; क, द तणुअं मि; ब तणु अंगि; 2. अ, स परिट्ठिउ; क, द, ब करि ट्ठिउ; 3. अ, ब ताह; क, द, स ताहं 4. अ दुसहो; क, ब दुसही; द, स दुसहा ।
128: पाहुडदोहा