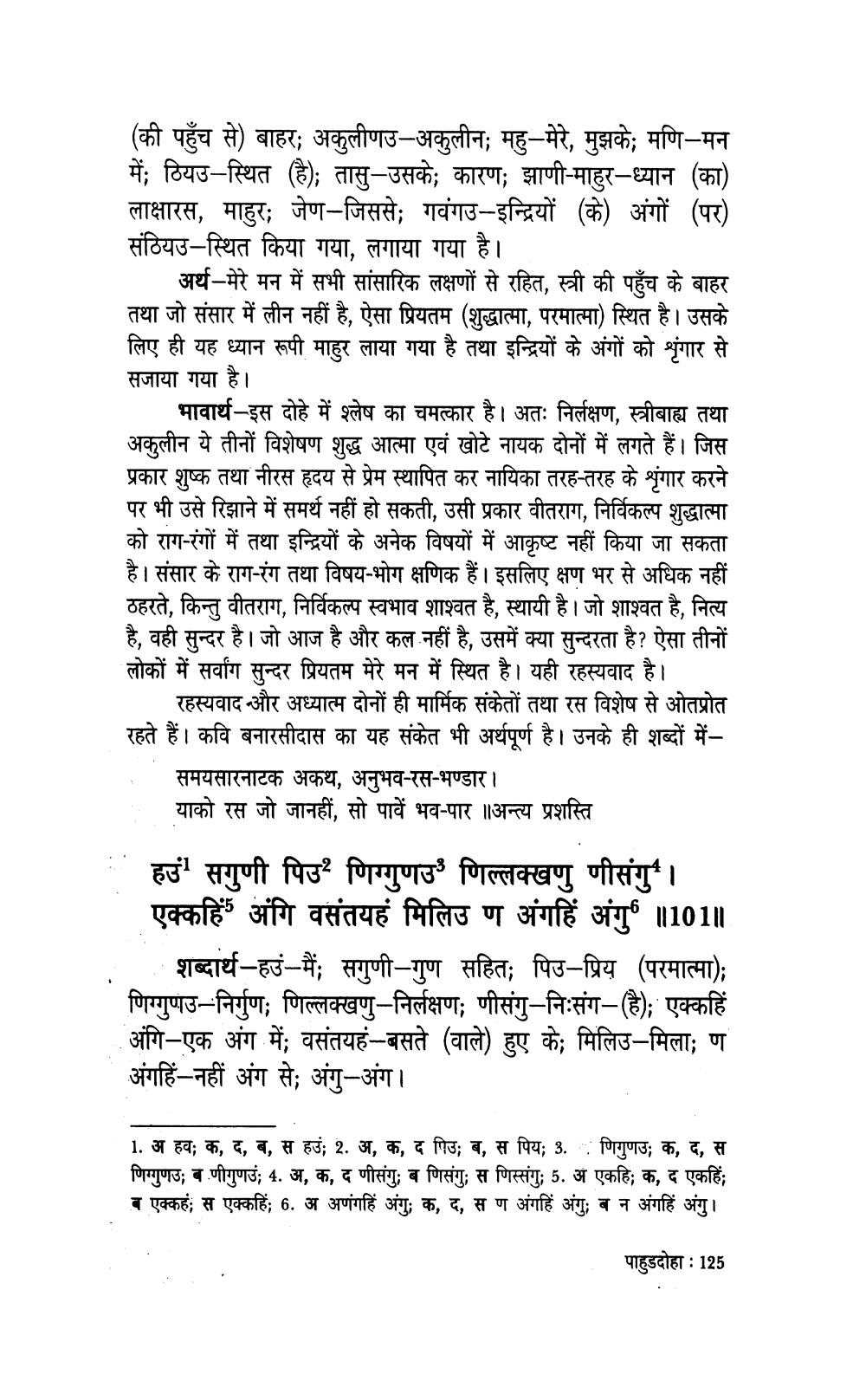________________
(की पहुँच से) बाहर; अकुलीणउ-अकुलीन; महु-मेरे, मुझके; मणि-मन में; ठियउ-स्थित (है); तासु-उसके; कारण; झाणी-माहुर-ध्यान (का) लाक्षारस, माहर; जेण-जिससे; गवंगउ-इन्द्रियों (के) अंगों (पर) संठियउ-स्थित किया गया, लगाया गया है।
अर्थ-मेरे मन में सभी सांसारिक लक्षणों से रहित, स्त्री की पहुँच के बाहर तथा जो संसार में लीन नहीं है, ऐसा प्रियतम (शुद्धात्मा, परमात्मा) स्थित है। उसके लिए ही यह ध्यान रूपी माहुर लाया गया है तथा इन्द्रियों के अंगों को शृंगार से सजाया गया है।
भावार्थ-इस दोहे में श्लेष का चमत्कार है। अतः निर्लक्षण, स्त्रीबाह्य तथा अकुलीन ये तीनों विशेषण शुद्ध आत्मा एवं खोटे नायक दोनों में लगते हैं। जिस प्रकार शुष्क तथा नीरस हृदय से प्रेम स्थापित कर नायिका तरह-तरह के शृंगार करने पर भी उसे रिझाने में समर्थ नहीं हो सकती, उसी प्रकार वीतराग, निर्विकल्प शुद्धात्मा को राग-रंगों में तथा इन्द्रियों के अनेक विषयों में आकृष्ट नहीं किया जा सकता है। संसार के राग-रंग तथा विषय-भोग क्षणिक हैं। इसलिए क्षण भर से अधिक नहीं ठहरते, किन्तु वीतराग, निर्विकल्प स्वभाव शाश्वत है, स्थायी है। जो शाश्वत है, नित्य है, वही सुन्दर है। जो आज है और कल नहीं है, उसमें क्या सुन्दरता है? ऐसा तीनों लोकों में सर्वांग सुन्दर प्रियतम मेरे मन में स्थित है। यही रहस्यवाद है।
रहस्यवाद और अध्यात्म दोनों ही मार्मिक संकेतों तथा रस विशेष से ओतप्रोत रहते हैं। कवि बनारसीदास का यह संकेत भी अर्थपूर्ण है। उनके ही शब्दों में
समयसारनाटक अकथ, अनुभव-रस-भण्डार। याको रस जो जानहीं, सो पावें भव-पार ॥अन्त्य प्रशस्ति
हउं' सगुणी पिउ' णिगुणउ णिल्लक्खणु णीसंगु । एक्कहिँ अंगि वसंतयहं मिलिउ ण अंगहिं अंगु ॥1010
शब्दार्थ-हउं-मैं; सगुणी-गुण सहित; पिउ-प्रिय (परमात्मा); णिग्गुणउ-निर्गुण; णिल्लक्खणु-निर्लक्षण; णीसंगु-निःसंग-(है); एक्कहिं अंगि-एक अंग में; वसंतयहं-बसते (वाले) हुए के; मिलिउ-मिला; ण अंगहिं-नहीं अंग से; अंगु-अंग।
1. अ हव; क, द, ब, स हउं; 2. अ, क, द पिउ; ब, स पिय; 3. . णिगुणउ; क, द, स णिग्गुणउ; ब णीगुणउं; 4. अ, क, द णीसंगु; ब णिसंगु; स णिस्संगु; 5. अ एकहि; क, द एकहिं; ब एक्कह; स एक्कहिं; 6. अ अणंगहिं अंगु, क, द, स ण अंगहिं अंगु; ब न अंगहिं अंगु।
पाहुडदोहा : 125