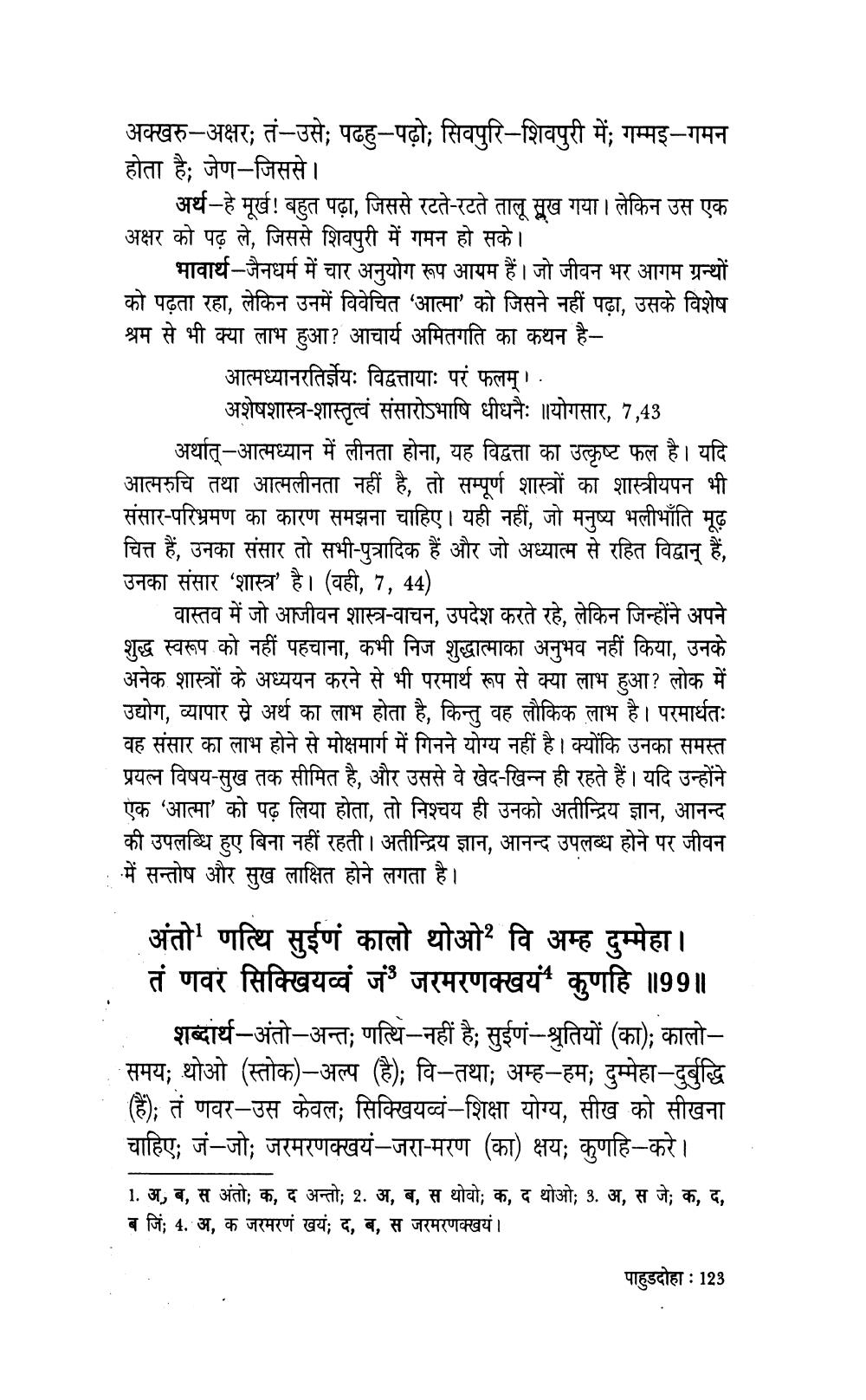________________
अक्खरु-अक्षर; तं-उसे; पढहु-पढ़ो; सिवपुरि-शिवपुरी में; गम्मइ-गमन होता है; जेण-जिससे।
अर्थ-हे मूर्ख! बहुत पढ़ा, जिससे रटते-रटते तालू सूख गया। लेकिन उस एक अक्षर को पढ़ ले, जिससे शिवपुरी में गमन हो सके।
भावार्थ-जैनधर्म में चार अनुयोग रूप आयम हैं। जो जीवन भर आगम ग्रन्थों को पढ़ता रहा, लेकिन उनमें विवेचित 'आत्मा' को जिसने नहीं पढ़ा, उसके विशेष श्रम से भी क्या लाभ हुआ? आचार्य अमितगति का कथन है
आत्मध्यानरतिज्ञेयः विद्वत्तायाः परं फलम्। .
अशेषशास्त्र-शास्तृत्वं संसारोऽभाषि धीधनैः ॥योगसार, 7,43 अर्थात्-आत्मध्यान में लीनता होना, यह विद्वत्ता का उत्कृष्ट फल है। यदि आत्मरुचि तथा आत्मलीनता नहीं है, तो सम्पूर्ण शास्त्रों का शास्त्रीयपन भी संसार-परिभ्रमण का कारण समझना चाहिए। यही नहीं, जो मनुष्य भलीभाँति मूढ़ चित्त हैं, उनका संसार तो सभी-पुत्रादिक हैं और जो अध्यात्म से रहित विद्वान् हैं, उनका संसार 'शास्त्र' है। (वही, 7, 44)
___ वास्तव में जो आजीवन शास्त्र-वाचन, उपदेश करते रहे, लेकिन जिन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचाना, कभी निज शुद्धात्माका अनुभव नहीं किया, उनके अनेक शास्त्रों के अध्ययन करने से भी परमार्थ रूप से क्या लाभ हुआ? लोक में उद्योग, व्यापार से अर्थ का लाभ होता है, किन्तु वह लौकिक लाभ है। परमार्थतः वह संसार का लाभ होने से मोक्षमार्ग में गिनने योग्य नहीं है। क्योंकि उनका समस्त प्रयत्न विषय-सुख तक सीमित है, और उससे वे खेद-खिन्न ही रहते हैं। यदि उन्होंने एक 'आत्मा' को पढ़ लिया होता, तो निश्चय ही उनको अतीन्द्रिय ज्ञान, आनन्द की उपलब्धि हुए बिना नहीं रहती। अतीन्द्रिय ज्ञान, आनन्द उपलब्ध होने पर जीवन में सन्तोष और सुख लाक्षित होने लगता है।
अंतो' णत्थि सुईणं कालो थोओ वि अम्ह दुम्मेहा। तं णवर सिक्खियव्वं जं जरमरणखयं कुणहि ॥99॥
शब्दार्थ-अंतो-अन्त; णत्थि-नहीं है; सुईणं-श्रुतियों (का); कालोसमय; थोओ (स्तोक)-अल्प (है); वि-तथा; अम्ह-हम; दुम्मेहा-दुर्बुद्धि (हैं); तं णवर-उस केवल; सिक्खियव्वं-शिक्षा योग्य, सीख को सीखना चाहिए; जं-जो; जरमरणक्खयं-जरा-मरण (का) क्षय; कुणहि-करे। 1. अ, ब, स अंतो; क, द अन्तो; 2. अ, ब, स थोवो; क, द थोओ; 3. अ, स जे; क, द, ब जिं; 4. अ, क जरमरणं खयं द, ब, स जरमरणक्खयं।
पाहुडदोहा : 123