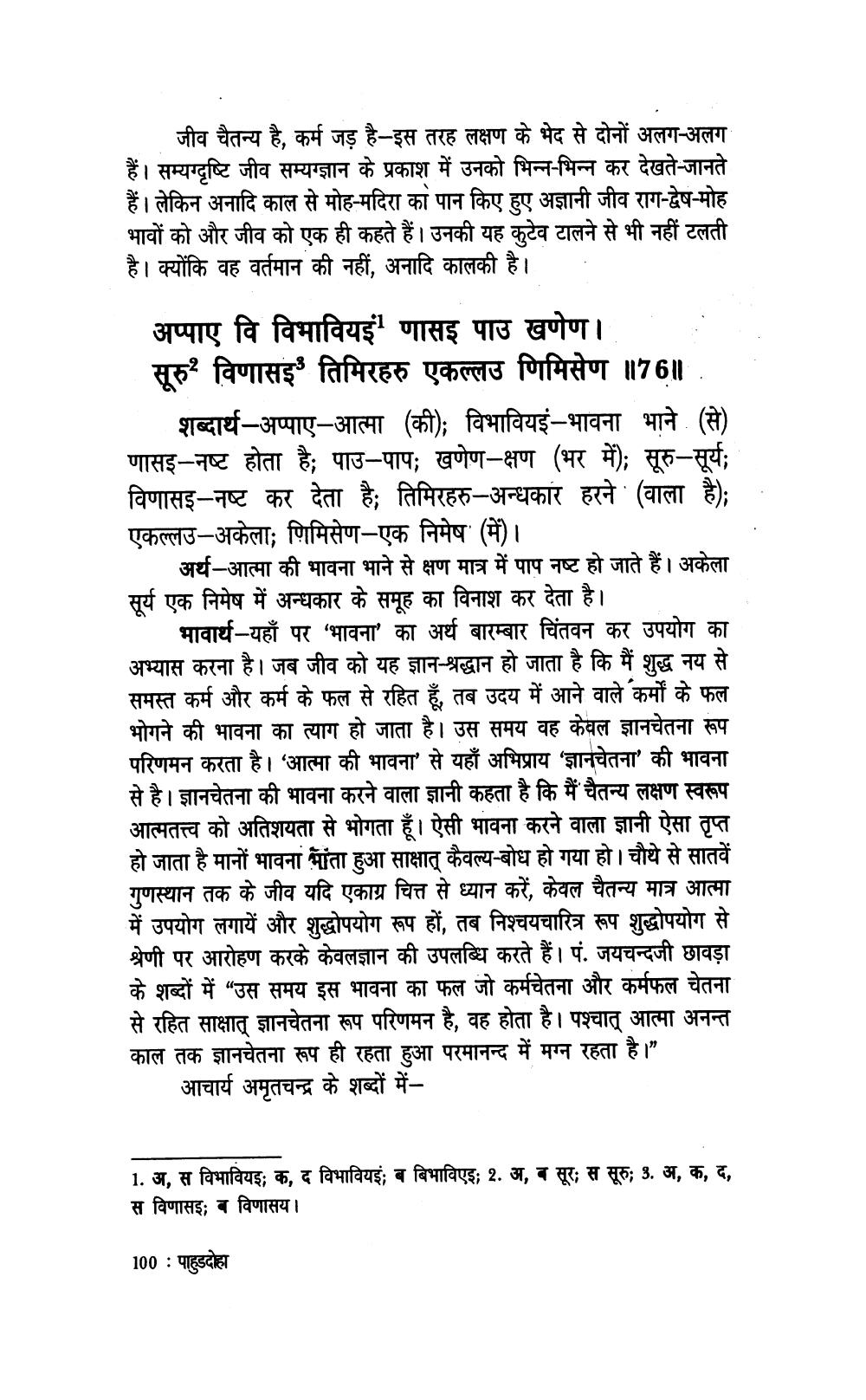________________
जीव चैतन्य है, कर्म जड़ है-इस तरह लक्षण के भेद से दोनों अलग-अलग हैं। सम्यग्दृष्टि जीव सम्यग्ज्ञान के प्रकाश में उनको भिन्न-भिन्न कर देखते-जानते हैं। लेकिन अनादि काल से मोह-मदिरा का पान किए हुए अज्ञानी जीव राग-द्वेष-मोह भावों को और जीव को एक ही कहते हैं। उनकी यह कुटेव टालने से भी नहीं टलती है। क्योंकि वह वर्तमान की नहीं, अनादि कालकी है।
अप्पाए वि विभावियई णासइ पाउ खणेण। सूरु विणासई तिमिरहरु एकल्लउ णिमिसेण ॥76॥ .
शब्दार्थ-अप्पाए-आत्मा (की); विभावियइं-भावना भाने (से) णासइ-नष्ट होता है; पाउ-पाप; खणेण-क्षण (भर में); सूरु-सूर्य विणासइ-नष्ट कर देता है; तिमिरहरु-अन्धकार हरने (वाला है); एकल्लउ-अकेला; णिमिसेण-एक निमेष (में)।
अर्थ-आत्मा की भावना भाने से क्षण मात्र में पाप नष्ट हो जाते हैं। अकेला सूर्य एक निमेष में अन्धकार के समूह का विनाश कर देता है।
भावार्थ-यहाँ पर 'भावना' का अर्थ बारम्बार चितवन कर उपयोग का अभ्यास करना है। जब जीव को यह ज्ञान-श्रद्धान हो जाता है कि मैं शुद्ध नय से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ, तब उदय में आने वाले कर्मों के फल भोगने की भावना का त्याग हो जाता है। उस समय वह केवल ज्ञानचेतना रूप परिणमन करता है। ‘आत्मा की भावना' से यहाँ अभिप्राय 'ज्ञानचेतना' की भावना से है। ज्ञानचेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि मैं चैतन्य लक्षण स्वरूप आत्मतत्त्व को अतिशयता से भोगता हूँ। ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हो जाता है मानों भावना माता हुआ साक्षात् कैवल्य-बोध हो गया हो। चौथे से सातवें गुणस्थान तक के जीव यदि एकाग्र चित्त से ध्यान करें, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगायें और शुद्धोपयोग रूप हों, तब निश्चयचारित्र रूप शुद्धोपयोग से श्रेणी पर आरोहण करके केवलज्ञान की उपलब्धि करते हैं। पं. जयचन्दजी छावड़ा के शब्दों में “उस समय इस भावना का फल जो कर्मचेतना और कर्मफल चेतना से रहित साक्षात् ज्ञानचेतना रूप परिणमन है, वह होता है। पश्चात् आत्मा अनन्त काल तक ज्ञानचेतना रूप ही रहता हुआ परमानन्द में मग्न रहता है।"
आचार्य अमृतचन्द्र के शब्दों में
1. अ, स विभावियइ क, द विभावियइं; ब बिभाविएइ; 2. अ, ब सूर; स सूरु; 3. अ, क, द, स विणासइ व विणासय।
100 : पाहुडदोहा