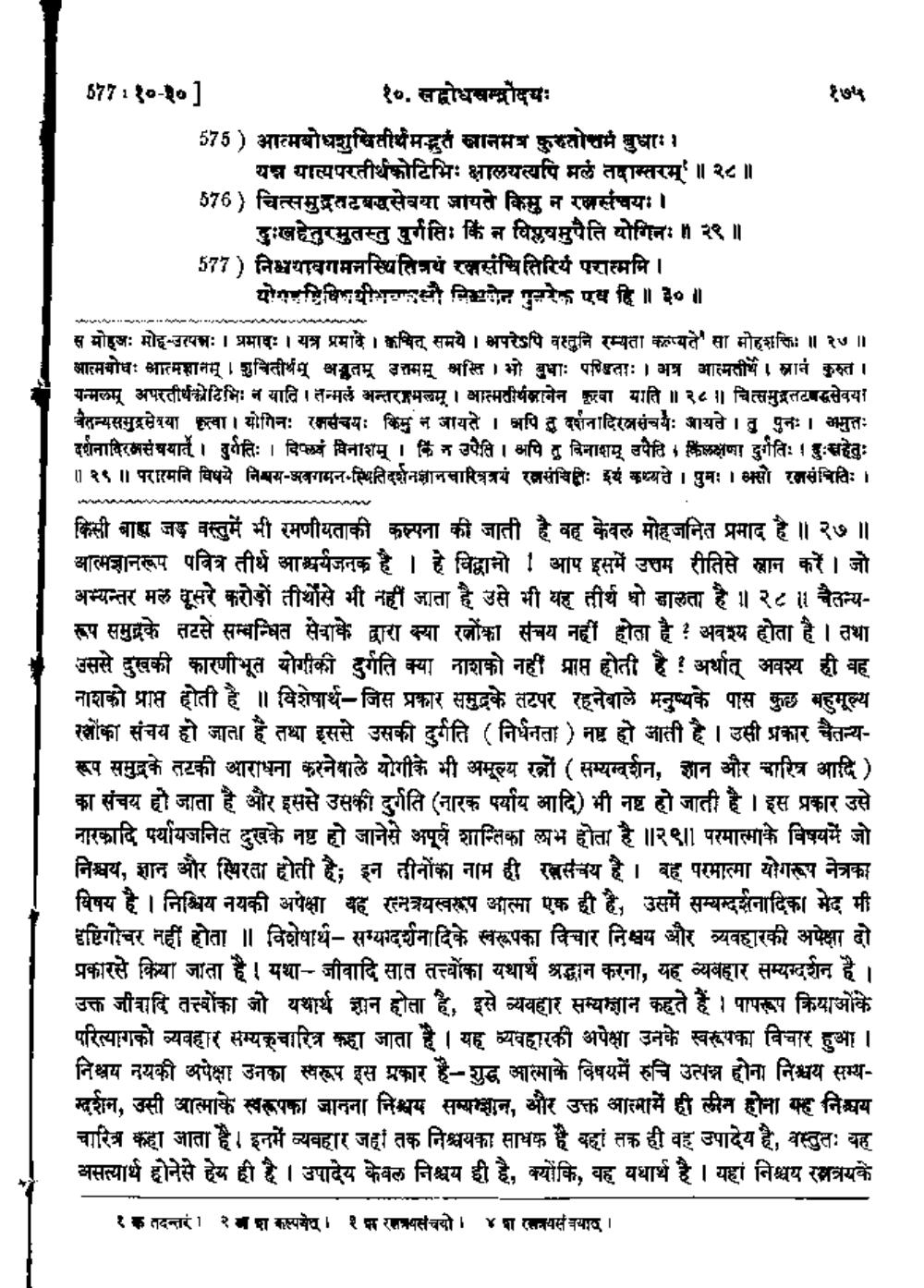________________
5771 १०-३०] १०. सद्बोधचन्द्रोदयः
१७५ 575) आत्मबोधशुधिसीर्थमद्धत मानमत्र कुस्तोत्तम बुधाः।
यन्न यात्यपरतीर्थकोटिभिः क्षालयत्यपि मलं तदातरम् ॥ २८ ॥ 576) चित्समुद्रतटबरसेवया जायते किमु न रखसंचयः।
दुलहेतुरमुतस्तु पुर्गतिः किं न विप्लवमुपैति योगिनः ॥ २९ ॥ 577) निधयावगमनस्थितित्रयं रखसंचितिरिय परात्ममि ।
योग विधियीभौ लिभोन गुहारेक एव हि ॥ ३०॥ समोइजः मोद-उस्पनः । प्रमावः। यत्र प्रमादे। कश्चित् समये। अपरेऽपि वस्तुनि रम्यता कप्यतेसा मोहशक्तिः ॥ २७ ॥ आत्मबोध: आत्मज्ञानम् । शुचितीर्थम् अवतम् उत्तमम् अस्ति । भो बुधाः पखिताः । अत्र आत्मतीर्थ । खान कुरुत । यन्मलम् अपरतीर्थकोटिभिः न याति । तन्मलं अन्तरामलम् । आत्मतीर्थमानेन कृत्वा याति ॥ २८ ॥ चित्समुद्रतटबद्धसेवया चैतन्यसमुद्रसेवया कृत्वा । योगिनः रमसंचयः किमुन जायते । अपितु दर्शनादिरश्नसंचयः आयते । तु पुनः । अतः दर्शनाविरमर्सषया । दुर्गतिः । विफल बिनाशम् । किन उपैति । अपितु विनाशम् उपैति । किंलक्षणा दुर्गतिः । दुःसहेतुः ॥ २९ ॥ परारमनि विषये निवय-अवगमन-स्थितिदर्शनज्ञानमारित्रत्रयं रनसंचितिः इयं कथ्यते । पुमः । असो रजसंचितिः ।
किसी बाह्य जड वस्तुमें भी रमणीयताकी कल्पना की जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥ आत्मज्ञानरूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है । हे विद्वानो ! आप इसमें उत्तम रीतिसे मान करें। जो अभ्यन्तर मल दूसरे करोड़ों तीर्थोसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीर्थ धो डालता है ॥ २८ ॥ चैतन्यरूप समुद्रके तटसे सम्बन्धित सेवाके द्वारा क्या रत्नोंका संचय नहीं होता है ? अवश्य होता है । तथा उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशको नहीं प्राप्त होती है ! अर्थात् अवश्य ही वह नाशको प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमूल्य स्तोका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गति (निर्धनता ) नष्ट हो जाती है । उसी प्रकार चैतन्यरूप समुद्र के तटकी आराधना करनेवाले योगीके भी अमूल्य रनों (सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि) का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुर्गति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उसे नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्तिका लाभ होता है ॥२९|| परमात्माके विषयमें जो निश्चय, शान और स्थिरता होती है। इन तीनोंका नाम ही रखसंचय है। वह परमात्मा योगरूप नेत्रका विषय है । निश्चिय नयकी अपेक्षा यह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यग्दर्शनादिका मेद मी दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ- सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपका विचार निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो प्रकारसे किया जाता है । यथा- जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यग्दर्शन है। उक्त जीवादि तत्वोंका जो यथार्थ ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यज्ञान कहते हैं। पापरूप क्रियाओंके परित्यागको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जाता है । यह व्यवहारकी अपेक्षा उनके स्वरूपका विचार हुआ । निश्चय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है-शुद्ध आत्माके विषयमें रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्यदर्शन, उसी आत्माके स्वरूपका जानना निश्चय सम्पमान, और उक्त आत्मामें ही लीन होना यह निश्चय चारित्र कहा जाता है। इनमें व्यवहार जहाँ तक निश्चयका साधक है वहां तक ही वह उपादेय है, वस्तुतः यह असत्यार्थ होनेसे हेय ही है । उपादेय केवल निश्चय ही है, क्योंकि, वह यथार्थ है । यहां निश्चय रखत्रयके
एक तदन्तरं । २मशकल्पयेत् ।
करसत्रयसंचयो। ४ा सत्यसंचयाव ।