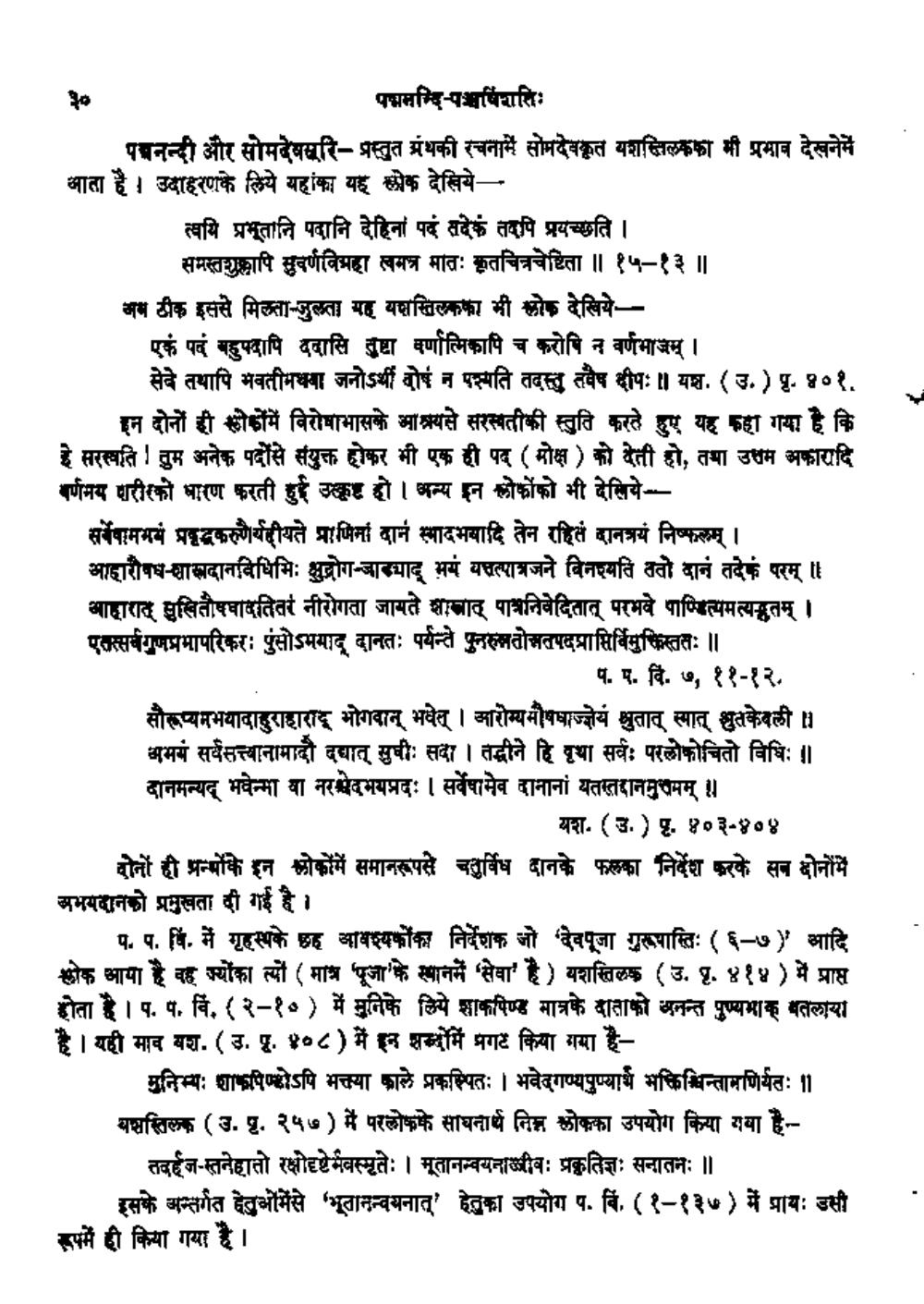________________
पद्ममन्दि- पञ्चविंशतिः
पचनन्दी और सोमदेवसूरि प्रस्तुत ग्रंथकी रचनायें सोमदेवकृत यशस्तिलकका भी प्रभाव देखने में आता है । उदाहरण के लिये यहांका यह लोक देखिये --
*
त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं सदेकं तदपि प्रयच्छति । समस्तशुक्लापि सुवर्णवित्रा त्वमत्र मातः कृतचित्रचेष्टिता ॥ १५-१३ ॥
are ठीक इससे मिलता-जुलता यह यशस्तिलकका भी लोक देखिये-
एकं पदं बहुपदापि ददासि तुष्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न वर्णभाजम् ।
सेवे तथापि भवतीमथवा जनोऽर्थी दोषं न पश्यति तदस्तु तवैष दीपः ॥ यश. ( उ. ) पृ. ४०१.
इन दोनों ही कोकोंमें विरोधाभासके आश्रयसे सरस्वतीकी स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि हे सरस्वति ! तुम अनेक पदोंसे संयुक्त होकर भी एक ही पद (मोक्ष) को देती हो, तथा उधम अकारादि वर्णमय शरीरको धारण करती हुई उत्कृष्ट हो । अन्य इन लोकोंको भी देखिये
सर्वेषामभयं प्रवृद्धकरुणैर्यद्दीयते प्राणिनां दानं स्यादभयादि तेन रहितं दानत्रयं निष्फलम् । आहारौवध शास्त्रदानविधिभिः क्षुद्रोग-जायाद् भयं यत्पात्रजने विनश्यति ततो दानं तदेकं परम् ॥ आहाराट् सुखितौषवादतितरं नीरोगता जायते शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परभवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम् । एतत्सर्वगुणप्रभापरिकरः पुंसोऽभयाद् दानतः पर्यन्ते पुनरुन तो अतपदप्राप्तिर्विमुक्तिस्ततः ॥
प. प. विं.
११-१२.
सौरूप्यमभयादाहुराहाराद् भोगवान् भवेत् । आरोग्यमौषधाज्ज्ञेयं श्रुतात् स्यात् श्रुतकेबली ॥ अभयं सर्वसत्त्वानामादौ दद्यात् सुधीः सदा । तद्धीने हि वृथा सर्वः परलोकोचितो विधिः । दानमन्यद् भवेन्मा वा नरश्वेदभयप्रदः । सर्वेषामेव दानानां यतस्तद्दानमुत्तमम् ॥
ܘ
यश. ( उ ) पृ. ४०३-४०४ दोनों ही अन्योंके इन लोकोंमें समानरूपसे चतुर्विध दानके फलका निर्देश करके सब दोनों में अभयदानको प्रमुखता दी गई है।
प.प. वि. में गृहस्थके छह आवश्यकका निर्देशक जो 'देवपूजा गुरूपास्तिः ( ६-७ )' आदि श्लोक आया है वह ज्योंका त्यों (मात्र 'पूजा' के स्थानमें 'सेवा' है) यशस्तिलक (उ. प्र. ४१४ ) में प्राप्त होता है । प. प. विं. (२ - १० ) में सुनिके लिये शाकपिण्ड मात्रके दाताको अनन्त पुण्यभाक् बतलाया है। यही मान यश. ( उ. पू. ४०८) में इन शब्दोंमें प्रगट किया गया है
मुनिभ्यः शाकपिण्डोऽपि भक्त्या काले प्रकल्पितः । भवेद्गण्यपुण्यार्थे भक्तिश्चिन्तामणिर्यतः || यशस्तिलक (उ. पृ. २५७) में परलोकके साघनार्थ निम्न लोकका उपयोग किया गया है
तदर्हज-स्तनेहातो रक्षोदृष्टेर्भवस्मृतेः । मूतानन्वयनाञ्जीवः प्रकृतिज्ञः सनातनः ॥
इसके अन्तर्गत हेतुओंमेंसे 'भूतानन्वयनात्' हेतुका उपयोग प. विं. (१ - १३७ ) में प्रायः उसी रूपमें ही किया गया है।