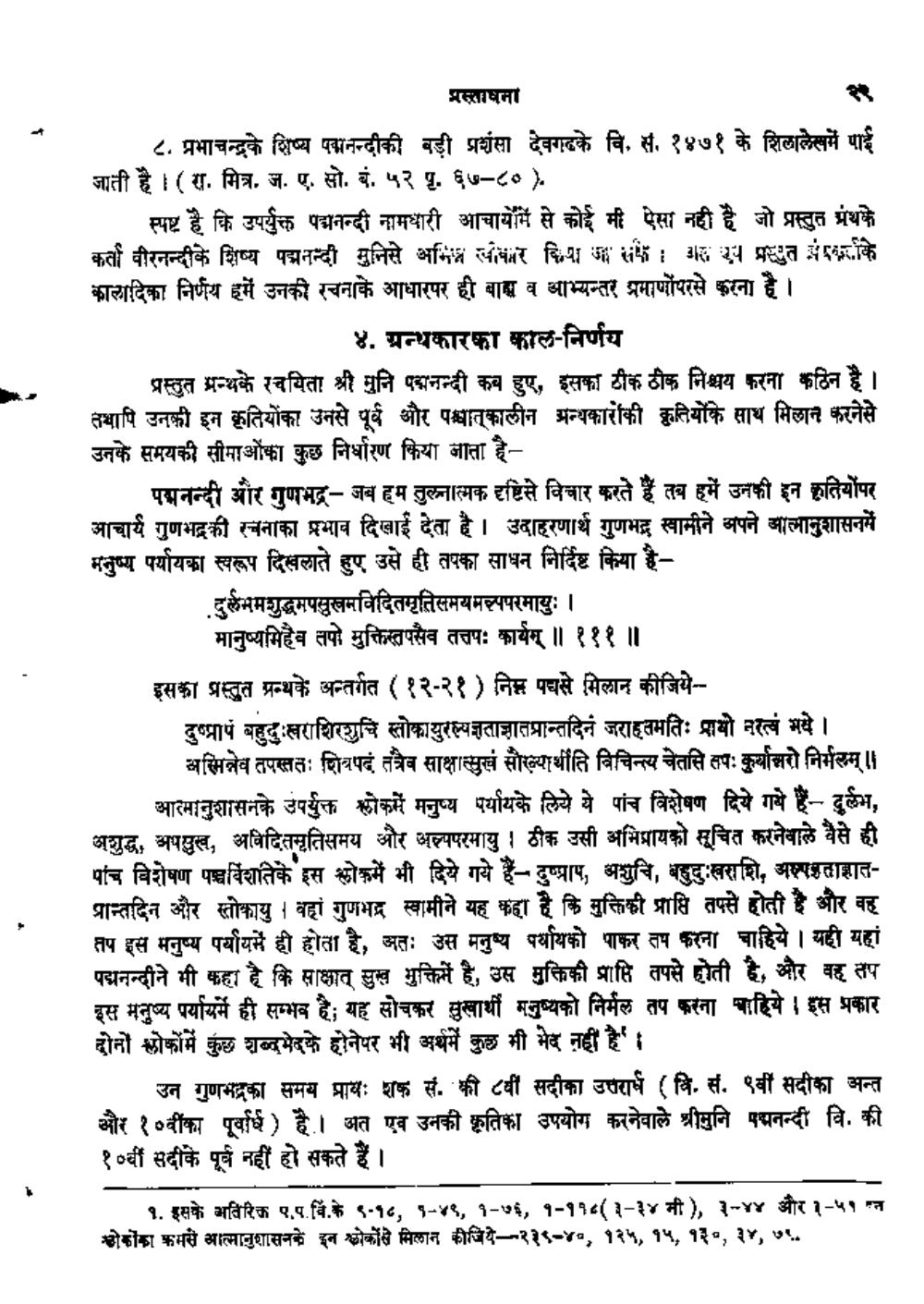________________
प्रस्तावना
८. प्रभाचन्द्रके शिष्य पानन्दीकी बड़ी प्रशंसा देवगढके वि. स. १४७१ के शिलालेख में पाई जाती है । (रा. मित्र. ज. ए. सो. बं. ५२ पृ. ६७–८० ).
स्पष्ट है कि उपर्युक्त पद्मनन्दी नामधारी आचार्यों में से कोई मी ऐसा नहीं है जो प्रस्तुत ग्रंथके कर्ता वीरनन्दीके शिष्य पद्मनन्दी मुनिसे अभिनवकार किया जा सके। प्रस्तुत कालादिका निर्णय हमें उनकी रचना के आधारपर ही बाह्य व आभ्यन्तर प्रमाणपरसे करना है ।
के
४. ग्रन्थकारका काल-निर्णय
प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता श्री मुनि पद्मनन्दी कब हुए, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है । तथापि उनकी इन कृतियोंका उनसे पूर्व और पश्चात्कालीन ग्रन्थकारोंकी कृतियोंके साथ मिलान करने से उनके समय की सीमाओंका कुछ निर्धारण किया जाता है
पद्मनन्दी और गुणभद्र - जब हम तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करते हैं तब हमें उनकी इन कृतियोंपर आचार्य गुणभद्रकी रचनाका प्रभाव दिखाई देता है । उदाहरणार्थ गुणभद्र स्वामीने अपने आत्मानुशासनमें मनुष्य पर्यायका स्वरूप दिखलाते हुए उसे ही तपका साधन निर्दिष्ट किया है
. दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृत्तिसमय मल्पपरमायुः । मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥ १११ ॥
इसका प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत (१२-२१) निम्न पद्यसे मिलान कीजिये -
दुष्प्रापं बहुदुः खराशिरशुचि स्तोका युरल्पज्ञताज्ञातप्रान्तदिनं जराहतमतिः प्रायो नरत्वं भये । अस्मिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षात्सुखं सौख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तपः कुर्यान्नरो निर्मलम् ॥ आत्मानुशासनके उपर्युक्त लोकमें मनुष्य पर्यायके लिये ये पांच विशेषण दिये गये हैं- दुर्लभ, अशुद्ध, अपसुख, अविदितमृतिसमय और अल्पपरमायु । ठीक उसी अभिप्रायको सूचित करनेवाले वैसे ही पांच विशेषण पञ्चविंशतिके इस श्लोक में भी दिये गये हैं- दुष्प्राप, अशुचि, बहुदुः खराशि, अश्पक्षताज्ञातप्रान्तदिन और स्तोकायु | वहां गुणभद्र स्वामीने यह कहा है कि मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है और वह तप इस मनुष्य पर्यायमें ही होता है, अतः उस मनुष्य पर्यायको पाकर तप करना चाहिये । यही यहां पद्मनन्दी ने भी कहा है कि साक्षात् सुख मुक्तिमें है, उस मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है, और वह तप इस मनुष्य पर्याय ही सम्भव है; यह सोचकर सुखार्थी मनुष्यको निर्मल तप करना चाहिये। इस प्रकार दोनों लोकों में कुछ शब्दभेदके होनेपर भी अर्थमें कुछ भी भेद नहीं है'।
उन गुणभद्रका समय प्रायः शक सं. की ८वीं सदीका उत्तरार्ध (वि. सं. ९वीं सदीका अन्त और १०वींका पूर्वार्ध) है । अत एव उनकी कृतिका उपयोग करनेवाले श्रीमुनि पद्मनन्दी वि. की १०वीं सदीके पूर्व नहीं हो सकते हैं।
१. इसके अतिरिक्त प. प. विं.के ९-१८, १४९, १-७६, १-११८ ( ३-३४ मी ), ३-४४ और १-५१ वो कमसे आत्मानुशासनके इन श्लोकों से मिलान कीजिये - २३९-४०, १२५, १५, १३०, ३४, ७९.