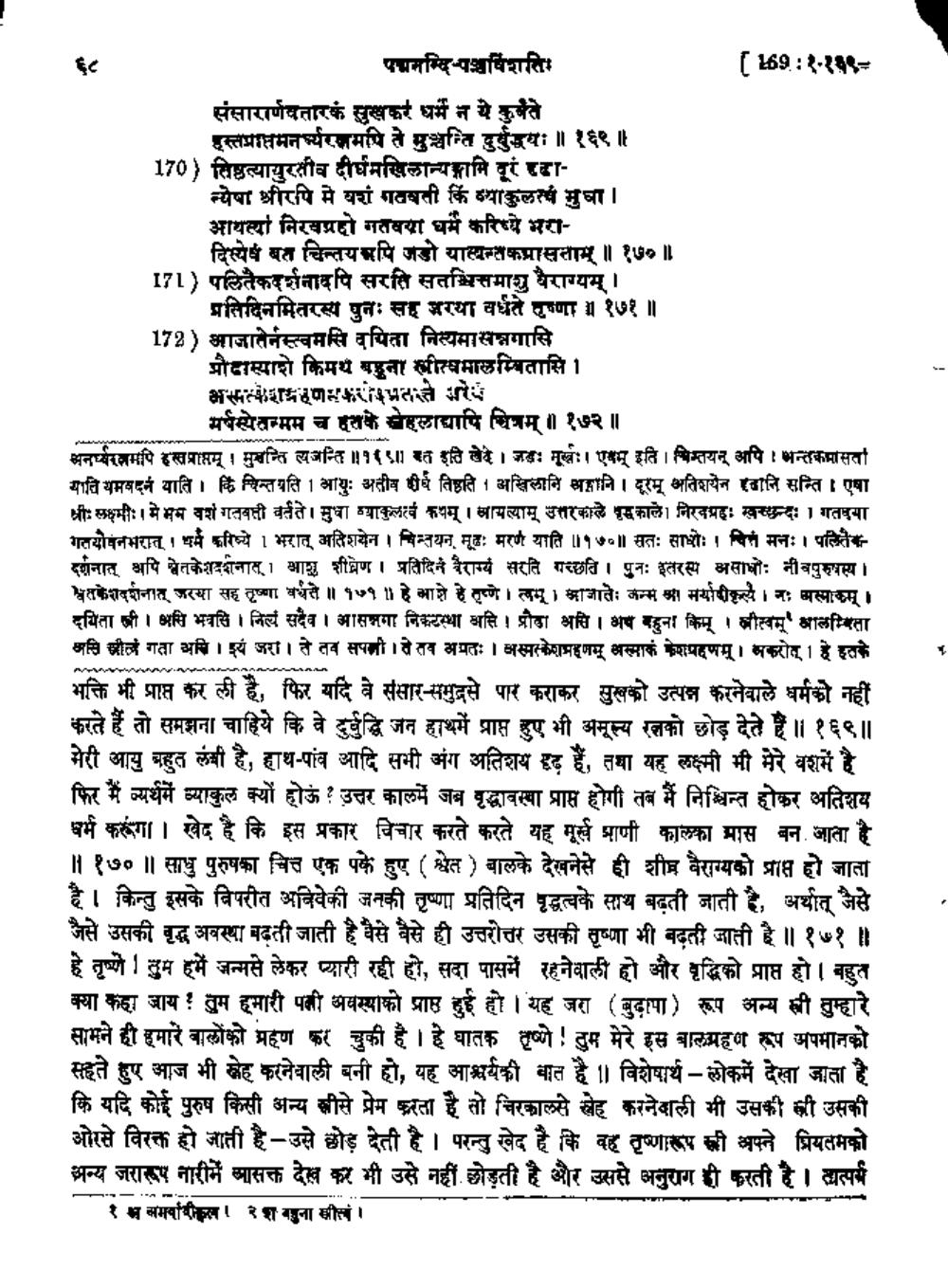________________
पचमन्दि-पञ्चर्षिशतिर
[169:१.२१९ संसारार्णवतारकं सुखकर धर्म न ये कुर्वते
हस्तपातमनर्व्यरनमपि ते मुञ्चन्ति दुर्बुद्धयः ॥ १९ ॥ 170) तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्यङ्गामि दूर रखा
न्येषा श्रीरपि मे वशं गतवती किं व्याकुलत्वं मुषा। आयत्या निरवग्रहो मतवया धर्म करिष्ये भरा
दिस्येष बत चिन्तयमपि जडो यात्यन्तकपासताम् ॥ १७॥ 171) पलितैकदर्शनादपि सरति सतश्चिसमाशु वैराग्यम् ।
प्रतिदिनमितरस्य पुनः सह जरया वर्धते शुष्णा ॥ १७१ ॥ 172) आजाते स्त्वमसि वयिता नित्यमासन्नगासि
प्रौदास्याशे किमथ बहुना स्त्रीस्वमालम्बितासि । भस्मशानणरमतरते बरेच
मर्षस्पेतम्मम च इतके खेहलाद्यापि चित्रम् ॥ १७२ ॥ मनरनमपि हस्सप्राप्तम् । मुखन्ति त्यजन्ति ॥१६॥ रत इति खेदे । जडः मूर्खः । एवम् इति । विस्तयन् अपि । भन्तकमासा याति यमबदन याति । किचिन्तयति 1 आयुः अतीव ही तिष्ठति । अखिलानि हानि । दूरम् अतिशयेन हतानि सन्ति । एषा श्री लक्ष्मी मे मम वशं गतवती वर्तते। मुधा व्याकुलवं कथम् । बायल्याम् उत्तरकाले वृक्षकाले। निरकप्रहः खस्छन्दः । गतवया गतयोवनभरात् । धर्म करिष्ये 1 भरात् अतिशयेन । चिन्तयन मूढः मरण याति ॥१७॥ सतः साशेः । पितं मनः। पलितक दर्शनात् अपि श्वेतकेशवशनास्। आशु शीघ्रण । प्रतिदिन वैराग्यं सरति गरछति । पुनः इतरस्म असाधोः नीवपुरुषस्य । श्वतकेशदर्शनात् जरया सह तृष्या वर्धते ॥ ११॥ हे आशे हे सृष्णे । त्वम् । माजातेः जन्म का मर्यापीकल्यै । नः अस्माकम् । दयिता श्री। असि भवसि । नित्यं सदैव । आसनगा निकटस्था असि । प्रौडा असि । अब बहुना किम् । श्रीस्वम् बालम्बिता मसि श्रीलं गता अपि । इयं जरा। ते तब सपनी । ते तव अपतः । अस्मस्केरामहणम् अस्माकं फेशपहणम् । मकरोत् । हे इतके भक्ति भी प्राप्त कर ली है, फिर यदि वे संसार-समुद्रसे पार कराकर सुखको उत्पन्न करनेवाले धर्मको नहीं करते हैं तो समझना चाहिये कि वे दुर्बुद्धि जन हाथमें प्राप्त हुए भी अमूल्य रक्षको छोड़ देते हैं ।। १६९।। मेरी आयु बहुत लंबी है, हाथ-पांव आदि सभी अंग अतिशय रद हैं, तथा यह लक्ष्मी मी मेरे वशमें है फिर मैं व्यर्थमें व्याकुल क्यों होऊ ? उत्तर कालमें जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मैं निश्चिन्त होकर अतिशय धर्म करूंगा। खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूर्ख प्राणी कालका ग्रास बन जाता है ॥ १७० ॥ साधु पुरुषका चित्त एक पके हुए ( श्वेत ) बालके देखनेसे ही शीघ्र वैराग्यको प्राप्त हो जाता है। किन्तु इसके विपरीत अविवेकी जनकी तृष्णा प्रतिदिन वृद्धत्वके साथ बढ़ती जाती है, अर्थात् जैसे जैसे उसकी वृद्ध अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर उसकी सृष्णा भी बढ़ती जाती है ॥ १७१ ॥ हे तृष्णे ! तुम हमें जन्मसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासमें रहनेवाली हो और वृद्धिको प्राप्त हो । बहुत क्या कहा जाय ! तुम हमारी पनी अवस्थाको प्राप्त हुई हो । यह जरा (बुढ़ापा) रूप अन्य स्त्री तुम्हारे सामने ही हमारे बालोंको ग्रहण कर चुकी है । हे घातक तृष्णे ! तुम मेरे इस बालग्रहण रूप अपमानको सहते हुए आज भी स्नेह करनेवाली बनी हो, यह आश्चर्यकी बात है | विशेषार्थ-लोकमें देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य शीसे प्रेम करता है तो चिरकालसे खेह करनेवाली भी उसकी ली उसकी ओरसे विरक्त हो जाती है-उसे छोड़ देती है। परन्तु खेद है कि वह तृष्णारूप स्त्री अपने प्रियतमको अन्य जरारूप नारीमें आसक्त देख कर भी उसे नहीं छोड़ती है और उससे अनुराग ही करती है। यत्पर्य
भ समयविकल । २श बहुना स्त्रीत्वं ।