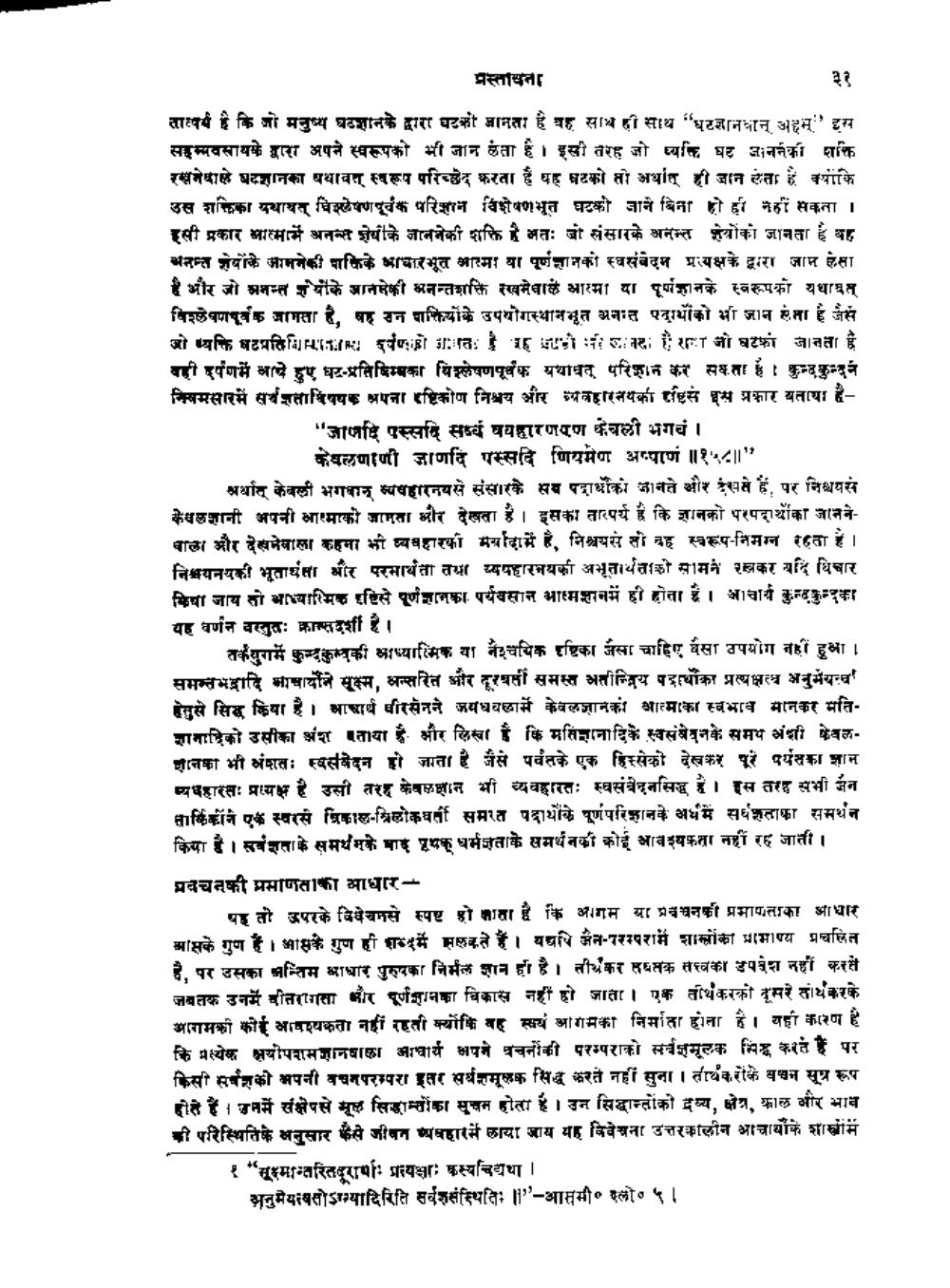________________
प्रस्तावना तात्पर्य है कि जो मनुष्य घटज्ञानके द्वारा घटको जानता है वह साथ ही साथ “घटज्ञानवान् अहम्' इय सहम्मवसायके द्वारा अपने स्वरूपको भी जान लेता है। इसी तरह जो व्यक्ति घट जानकी शक्ति रखनेवाले घदज्ञानका यथावत् स्वरूप परिच्छेद करता है यह घटको तो अर्थात् ही जान लेता है क्योंकि उस शक्तिका यथावत् विश्लेषणपूर्वक परिझान विशेषाभूत घटको जाने बिना हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार आरमामें अनन्त ज्ञेयोके जाननेकी शक्ति है अतः जो संसारके अनन्त शेयोंको जानता है वह अनन्त शेयोंके आमनेकी पाकिके आधारभूत आत्मा या पूर्ण ज्ञानको स्वसंवेदम प्रत्यक्षके द्वारा जाम हे.सा है और जो अमम्स शेयोके जानकी अनन्तशक्ति रखमेवाके आरमा या पूर्वज्ञानके स्वरूपको यथावत विश्लेषणपूर्वक जामता है, यह सन शक्तियों के उपयोगस्थानभूत अनात पदार्थों को भी जान सेता है जैसे ओ व्यक्ति घटप्रतिEिTARA हो जाता है हमीभीनस है सा जो घटकां जानता है वही दर्पगमें आये हुए घर-प्रतिविम्बका विश्लेषणपूर्वक यथावत् परिज्ञान कर सकता है। कुन्दकुन्दन नियमसारमें सर्वज्ञताविषयक अपना दृष्टिकोण निश्रय और व्यवहारनयका राष्टसे इस प्रकार बताया है
"जाणादि पस्सदि सर्व पयहारणपण केचली भगवं ।
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१५८॥" श्रर्थात् केबली भगवान ध्यपहारनयसे संसारकै सब पदााँको जानते और इससे है. पर निश्चय केवलज्ञानी अपनी आत्माको जामता और देखता है। इसका तात्पर्य है कि ज्ञानको परपदार्थोका जाननेपाला और देखनेवाला कहना भी व्यवहारको मर्यादा में है, निश्चयस तो वह स्वरूप-निमग्न रहता है। निश्चयनयकी भूतार्थता और परमार्थता तया य्यपहारमयी अभूतार्थताको सामने रखकर यदि विचार किया जाय तो भाभ्यात्मिक दृष्टिसे पूर्ण ज्ञानका पर्यवसान माध्मज्ञानमें ही होता है। आचार्य कुन्ठान्दका यह वर्णन वस्तुतः क्रासदी है।
तर्क युगमें कुन्दकुम्बकी आध्यात्मिक या नैश्चयिक रष्टिका जैसा चाहिए पैसा उपयोग नहीं हुआ। समन्तभद्रादि भाचार्योंने सूक्ष्म, आन्तरित और दूरवती समस्त अतीन्द्रिय पदाथाँका प्रत्यक्षत्व अनुमैयन्च' हेतुसे सिद्ध किया है। आचार्य धीरसेनने जयधवलामें केवलज्ञानको आत्माका स्वभाव मानकर मतिज्ञानाटिको उसीका अंश बताया है और लिस्वा ई कि मसिज्ञानादिक स्वसंवेवन के समय अंशी केवलज्ञानका भी अंशतः स्वसवेदन हो जाता है जैसे पर्वतके एक हिस्सेको देखकर पूरे पर्यतका ज्ञान प्यवहारतः प्रत्यक्ष है उसी तरह केवलज्ञान भी व्यवहारतः स्वसंबेदनसिद्ध है। इस तरह सभी जैन तार्किकॉने एक स्वरस निकाल-श्रिलोकवर्ती समरत पदायोंके चूर्णपरिझानके अर्थ में सर्वशताफा समर्थन किया है। सर्वज्ञता के समर्थमके माद पृथक् धर्मज्ञताके समर्थनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रवचनकी प्रमाणसाका आधार
यह तो उपरके विधेयमसे स्पष्ट हो जाता है कि आगम या प्रवचनकी प्रमापाताका आधार आप्लके गुण है। आक्षक गुण ही शमदमें मलबते हैं। यद्यपि जन-परम्परामें शाम्सोका प्रामाण्य प्रचलित है, पर उसका अन्तिम भाधार पुरुषका निर्मल ज्ञान ही है। तीर्थकर हषप्तक सत्त्वका उपश नहीं करते जबतक उनमें बीतनरागसा और पूर्णज्ञानका विकास नहीं हो जाता। एक तीर्थकरको दूसरे तीर्थकरके आगमकी कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वह स्वयं आगमका निर्माता होता है। यही कारण है कि प्रत्येक भयोपशमज्ञानधाका आचार्य अपने वचन की परम्पराको सर्वज्ञमूलक सिद्ध करते हैं पर किसी सशको अपनी वचनपरम्परा इतर सर्वशमूलक सिद्ध करते नहीं सुना । ताथवरोके वचन सूत्र रूप होते हैं। उनमें संक्षेपसे मूह सिद्धान्तोंका सचम होता है। उन सिद्धान्तोंको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की परिस्थिति के अनुसार कैसे जीवन व्यवहार में लाया जाय यह विवेचना उत्तरकालीन आचायाँके शास्त्राम
१ "सूक्ष्मान्तरितदुरापः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा |
अनुमेयत्वतोऽम्यादिरिति सशसंस्थिति"-आसमी० श्लो० ५।