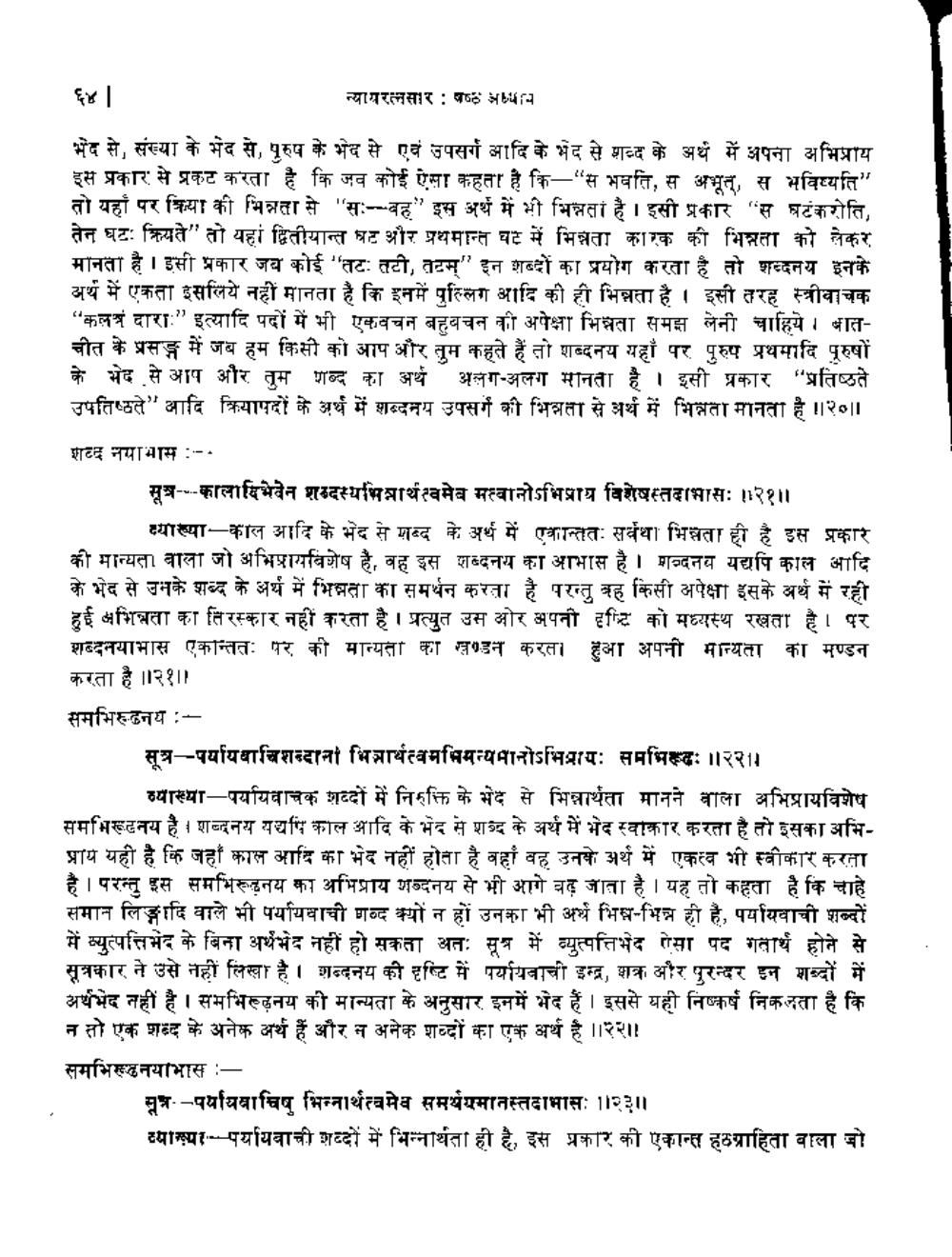________________
६४ |
न्यायरत्नसार : षष्ठ अध्याय
भेद से, संस्या के भेद से, पुरुष के भेद से एवं उपसर्ग आदि के भेद से शब्द के अर्थ में अपना अभिप्राय इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब कोई ऐसा कहता है कि-"स भवति, स अभूत्, स भविष्यति" तो यहाँ पर क्रिया की भिन्नता से "सः--बह" इस अर्थ में भी भिन्नता है । इसी प्रकार “स घटंकरोति, तेन घटः क्रियते" तो यहां द्वितीयान्त घट और प्रथमान्त घट में भिन्नता कारक की भिन्नता को लेकर मानता है । इसी प्रकार जब कोई "तटः तटी, तटम्" इन शब्दों का प्रयोग करता है तो शब्दन य इनके अर्थ में एकता इसलिये नहीं मानता है कि इनमें पुल्लिग आदि की ही भिन्नता है । इसी तरह स्त्रीवाचक "कलत्रं दाराः" इत्यादि पदों में भी एकवचन बहुवचन की अपेक्षा भिन्नता समझ लेनी चाहिये । बातचीत के प्रसङ्ग में जब हम किसी को आप और तुम कहते हैं तो शब्दनय यहाँ पर पुरुष प्रथमादि पुरुषों के भेद से आप और तुम शब्द का अर्थ अलग-अलग मानता है । इसी प्रकार "प्रतिष्ठते उपतिष्ठते" आदि क्रियापदों के अर्थ में शब्दमय उपसर्ग की भिन्नता से अर्थ में भिन्नता मानता है ।।२०।।
शब्द नयाभाम:
मूत्र---कालादिभेवेन शम्दस्यभिन्नार्थत्वमेव मत्वानोऽभिप्राय विशेषस्तदाभासः ॥२१॥
क्ष्याख्या-काल आदि के भेद से शब्द के अर्थ में एवान्ततः सर्वथा भिन्नता ही है इस प्रकार की मान्यता वाला जो अभिप्रायबिशेष है, वह इस शब्दनय का आभास है। शन्दनय यद्यपि काल आदि के भेद से उनके शब्द के अर्थ में भिन्नता का समर्थन करता है परन्तु वह किसी अपेक्षा इसके अर्थ में रही हुई अभिन्नता का तिरस्कार नहीं करता है । प्रत्युत उस ओर अपनी दृष्टि को मध्यस्थ रखता है। पर शब्दनयाभास एकान्ततः पर की मान्यता का खाउन करता हुआ अपनी मान्यता का मण्डन करता है ।।२१।। समभिरूढनय :
सूत्र-पर्यायवाचिशन्दाना भिन्नार्थत्वमभिमन्यमानोऽभित्रायः समभिदः ॥२२॥
व्याख्या–पर्यायवाचक शब्दों में निरुक्ति के भेद से भिन्नार्थता मानने वाला अभिप्रायविशेष समभिरूटनय है । शब्दनय यद्यपि काल आदि के भेद से शब्द के अर्थ में भेद स्वाक्रार करता है तो इसका अभिप्राय यही है कि जहाँ काल आदि का भेद नहीं होता है वहाँ वह उनके अर्थ में एकत्व भी स्वीकार करता है । परन्तु इस समभिरूढनय का अभिप्राय शब्दनय से भी आगे बढ़ जाता है । यह तो कहता है कि चाहे समान लिङ्गादि वाले भी पर्यायवाची शब्द क्यों न हों उनका भी अर्थ भिन्न-भिन्न ही है, पर्यायवाची शब्दों में व्युत्पत्तिभेद के बिना अर्थभेद नहीं हो सकता अतः सूत्र में व्युत्पत्तिभेद ऐसा पद गतार्थ होने से सूत्रकार ने उसे नहीं लिखा है। शन्दनय की दृष्टि में पर्यायवाची इन्द्र, शक्र और पुरन्दर इन शब्दों में अर्थभेद नहीं है । समभिरूडनय की मान्यता के अनुसार इनमें भेद हैं । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि न तो एक शब्द के अनेक अर्थ हैं और न अनेक शब्दों का एक अर्थ है ।।२२॥ समभिरुवनयाभास :
सूत्र--पर्यायवाचिषु भिन्नार्थत्वमेव समर्थयमानस्तदाभासः ॥२३॥ व्याया---पर्यायवाची शब्दों में भिन्नार्थता ही है, इस प्रकार की एकान्त हतग्राहिता वाला बो