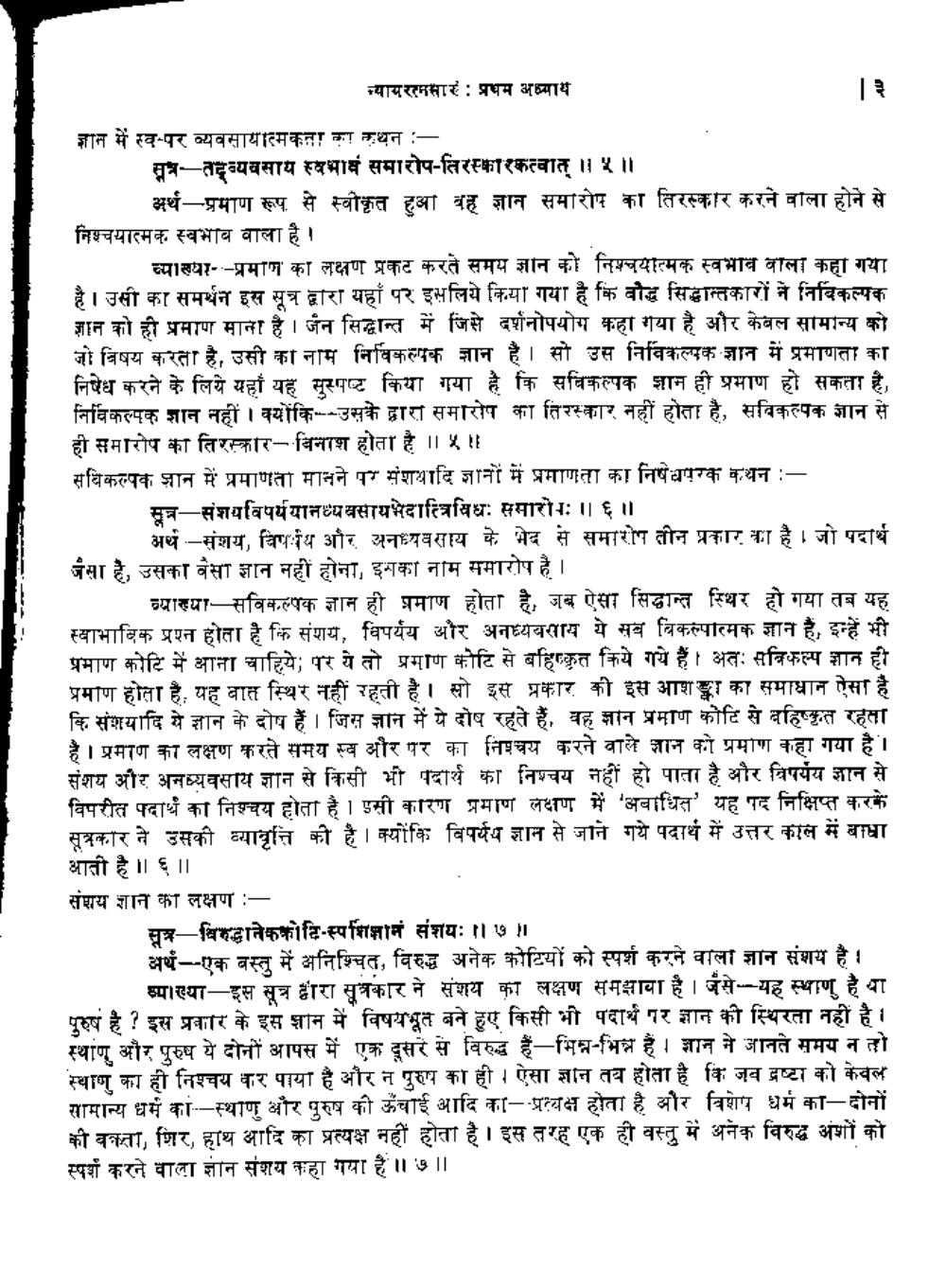________________
न्यायररमसार: प्रथम अध्याय
ज्ञान में स्व-पर व्यवसायात्मकता का कथन :
सूत्र-तव्यवसाय स्वभावं समारोप-तिरस्कारकत्वात् ॥५॥
अर्थ-प्रमाण रूप से स्वीकृत हुआ वह ज्ञान समारोप का तिरस्कार करने वाला होने से निश्चयात्मक स्वभाव वाला है।
व्याख्या---प्रमाण का लक्षण प्रकट करते समय ज्ञान को निश्चयात्मक स्वभाव वाला कहा गया है। उसी का समर्थन इस सूत्र द्वारा यहाँ पर इसलिये किया गया है कि बौद्ध सिद्धान्तकारों ने निर्विकल्पक ज्ञान को ही प्रमाण माना है । जंन सिद्धान्त में जिसे दर्शनोपयोग कहा गया है और केवल सामान्य को जो विषय करता है, उसी का नाम निर्विकल्पक ज्ञान है । सो उस निर्विकल्पक ज्ञान में प्रमाणता का निषेध करने के लिये यहाँ यह सुस्पष्ट किया गया है कि सविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, निर्विकल्पक ज्ञान नहीं। क्योंकि उसके द्वारा समारोप का तिरस्कार नहीं होता है, सविकल्पक ज्ञान से ही समारोप का तिरस्कार-विनाश होता है ।। ५ ॥ सविकल्पक ज्ञान में प्रमाणता मानने पर संशयादि ज्ञानों में प्रमाणता का निषेधपरक कथन :
सूत्र-संशयविपर्ययानध्यवसायभेदात्त्रिविधः समारोपः ।। ६॥
अर्थ -संशय, विपर्षय और अनाध्यवसाय के भेद से समारोप तीन प्रकार का है। जो पदार्थ जसा है, उसका वैसा ज्ञान नहीं होना, इसका नाम समारोप है ।
व्याख्या सविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण होता है, जब ऐसा सिद्धान्त स्थिर हो गया तब यह स्वाभाविक प्रश्न होता है कि संशय, विपर्यय और अनध्यबसाय ये सब बिकल्पात्मक ज्ञान हैं, इन्हें भी प्रमाण कोटि में आना चाहिये, पर ये तो प्रमाण कोटि से बहिष्कृत किये गये हैं। अतः सविकल्प ज्ञान ही प्रमाण होता है. यह बात स्थिर नहीं रहती है। सो इस प्रकार की इस आशङ्का का समाधान ऐसा है कि संशयादि ये ज्ञान के दोष हैं। जिस ज्ञान में ये दोष रहते हैं, वह ज्ञान प्रमाण कोटि से बहिष्कृत रहता है। प्रमाण का लक्षण करते समय स्व और पर का निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। संशय और अनध्यवसाय ज्ञान से किसी भी पदार्थ का निश्चय नहीं हो पाता है और विपर्यय ज्ञान से विपरीत पदार्थ का निश्चय होता है । एमी कारण प्रमाण लक्षण में 'अबाधित' यह पद निक्षिप्त करके सूत्रकार ने उसकी ध्यावृत्ति की है। क्योंकि विपर्यय ज्ञान से जाने गये पदार्थ में उत्तर काल में बाधा आती है ॥ ६॥ संशय ज्ञान का लक्षण :
सूत्र-विद्धानेककोदि-स्पशिज्ञानं संशयः ॥ ७ ॥ अर्थ--एक बस्तु में अनिश्चित, विरुद्ध अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय है।
व्याख्या-इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने संशय का लक्षण समझाया है । जैसे-यह स्थाणु है या पुरुष है ? इस प्रकार के इस शान में विषयभूत बने हुए किसी भी पदार्थ पर ज्ञान की स्थिरता नहीं है। स्थाणु और पुरुष ये दोनों आपस में एक दूसरे से विरुद्ध हैं-भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञान ने जानते समय न तो स्थाणु का ही निश्चय कर पाया है और न पुरुष का ही । ऐसा ज्ञान तब होता है कि जब द्रष्टा को केवल सामान्य धर्म का-स्थाणु और पुरुष की ऊँचाई आदि का- प्रत्यक्ष होता है और विशेष धर्म का-दोनों की वक्रता, शिर, हाथ आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस तरह एक ही वस्तु में अनेक विरुद्ध अंशों को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय कहा गया है ।। ७ ।।