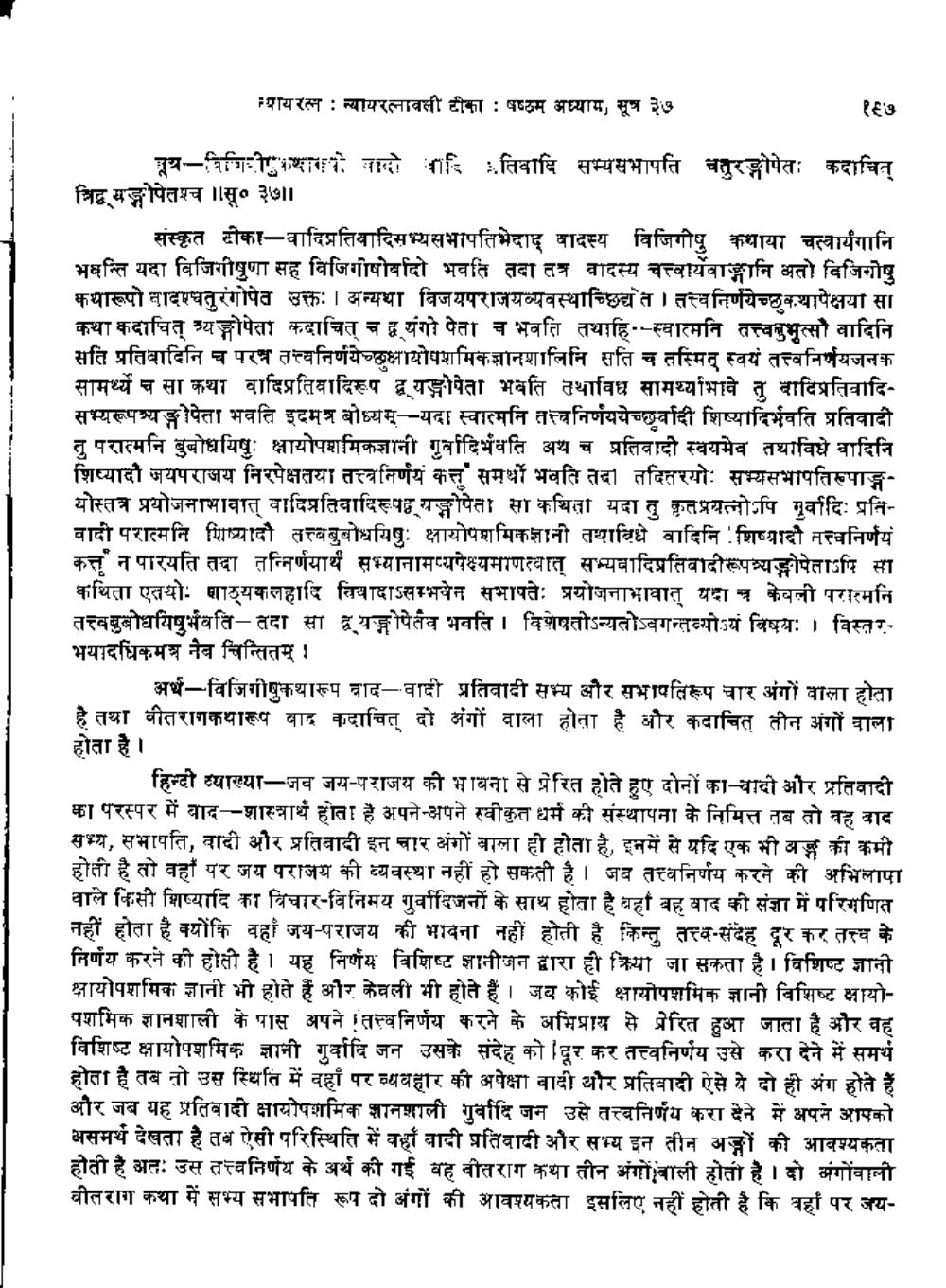________________
म्पायरत्न : न्यायरत्नावली टीका : षष्ठम अध्याय, सूत्र ३७
जून-त्रिणिती काय जादो दि तिवादि सभ्यसभापति चतुरङ्गोपेतः कदाचित् त्रि मङ्गोपेतश्च ॥सू० ३७।।
__ संस्कृत टोका-वादिप्रतियादिमभ्यसभापतिभेदाद् वादस्य विजिगीषु कथाया चत्वार्यगानि भवन्ति यदा विजिगीषुणा सह विजिगीषो दो भवति तदा तत्र बादस्य चत्त्वार्यवाङ्गानि अतो दिजिगोषु कथारूपो बादश्चतुरंगोपेत उक्तः । अन्यथा विजयपराजयव्यवस्थाच्छिद्यत । तत्त्वनिर्णयेच्छकथापेक्षया सा कथा कदाचित् व्यङ्गोपेता कदाचित् च द यंगो पेता च भवति तथाहि- स्वात्मनि तत्त्वानुभूत्सौ वादिनि सति प्रतिवादिनि च परत्र तत्त्वनिर्णयेच्छुक्षायोपशमिकज्ञानशालिनि सति च तस्मित् स्वयं तत्त्वनिर्णयजनक सामर्थ्य च सा कथा वादिप्रतिवादिरूप द यजोपेता भवति तथाविध सामाभावे त वादिप्रतिवादिसभ्यरूपयङ्गोपेता भवति इदमत्र बोध्यम्-यदा स्वात्मनि तत्त्वनिर्णययेच्छर्वादी शिष्यादिर्भवति प्रतिवादी तु परात्मनि बुबोधयिषुः क्षायोपशमिकज्ञानी गुर्वादिर्भवति अथ च प्रतिवादी स्वयमेव तथाविधे वादिनि शिष्यादी जयपराजय निरपेक्षतया तत्त्वनिर्णय कत्तु समों भवति तदा तदितरयोः सभ्यसभापतिरूपाङ्गयोस्तत्र प्रयोजनाभावात् वादिप्रतिवादिरूपह यगोपेता सा कथिता यदा तु कृतप्रयत्नोऽपि मुर्वादिः प्रतिवादी परात्मनि शिष्यादौ तत्त्वबुबोधयिषुः क्षायोपशामिकज्ञानी तथाविधे वादिनि 'शिष्यादौ तत्त्वनिर्णय कत्तुं न पारयति तदा तन्निर्णयार्थ सभ्यानामप्यपेक्ष्यमाणत्वात् सभ्यवादिप्रतिबादीरूपश्यङ्गोपेताऽपि सा कथिता एतयोः शाठ्यकलहादि विवादाऽसम्भवेन सभापतेः प्रयोजनाभावात् यदा न केवली परात्मनि तत्त्वबुबोधयिषुर्भवति- तदा सा दू यङ्गोपेतैव भवति । विशेषतोऽन्यतोऽवगन्तव्योऽयं विषयः । विस्तरभयादधिकमत्र नैव चिन्तितम् ।
अर्थ-विजिगीषुकथारूप वाद-वादी प्रतिवादी सभ्य और सभापतिरूप चार अंगों वाला होता है तथा वीतरागकथारूप बाद कदाचित् दो अंगों वाला होता है और कदाचित तीन अंगों वाला होता है।
हिन्दी व्याख्या-जव जय-पराजय की भावना से प्रेरित होते हुए दोनों का चादी और प्रतिवादी का परस्पर में बाद-शास्त्रार्थ होता है अपने-अपने स्वीकृत धर्म की संस्थापना के निमित्त तब तो वह वाद सभ्य, सभापति, वादी और प्रतिवादी इन चार अंगों वाला ही होता है, इनमें से यदि एक भी अङ्ग की कमी होती है तो वहाँ पर जय पराजय की व्यवस्था नहीं हो सकती है। जब तत्त्वनिर्णय करने की अभिलापा वाले किसी शिष्यादि का विचार-विनिमय गुर्वादिजनों के साथ होता है वहाँ वह वाद की संज्ञा में परिगणित नहीं होता है क्योंकि वहाँ जय-पराजय की भावना नहीं होती है किन्तु तत्त्व-संदेह दूर कर तत्त्व के निर्णय करने की होती है। यह निर्णय विशिष्ट ज्ञानीजन द्वारा ही क्रिया जा सकता है। विशिष्ट ज्ञानी क्षायोपशमिक ज्ञानी भी होते हैं और केवली भी होते हैं। जब कोई क्षायोपशमिक ज्ञानी विशिष्ट क्षायोपशमिक ज्ञानशाली के पास अपने तत्त्वनिर्णय करने के अभिप्राय से प्रेरित हुआ जाता है और वह विशिष्ट क्षायोपशमिक ज्ञानी गुर्वादि जन उसके संदेह को दूर कर तत्त्वनिर्णय उसे करा देने में समर्थ होता है तब तो उस स्थिति में वहाँ पर व्यवहार की अपेक्षा बादी और प्रतिवादी ऐसे ये दो ही अंग होते हैं और जब यह प्रतिवादी क्षायोपशमिक शानशाली गुर्वादि जन उसे तत्त्वनिर्णय करा देने में अपने आपको असमर्थ देखता है तब ऐसी परिस्थिति में वहाँ वादी प्रतिवादी और सभ्य इन तीन अङ्गों की आवश्यकता होती है अतः उस तत्त्वनिर्णय के अर्थ की गई वह वीतराग कथा तीन अंगोंवाली होती है । दो अंगोंवाली वीतराग कथा में सभ्य सभापति रूप दो अंगों की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि वहां पर जय