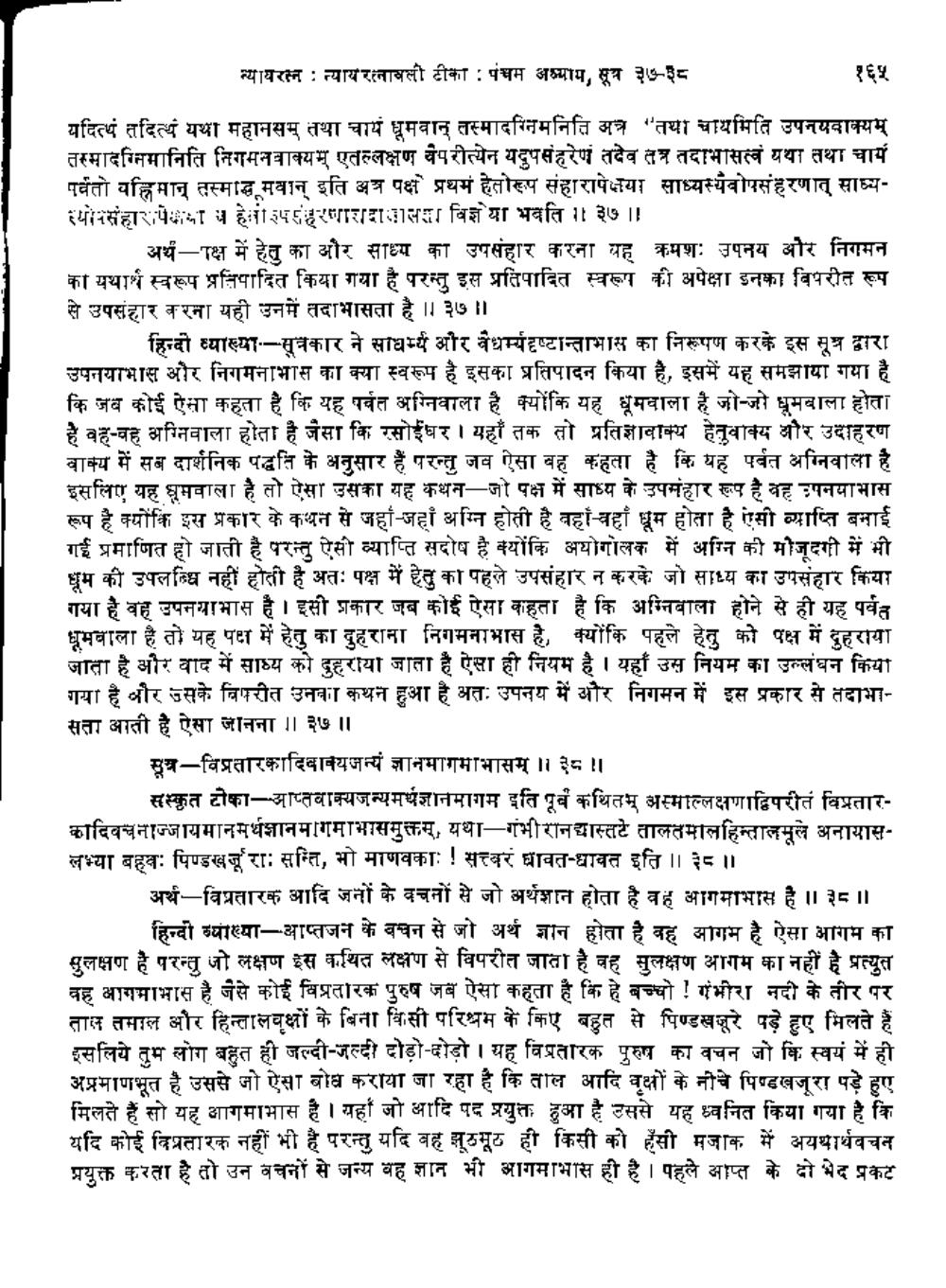________________
न्यायरन : न्याय रत्नावली टीका : पंचम अध्याय, सूत्र ३७-३८
१६५
यदित्थं तदित्यं यथा महानसम् तथा चायं धूमवान् तस्मादग्निमनिति अत्र "तथा चायमिति उपनयवाक्यम् तस्मादग्निमानिति निगमनवाक्यम् एतल्लक्षण वैपरीत्येन यदुपसंहरेणं तदेव तत्र तदाभासत्वं यथा तथा चार्य पर्वतो पह्निमान् तस्माद्ध मवान् इति अत्र पक्ष प्रथमं हेतोरूप संहारापेक्षया साध्यस्यवोपसंहरणात् साध्यस्योपसंहा पक्षमा पहेको इपहरणासदालासमा विज्ञ या भवति ।। ३७ ।।।
अर्थ-पक्ष में हेतु का और साध्य का उपसंहार करना यह क्रमशः उपनय और निगमन का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादित किया गया है परन्तु इस प्रतिपादित स्वरूप की अपेक्षा इनका विपरीत रूप से उपसंहार करना यही उनमें तदाभासता है ।। ३७ ॥
हिन्दी व्याख्या--सूत्रकार ने साधम्र्य और वैधर्म्यदृष्टान्ताभास का निरूपण करके इस सूत्र द्वारा उपनयाभास और निगमनाभास का क्या स्वरूप है इसका प्रतिपादन किया है, इसमें यह समझाया गया है कि जब कोई ऐसा कहता है कि यह पर्वत अग्निवाला है क्योंकि यह धूमधाला है जो-जो धूमबाला होता है वह-वह अग्निवाला होता है जैसा कि रसोईघर । यहाँ तक तो प्रतिज्ञावाक्य हेतुवाक्य और उदाहरण वाक्य में सब दार्शनिक पद्धति के अनुसार हैं परन्तु जव ऐसा वह कहता है कि यह पर्वत अग्निवाला है इसलिए यह धूमवाला है तो ऐसा उसका यह कथन-जो पक्ष में साध्य के उपमहार रूप है वह उपनयाभास रूप है क्योंकि इस प्रकार के कथन से जहाँ-जहाँ अग्नि होती है वहाँ-वहाँ धूम होता है ऐसी व्याप्ति बनाई गई प्रमाणित हो जाती है परन्तु ऐसी व्याप्ति सदोष है क्योंकि अयोगोलक में अग्नि की मौजूदगी में भी धूम की उपलब्धि नहीं होती है अतः पक्ष में हेतु का पहले उपसंहार न करके जो साध्य का उपसंहार किया गया है वह उपनयाभास है। इसी प्रकार जब कोई ऐसा कहता है कि अग्निबाला होने से ही यह पर्वत धूमबाला है तो यह पक्ष में हेतु का दुहराना निगमनाभास है, क्योंकि पहले हेतु को पक्ष में दुहराया जाता है और बाद में साध्य को दुहराया जाता है ऐसा ही नियम है । यहाँ उस नियम का उल्लंघन किया गया है और उसके विपरीत उनका कथन हुआ है अतः उपनय में और निगमन में इस प्रकार से तदाभासता आती है ऐसा जानना ।। ३७ ।।
सूत्र-विप्रतारकादिवाक्यजन्यं ज्ञानमागमाभासम् ॥ ३८॥
संस्कृत टोका-आप्तवाक्यजन्यमर्थज्ञानमागम इति पूर्व कथितम् अस्माल्लक्षणाद्विपरीतं विप्रतारकादिवचनाज्जायमानमर्थज्ञानमागमाभासमुक्तम्, यथा-गंभीरानद्यास्तटे तालतमालहिन्तालमूले अनायासलभ्या बहवः पिण्डखजू रा: सन्ति, भो माणवकाः ! सत्त्वरं धावत-धावत इति ।। ३८॥
अर्थ-विप्रतारक आदि जनों के वचनों से जो अर्थशान होता है वह आगमाभास है ।। ३८ ॥
हिन्दी व्याख्या-आप्तजन के बचन से जो अर्थ ज्ञान होता है वह आगम है ऐसा आगम का सुलक्षण है परन्तु जो लक्षण इस कथित लक्षण से विपरीत जाता है वह सुलक्षण आगम का नहीं है प्रत्युत वह आगमाभास है जैसे कोई विप्रतारक पुरुष जब ऐसा कहता है कि हे बच्चो ! गंभीरा नदी के तीर पर ताल तमाल और हिन्तालवृक्षों के बिना विसी परिश्रम के किए बहुत से पिण्डखजूरे पड़े हुए मिलते हैं इसलिये तुम लोग बहुत ही जल्दी-जल्दी दोड़ो-दोड़ो । यह विप्रतारक पुरुष का वचन जो कि स्वयं में ही अप्रमाणभूत है उससे जो ऐसा बोध कराया जा रहा है कि ताल आदि वृक्षों के नीचे पिण्डखजूरा पड़े हए मिलते हैं सो यह आगमाभास है । यहाँ जो आदि पद प्रयुक्त हुआ है उससे यह ध्वनित किया गया है कि यदि कोई विप्रतारक नहीं भी है परन्तु यदि वह झूठमूठ ही किसी को हँसी मजाक में अयथार्थवचन प्रयक्त करता है तो उन वचनों से जन्य वह ज्ञान भी आगमाभास ही है। पहले आप्त के दो भेद प्रकट