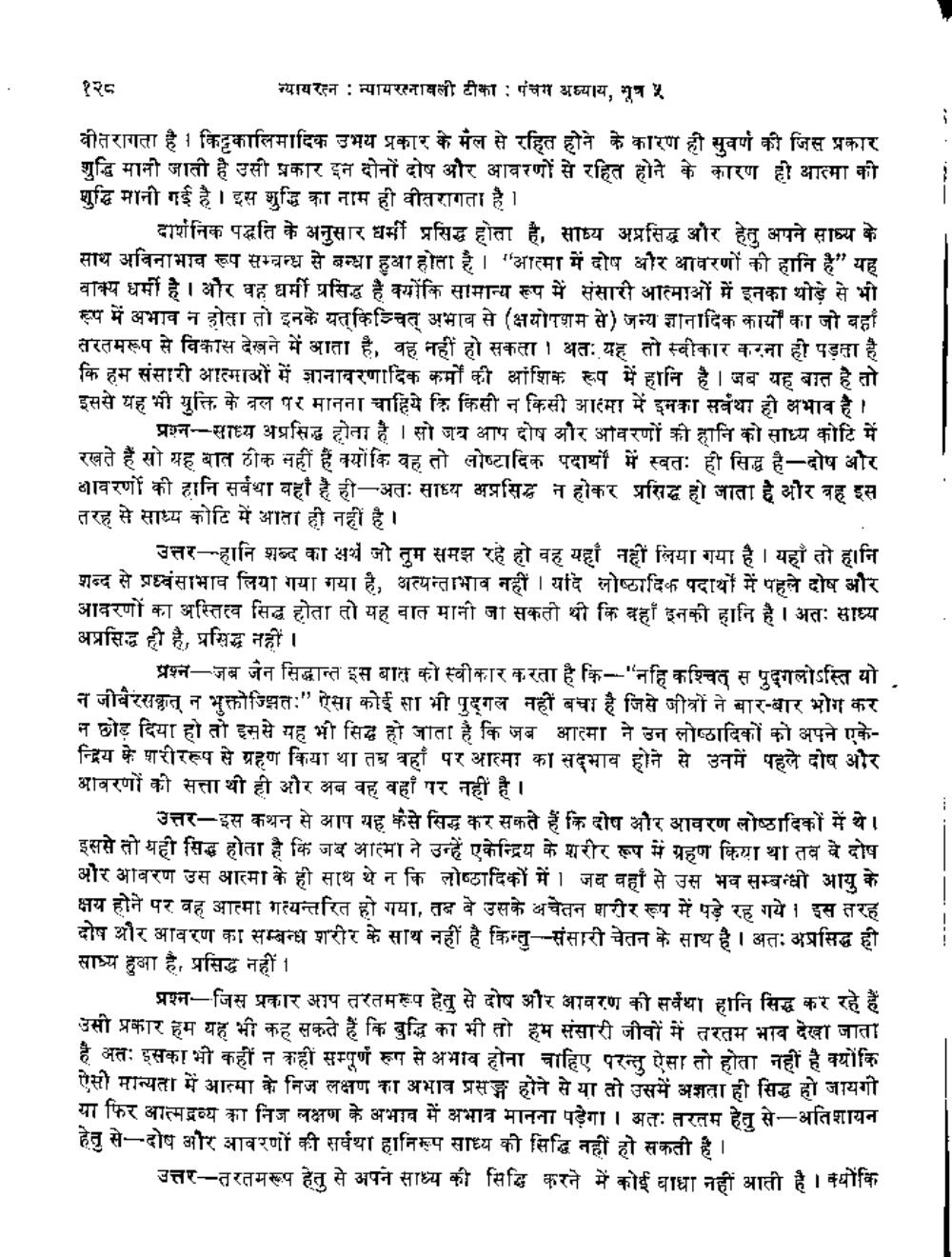________________
१२८
न्यायरत्न : न्यायरत्नावली टीका : पंचग अध्याय, मूत्र ५
वीतरागता है । किट्टकालिमादिक उभय प्रकार के मल से रहित होने के कारण ही सुवर्ण की जिस प्रकार शुद्धि मानी जाती है उसी प्रकार इन दोनों दोष और आवरणों से रहित होने के कारण ही आत्मा की शुद्धि मानी गई है। इस शुद्धि का नाम ही वीतरागता है।
दार्शनिक पद्धति के अनुसार धर्मी प्रसिद्ध होता है, साध्य अप्रसिद्ध और हेतु अपने साध्य के साथ अविनाभाव रूप सम्बन्ध से बन्धा हुआ होता है । "आत्मा में दोष और आवरणों की हानि है" यह वाक्य धर्मी है । और वह धर्मी प्रसिद्ध है क्योंकि सामान्य रूप में संसारी आत्माओं में इनका थोड़े से भी रूप में अभाव न होता तो इनके यत्किञ्चित् अभाब से (क्षयोपशम से) जन्य ज्ञानादिक कार्यों का जो वहाँ तरतमरूप से विकास देखने में आता है, वह नहीं हो सकता। अतः यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि हम संसारी आत्माओं में ज्ञानाबरणादिक कर्मों की आंशिक रूप में हानि है । जब यह बात है तो इससे यह भी युक्ति के बल पर मानना चाहिये कि किसी न किसी आत्मा में इनका सर्वथा है व है।
प्रश्न-साध्य अप्रसिद्ध होता है । सो जब आप दोष और ओवरणों को हानि को साध्य कोटि में रखते हैं सो यह बात ठीक नहीं हैं क्योंकि वह तो लोष्टादिक पदार्थों में स्वतः ही सिद्ध है-दोष और बावरणों की हानि सर्वथा वहाँ है ही-अतः साध्य अप्रसिद्ध न होकर प्रसिद्ध हो जाता है और वह इस तरह से साध्य कोटि में आता ही नहीं है।
उत्तर-हानि शब्द का अर्थ जो तुम समझ रहे हो वह यहाँ नहीं लिया गया है । यहाँ तो हानि शब्द से प्रध्वंसाभाव लिया गया गया है, अत्यन्ताभाव नहीं । यदि लोष्ठादिक पदार्थों में पहले दोष और आवरणों का अस्तित्व सिद्ध होता तो यह बात मानी जा सकती थी कि वहाँ इनकी हानि है । अतः साध्य अप्रसिद्ध ही है, प्रसिद्ध नहीं ।
प्रश्न-जब जैन सिद्धान्त इस बात को स्वीकार करता है कि-"नहि कश्चित् स पुद्गलोऽस्ति यो न जीवरसकृत् न भुक्तोज्झितः" ऐसा कोई सा भी पुद्गल नहीं बचा है जिसे जीवों ने बार-बार भोग कर न छोड़ दिया हो तो इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जब आत्मा ने उन लोष्ठादिकों को अपने एकेन्द्रिय के शरीररूप से ग्रहण किया था तब वहाँ पर आत्मा का सद्भाव होने से उनमें पहले दोष और आवरणों की सत्ता थी ही और अब वह वहाँ पर नहीं है ।
उत्तर-इस कथन से आप यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि दोष और आवरण लोष्ठादिकों में थे। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जब आत्मा ने उन्हें एकेन्द्रिय के शरीर रूप में ग्रहण किया था तव वे दोष और आवरण उस आत्मा के ही साथ थे न कि लोष्ठादिकों में। जब वहाँ से उस भव सम्बन्धी आयु के क्षय होने पर वह आत्मा गत्यन्तरित हो गया, तद वे उसके अचेतन शरीर रूप में पड़े रह गये। इस तरह दोष और आवरण का सम्बन्ध शरीर के साथ नहीं है किन्तु-संसारी चेतन के साथ है । अतः अप्रसिद्ध ही साध्य हुआ है, प्रसिद्ध नहीं।
प्रश्न-जिस प्रकार आप तरतमरूप हेतु से दोष और आवरण की सर्वथा हानि सिद्ध कर रहे हैं उसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि बुद्धि का भी तो हम संसारी जीवों में तरतम भाव देखा जाता है अतः इसका भी कहीं न कहीं सम्पूर्ण रूप से अभाव होना चाहिए परन्तु ऐसा तो होता नहीं है क्योकि ऐसी मान्यता में आत्मा के निज लक्षण का अभाव प्रसङ्ग होने से या तो उसमें अशता ही सिद्ध हो जायगी या फिर आत्मद्रव्य का निज लक्षण के अभाव में अभाव मानना पड़ेगा । अतः तरतम हेतु से-अतिशायन हेतु से-दोष और आवरणों की सर्वथा हानिरूप साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है ।
उत्तर-तरतमरूप हेतु से अपने साध्य की सिद्धि करने में कोई बाधा नहीं आती है। क्योंकि