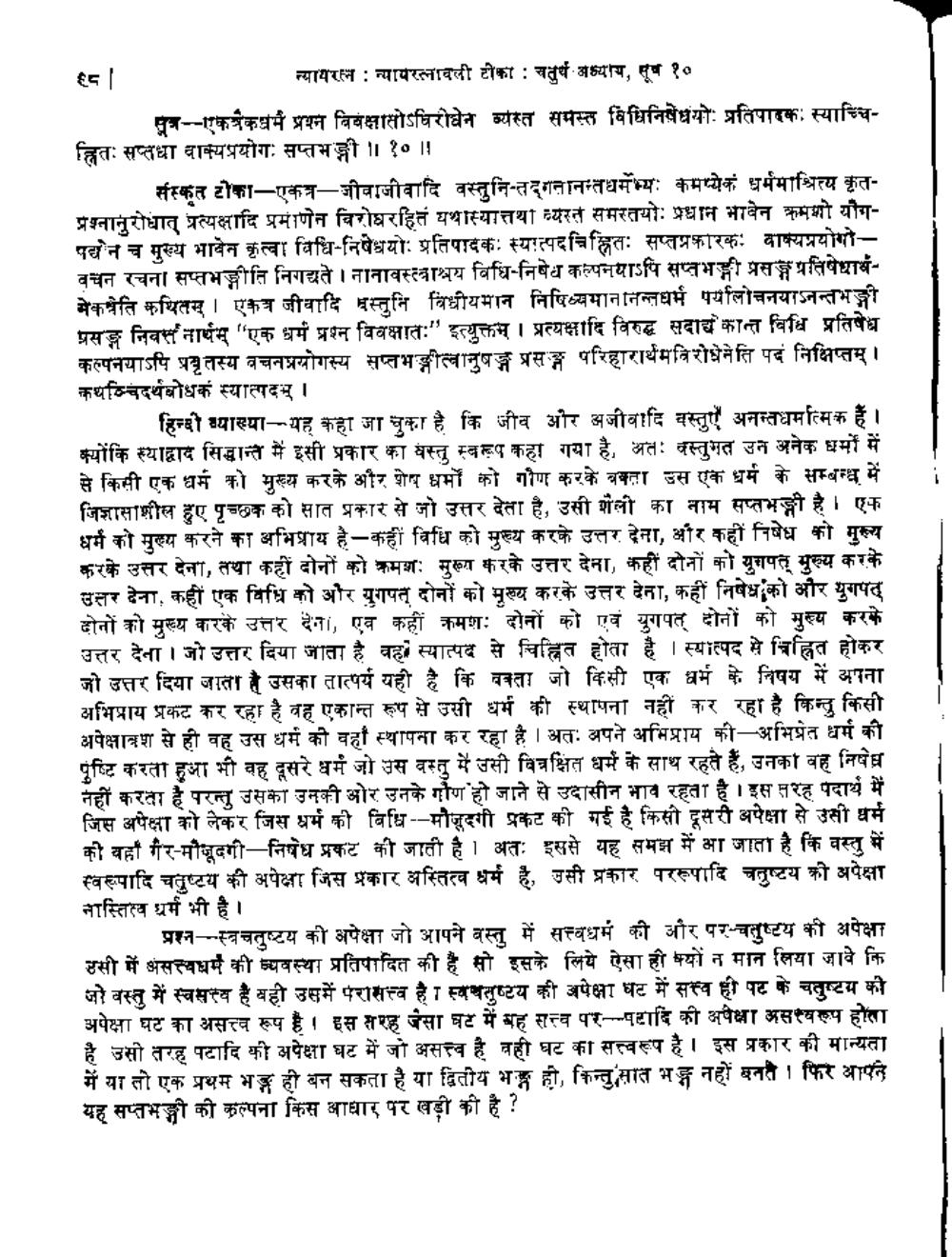________________
१८ |
न्यायरल : न्यायरत्नावली टोका : चतुर्थ अध्याय, सूच १० सूत्र--एकत्रकधर्म प्रश्न विवक्षातोऽधिरोधेन व्यस्त समस्त विधिनिषेधयोः प्रतिपादकः स्याच्चिह्नितः सप्तधा वाक्यप्रयोगः सप्तभङ्गी ।। १० ।।
संस्कृत टोका-एकत्र-जीवाजीवादि वस्तुनि-तद्गनानन्तधर्मेभ्यः कमध्येकं धर्ममाश्रित्य कृतप्रश्नानुरोधात् प्रत्यक्षादि प्रमाणेन विरोघरहितं यथास्यात्तथा व्यस्त समरतयोः प्रधान भावेन क्रमशो योगपद्य न च मुख्य भावेन कृत्वा विधि-निषेधयोः प्रतिपादकः स्यात्पदचिह्नितः सप्तप्रकारकः वाक्यप्रयोगोवचन रचना सप्तभङ्गीति निगद्यते । नानावस्वाश्रय विधि-निषेध कल्पनयाऽपि सप्तभङ्गी प्रसङ्गप्रतिषेधार्थमेकवेति कथितम् । एकत्र जीवादि वस्तुनि विधीयमान निषिध्यमानानन्तधर्म पर्यालोचनयाऽनन्तभङ्गी प्रसङ्ग निवसं नार्थम् "एक धर्म प्रश्न विवक्षातः" इत्युक्तम् । प्रत्यक्षादि विरुद्ध सदायकान्त विधि प्रतिषेध कल्पनयाऽपि प्रवृतस्य वचनप्रयोगस्य सप्तभङ्गीत्वानुषङ्ग प्रसङ्ग परिहारार्थमविरोधेनेति पदं निक्षिप्तम् । कथञ्चिदर्थबोधकं स्यात्पदम् ।
हिन्दी व्याख्या-यह कहा जा चुका है कि जीव और अजीवादि वस्तुएँ अनन्तधर्मात्मक हैं। क्योंकि स्याद्वाद सिद्धान्त मैं इसी प्रकार का वस्तु स्वरूप कहा गया है, अतः वस्तुमत उन अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य करके और शेष धर्मों को गौण करके बक्ता उस एक धर्म के सम्बन्ध में जिज्ञासाशील हुए पृच्छक को सात प्रकार से जो उसर देता है, उसी शैली का नाम सप्तभङ्गी है। एक धर्म को मुख्य करने का अभिप्राय है-कहीं विधि को मुख्य करके उत्तर देना, और कहीं निषेध को मुख्य करके उसर देना, तथा कहीं दोनों को क्रमशः मुख्य करके उत्तर देना, कहीं दोनों को युगपत् मुख्य करके उत्तर देना, कहीं एक विधि को और युगपत् दोनों को मुख्य करके उत्तर देना, कहीं निषेधको और युगपद दोनों को मुख्य करके उत्तर देना, एव कहीं क्रमशः दोनों को एवं युगपत् दोनों को मुख्य करके उत्तर देना । जो उत्तर दिया जाता है वहीं स्यात्पद से चिह्नित होता है । स्यात्पद से चिह्नित होकर जो उत्तर दिया जाता है उसका तात्पर्य यही है कि वक्ता जो किसी एक धर्म के विषय में अपना अभिप्राय प्रकट कर रहा है वह एकान्त रूप से उसी धर्म की स्थापना नहीं कर रहा है किन्तु किसी अपेक्षाक्श से ही वह उस धर्म को वहाँ स्थापना कर रहा है । अतः अपने अभिप्राय की-अभिप्रेत धर्म की पुष्टि करता हुआ भी वह दूसरे धर्म जो उस वस्तु में उसी विवक्षित धर्म के साथ रहते हैं, उनका वह निषेध नहीं करता है परन्तु उसका उनकी ओर उनके गौण हो जाने से उदासीन भाव रहता है । इस सरह पदार्थ में जिस अपेक्षा को लेकर जिस धर्म की विधि --मौजूदगी प्रकट की गई है किसी दूसरी अपेक्षा से उसी धर्म को वहाँ गैर-मौजूदगी-निषेध प्रकट की जाती है । अतः इससे यह समझ में आ जाता है कि वस्तु में स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा जिस प्रकार अस्तित्व धर्म है, उसी प्रकार पररूपादि चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व धर्म भी है।
प्रश्न-स्त्रचतुष्टय की अपेक्षा जो आपने वस्तु में सत्त्वधर्म की और पर चतुष्टय की अपेक्षा उसी में असत्त्वधर्म की व्यवस्था प्रतिपादित की है सो इसके लिये ऐसा ही क्यों न मान लिया जावे कि जरे वस्तु में स्वसत्य है वही उसमें परासत्व है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा घट में सत्त्व ही पट के चतुष्टय की अपेक्षा घट का असत्त्व रूप है। इस सरह जैसा घट में बह सत्व पर पटादि की अपेक्षा असत्वरूप होता है उसी तरह पटादि की अपेक्षा घट में जो असत्त्व है वही घट का सत्त्वरूप है। इस प्रकार की मान्यता में या तो एक प्रथम भङ्ग ही बन सकता है या द्वितीय भङ्ग हो, किन्तु सात भङ्ग नहीं बनते । फिर आपने यह सप्तभङ्गी की कल्पना किस आधार पर खड़ी की है ?