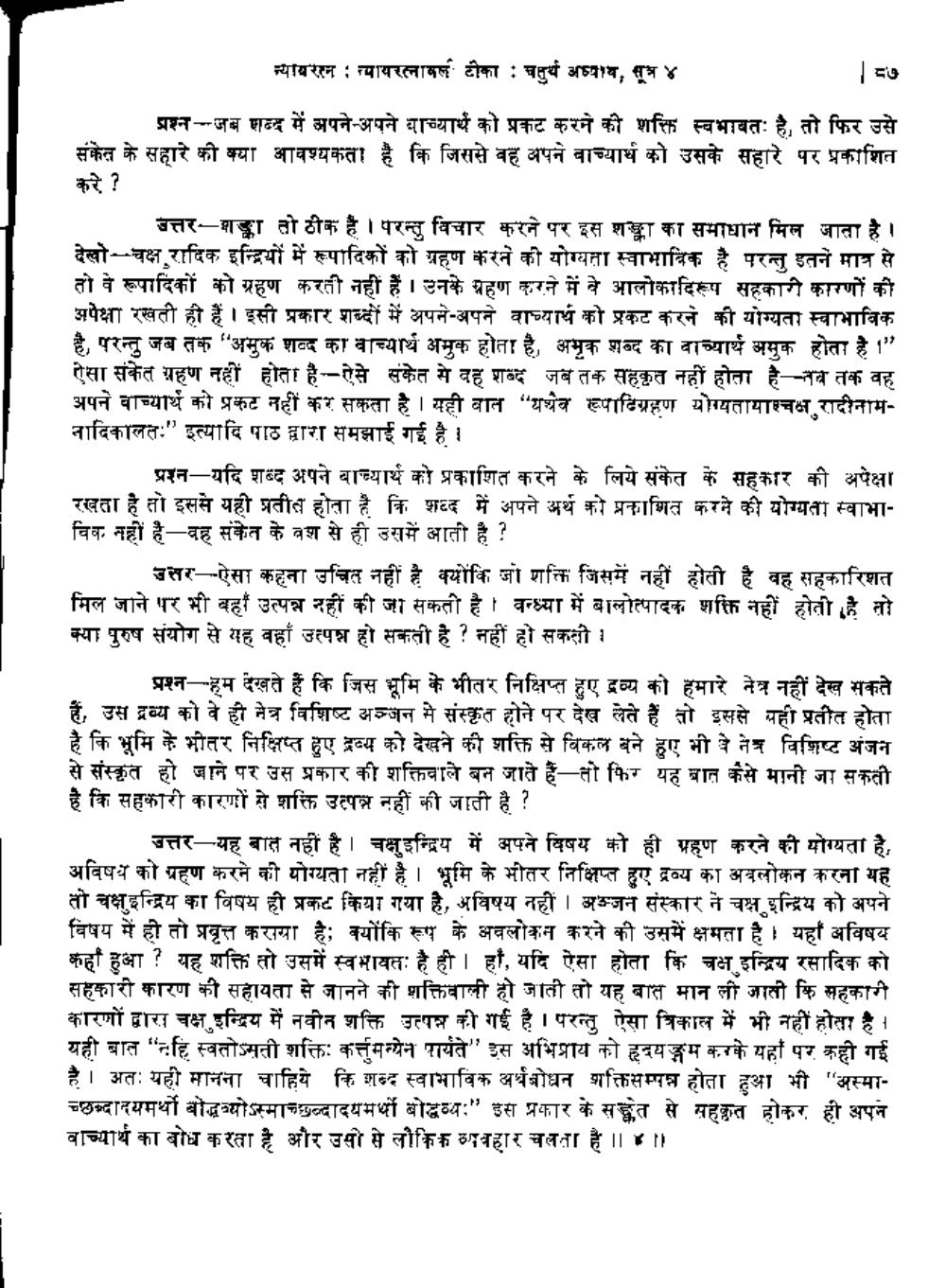________________
न्यायरत्न : यायरत्नावल टीका : चतुर्थ अध्याय, सूत्र ४
प्रश्न- जब शब्द में अपने-अपने बाच्यार्य को प्रकट करने की शक्ति स्वभावतः है, तो फिर उसे संकेत के सहारे की क्या आवश्यकता है कि जिससे वह अपने वाच्यार्थ को उसके सहारे पर प्रकाशित
करे?
उत्तर-शङ्का तो ठीक है । परन्तु विचार करने पर इस शङ्का का समाधान मिल जाता है। देखो-चक्ष रादिक इन्द्रियों में रूपादिकों को ग्रहण करने की योग्यता स्वाभाविक है परन्तु इतने मात्र से तो वे रूपादिकों को ग्रहण करती नहीं हैं । उनके ग्रहण करने में वे आलोकादिरूप सहकारी कारणों की अपेक्षा रखती ही हैं। इसी प्रकार शब्दों में अपने-अपने वाच्यार्थ को प्रकट करने की योग्यता स्वाभाविक है, परन्तु जब तक "अमुक शब्द का वाच्यार्थ अमुक होता है, अमृक शब्द का वाच्यार्थ अमुक होता है।" ऐसा संकेत ग्रहण नहीं होता है-ऐसे संकेत से वह शब्द जब तक सहकृत नहीं होता है जब तक वह अपने वाच्यार्थ को प्रकट नहीं कर सकता है । यही बात "यौव रूपादिग्रहण योग्यतायाश्चम रादीनामनादिकालतः" इत्यादि पाठ द्वारा समझाई गई है।
प्रश्न-यदि शब्द अपने बाच्यार्थ को प्रकाशित करने के लिये संकेत के सहकार की अपेक्षा रखता है तो इससे यही प्रतीत होता है कि शब्द में अपने अर्थ को प्रकाशित करने की योग्यता स्वाभाविव नहीं है-वह संकेत के वश से ही उसमें आती है ?
उसर-ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि जो शक्ति जिसमें नहीं होती है वह सहकारिशत मिल जाने पर भी वहाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती है । वन्ध्या में बालोत्पादक शक्ति नहीं होती है तो क्या पुरुष संयोग से यह वहाँ उत्पन्न हो सकती है ? नहीं हो सकती।
प्रश्न- हम देखते हैं कि जिस भूमि के भीतर निक्षिप्त हुए द्रव्य को हमारे नेत्र नहीं देख सकते हैं, उस द्रव्य को वे ही नेत्र विशिष्ट अजन मे संस्कृत होने पर देख लेते हैं तो इससे यही प्रतीत होता है कि भूमि के भीतर निक्षिप्त हुए द्रव्य को देखने की शक्ति से विकल बने हुए भी वे नेत्र विशिष्ट अंजन से संस्कृत हो जाने पर उस प्रकार की शक्तिवाले बन जाते हैं तो फिर यह बात कैसे मानी जा सकती है कि सहकारी कारणों से शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती है ?
उत्तर-यह बात नहीं है। चाइन्द्रिय में अपने विषय को ही ग्रहण करने की योग्यता है, अविषय को ग्रहण करने की योग्यता नहीं है । भूमि के भीतर निक्षिप्त हुए द्रव्य का अवलोकन करना यह तो चाइन्द्रिय का विषय ही प्रकट किया गया है, अविष्य नहीं । अञ्जन संस्कार ने चक्ष इन्द्रिय को अपने विषय में ही तो प्रवृत्त कराया है; क्योंकि रूप के अवलोकन करने की उसमें क्षमता है। यहाँ अविषय कहाँ हुआ? यह शक्ति तो उसमें स्वभावतः है ही। हो, यदि ऐसा होता कि चक्ष इन्द्रिय रसादिक को सहकारी कारण की सहायता से जानने की शक्तिवाली हो जाती तो यह बात मान ली जाती कि सहकारी कारणों द्वारा चक्ष इन्द्रिय में नवीन शक्ति उत्पन्न की गई है । परन्तु ऐसा त्रिकाल में भी नहीं होता है। यही बाल "वहि स्वतोऽमती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते" इस अभिप्राय को हृदयङ्गम करके यहाँ पर कही गई है। अतः यही मानना चाहिये कि शब्द स्वाभाविक अर्थबोधन शक्तिसम्पन्न होता हुआ भी "अस्माच्छन्दादयमर्थो बोद्धयोऽस्मान्छन्दादयमों बोद्धव्यः" इस प्रकार के सङ्केत से सहकृत होकर ही अपने वाच्यार्थ का बोध करता है और उसी से लौकिक पवहार चलता है ।। ४ ।।