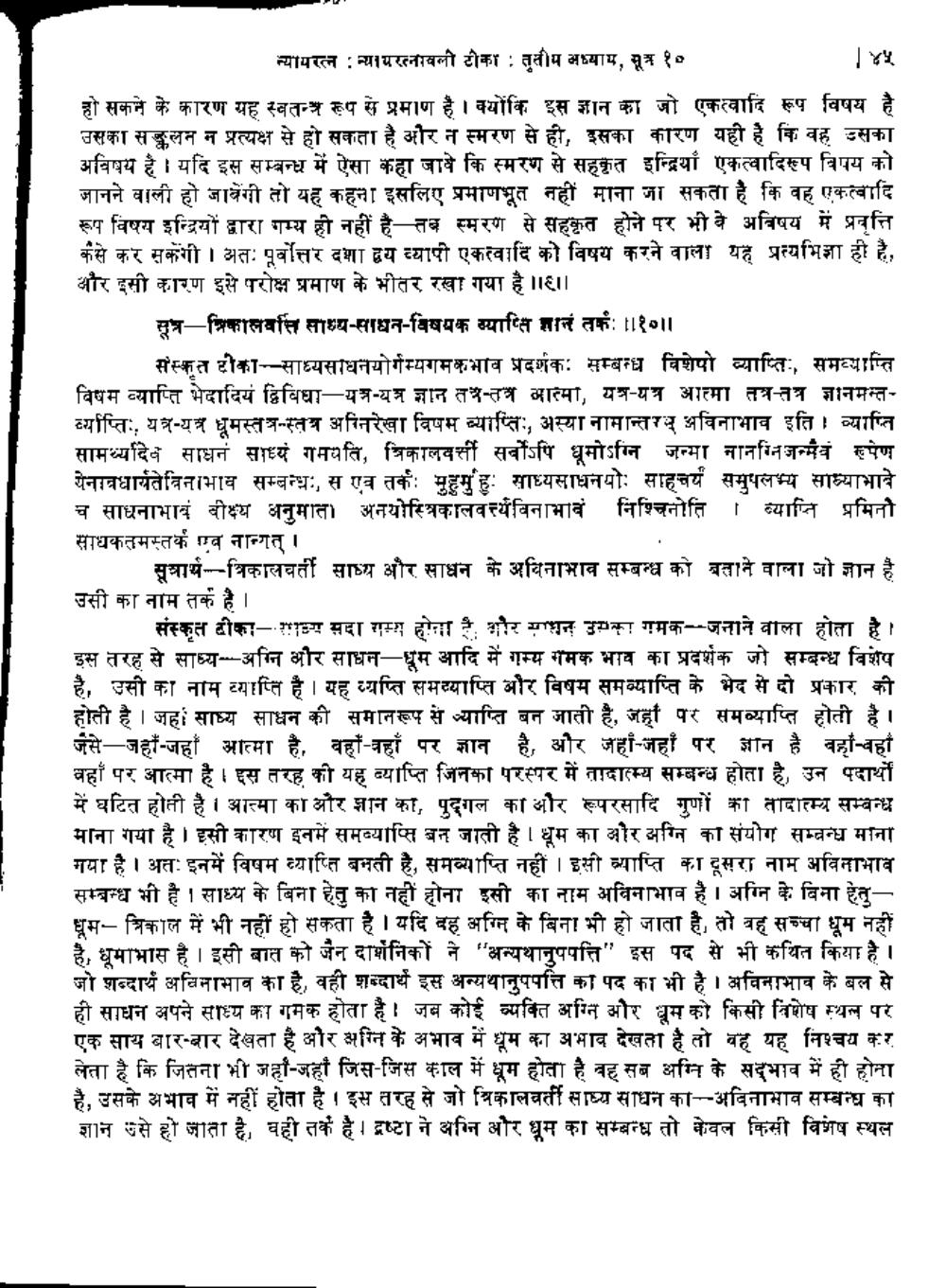________________
न्यायरत्न : न्यायरत्नावली टीका : तृतीय अध्याय, सूत्र १०
|४५ हो सकने के कारण यह स्वतन्त्र रूप से प्रमाण है । क्योंकि इस ज्ञान का जो एकत्वादि रूप विषय है उसका सङ्कलन न प्रत्यक्ष से हो सकता है और न स्मरण से ही, इसका कारण यही है कि वह उसका अविषय है। यदि इस सम्बन्ध में ऐसा कहा जाये कि स्मरण से सहकृत इन्द्रियाँ एकत्वादिरूप विषय को जानने वाली हो जावेगी तो यह कहना इसलिए प्रमाणभूत नहीं माना जा सकता है कि वह एकत्वादि रूप विषय इन्द्रियों द्वारा गम्य ही नहीं है तब स्मरण से सहकृत होने पर भी वे अविषय में प्रवृत्ति कसे कर सकेंगी। अतः पूर्वोत्तर दशा द्वय व्यापी एकत्वादि को विषय करने वाला यह प्रत्यभिज्ञा ही है, और इसी कारण इसे परोक्ष प्रमाण के भीतर रखा गया है ।।६।।
सूत्र-त्रिकालवति साध्य-साधन-विषयक व्याप्ति शान तकः ।।१०।।
संस्कृत टीका-साध्यसाधनयोर्गम्यगमकभाव प्रदर्शकः सम्बन्ध विशेपो व्याप्तिः, समव्याप्ति विषम व्याप्ति भेदादियं द्विविधा-यत्र-यत्र ज्ञान तत्र-तत्र आत्मा, यत्र-यत्र आत्मा तत्र-तत्र ज्ञानमन्तयाप्तिः, यत्र-यत्र धूमस्तत्र-स्तत्र अग्निरेखा विषम व्याप्तिः, अस्या नामान्तर अविनाभाव इति । व्याप्ति सामर्थ्यादेव साधनं साध्यं गमयति, त्रिकालवी सर्वोऽपि धूमोऽग्नि जन्मा नानग्निजन्मवं रूपेण येनाबधार्यतेविनाभाव सम्बन्धः, स एव तर्क: मुहमुहुः साध्यसाधनयोः साहचर्यं समुपलभ्य साध्याभावे च साधनाभावं वीक्ष्य अनुमाता अनयोस्त्रिकालवयंविनाभावे निश्चिनोति । व्याप्ति प्रमिनो साधकतमस्तर्क एब नान्गत् ।
सूत्रार्य-त्रिकालवी साध्य और साधन के अविनाभाव सम्बन्ध को बताने वाला जो ज्ञान है उसी का नाम तक है।
संस्कृत टीका-साध्य सदा गम्य होता है. और साधन उसका गमक-जनाने वाला होता है। इस तरह से साध्य-अग्नि और साधन-धूम आदि में गम्य गमक भाव का प्रदर्शक जो सम्बन्ध विशेष है, उसी का नाम व्याप्ति है। यह व्यप्ति समयाप्ति और विषम समन्याप्ति के भेद से दो प्रकार की होती है । जहाँ साध्य साधन की समानरूप से ज्याप्ति बन जाती है, जहां पर समव्याप्ति होती है। जैसे-जहाँ-जहाँ आत्मा है, वहाँ-वहाँ पर ज्ञान है, और जहाँ-जहाँ पर ज्ञान है वहां-वहाँ वहाँ पर आत्मा है। इस तरह की यह व्याप्ति जिनका परस्पर में तादात्म्य सम्बन्ध होता है, उन पदार्थों में घटित होती है । आत्मा का और ज्ञान का, पुद्गल का और रूपरसादि गुणों का तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है । इसी कारण इनमें समव्याप्सि बन जाती है । धूम का और अग्नि का संयोग सम्बन्ध माना गया है। अतः इनमें विषम व्याप्ति बनती है, समव्याप्ति नहीं । इसी व्याप्ति का दूसरा नाम अविनाभाव सम्बन्ध भी है । साध्य के बिना हेतु का नहीं होना इसी का नाम अविनाभाव है। अग्नि के बिना हेतुधूम- त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है । यदि वह अग्नि के बिना भी हो जाता है, तो वह सच्चा धूम नहीं है, धूमाभास है । इसी बात को जैन दार्शनिकों ने "अन्यथानुपपत्ति" इस पद से भी कथित किया है । जो शब्दार्थ अविनाभाव का है, वही शब्दार्थ इस अन्यथानुपपत्ति का पद का भी है। अविनाभाव के बल से ही साधन अपने साध्य का गमक होता है। जब कोई व्यक्ति अग्नि और धूम को किसी विशेष स्थल पर एक साथ बार-बार देखता है और अग्नि के अभाव में धूम का अभाव देखता है तो वह यह निश्चय कर लेता है कि जितना भी जहाँ-जहाँ जिस-जिस काल में धूम होता है वह सब अनि के सद्भाव में ही होना है. उसके अभाव में नहीं होता है। इस तरह से जो त्रिकालवर्ती साध्य साधन का अविनाभाव सम्बन्ध का ज्ञान उसे हो जाता है, वही तर्क है । द्रष्टा ने अग्नि और धूम का सम्बन्ध तो केवल किसी विशेष स्थल