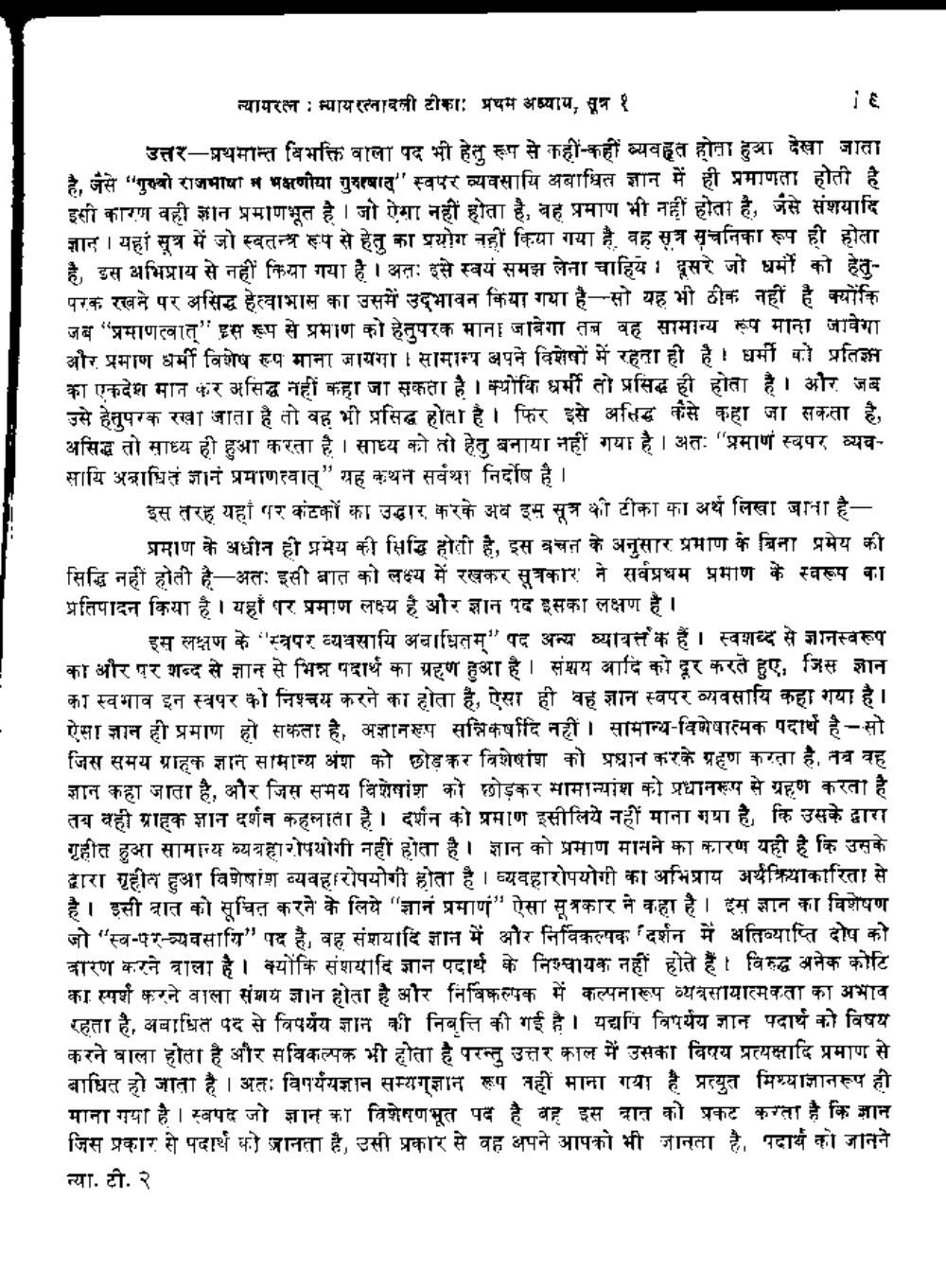________________
न्यायरल : न्याय रत्नाबली टीकाः प्रथम अध्याय, सत्र १
उत्तर-प्रथमान्त विभक्ति वाला पद भी हेतु रूप से कहीं-कहीं व्यवहृत होता हुआ देखा जाता है, जैसे "गुल्यो राजभाषा न भक्षणीया गुरुवात्" स्वपर व्यवसायि अबाधित ज्ञान में ही प्रमाणता होती है इसी कारण वही ज्ञान प्रमाणभूत है । जो ऐमा नहीं होता है, वह प्रमाण भी नहीं होता है, जैसे संशयादि ज्ञान । यहाँ सूत्र में जो स्वतन्त्र रूप से हेतु का प्रयोग नहीं किया गया है. वह सूत्र सूचनिका रूप ही होता है, इस अभिप्राय से नहीं किया गया है । अतः इसे स्वयं समझ लेना चाहिय। दूसरे जो धर्मों को हेतुपरक रखने पर असिद्ध हेत्वाभास का उसमें उद्भावन किया गया है-सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जब "प्रमाणत्वात्" इस रूप से प्रमाण को हेतुपरक माना जाबेगा तब वह सामान्य रूप माना जावेगा और प्रमाण धर्मी विशेष रूप माना जायगा । सामान्य अपने विशेषों में रहता ही है। धर्मी पो प्रतिज्ञा का एकदेश मानकर असिद्ध नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि धर्मी तो प्रसिद्ध ही होता है। और जब उसे हेतुपरक रखा जाता है तो वह भी प्रसिद्ध होता है। फिर इसे असिद्ध कैसे कहा जा सकता है, असिद्ध तो माध्य ही हुआ करता है । साध्य को तो हेतु बनाया नहीं गया है । अतः "प्रमाणं स्वपर व्यवसायि अबाधितं ज्ञानं प्रमाणत्वात्" यह कथन सर्वथा निर्दोष है ।
इस तरह यहां पर कंटकों का उद्धार करके अब इस सूत्र की टीका का अर्थ लिखा जाना है
प्रमाण के अधीन ही प्रमेय की सिद्धि होती है, इस वचन के अनुसार प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है अतः इसी बात को लक्ष्य में रखकर सुत्रकार ने सर्वप्रथम प्रमाण के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर प्रमाण लक्ष्य है और ज्ञान पद इसका लक्षण है ।
इस लक्षण के "स्वपर व्यवसायि अबाधितम्" पद अन्य व्यावर्त के हैं। स्वशब्द से ज्ञानस्वरूप का और पर शब्द से ज्ञान से भिन्न पदार्थ का ग्रहण हुआ है। संशय आदि को दूर करते हुए, जिस ज्ञान का स्वभाव इन स्वपर को निश्चय करने का होता है, ऐसा ही वह ज्ञान स्वपर व्यवसायि कहा गया है। ऐसा ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, अज्ञानरूप सन्निकर्षादि नहीं। सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ है-सो जिस समय ग्राहक ज्ञान सामान्य अंश को छोड़कर विशेषांश को प्रधान करके ग्रहण करता है, तब वह ज्ञान कहा जाता है, और जिस समय विशेषांश को छोड़कर मामान्यांश को प्रधानरूप से ग्रहण करता है तब वही ग्राहक ज्ञान दर्शन कहलाता है। दर्शन को प्रमाण इसीलिये नहीं माना गया है, कि उसके द्वारा गृहीत हुआ सामान्य व्यवहारोपयोगी नहीं होता है। ज्ञान को प्रमाण मानने का कारण यही है कि उसके द्वारा गृहीव हुआ विशेषांश व्यवहारोपयोगी होता है । व्यवहारोपयोगी का अभिप्राय अर्थक्रियाकारिता से है। इसी बात को सूचित करने के लिये "ज्ञानं प्रमाण" ऐसा सूत्रकार ने कहा है। इस ज्ञान का विशेषण जो "स्व-पर-व्यवसायि" पद है, वह संशयादि ज्ञान में और निर्विकल्पक 'दर्शन में अतिव्याप्ति दोष को वारण करने वाला है। क्योंकि संशयादि ज्ञान पदार्थ के निश्चायक नहीं होते हैं। विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाला संशय ज्ञान होता है और निर्विकल्पक में कल्पनारूप व्यवसायात्मकता का अभाव रहता है, अबाधित पद से विपर्यय ज्ञान की निबत्ति की गई है। यद्यपि विपर्यय ज्ञान पदार्थ को विषय करने वाला होता है और सविकल्पक भी होता है परन्तु उत्तर काल में उसका विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित हो जाता है । अतः विपर्ययज्ञान सम्यग्ज्ञान रूप नहीं माना गया है प्रत्युत मिथ्याज्ञानरूप ही माना गया है । स्वपद जो ज्ञान का विशेषणभूत पद है वह इस बात को प्रकट करता है कि ज्ञान जिस प्रकार से पदार्थ को जानता है, उसी प्रकार से वह अपने आपको भी जानता है, पदार्थ को जानने न्या. टी.२