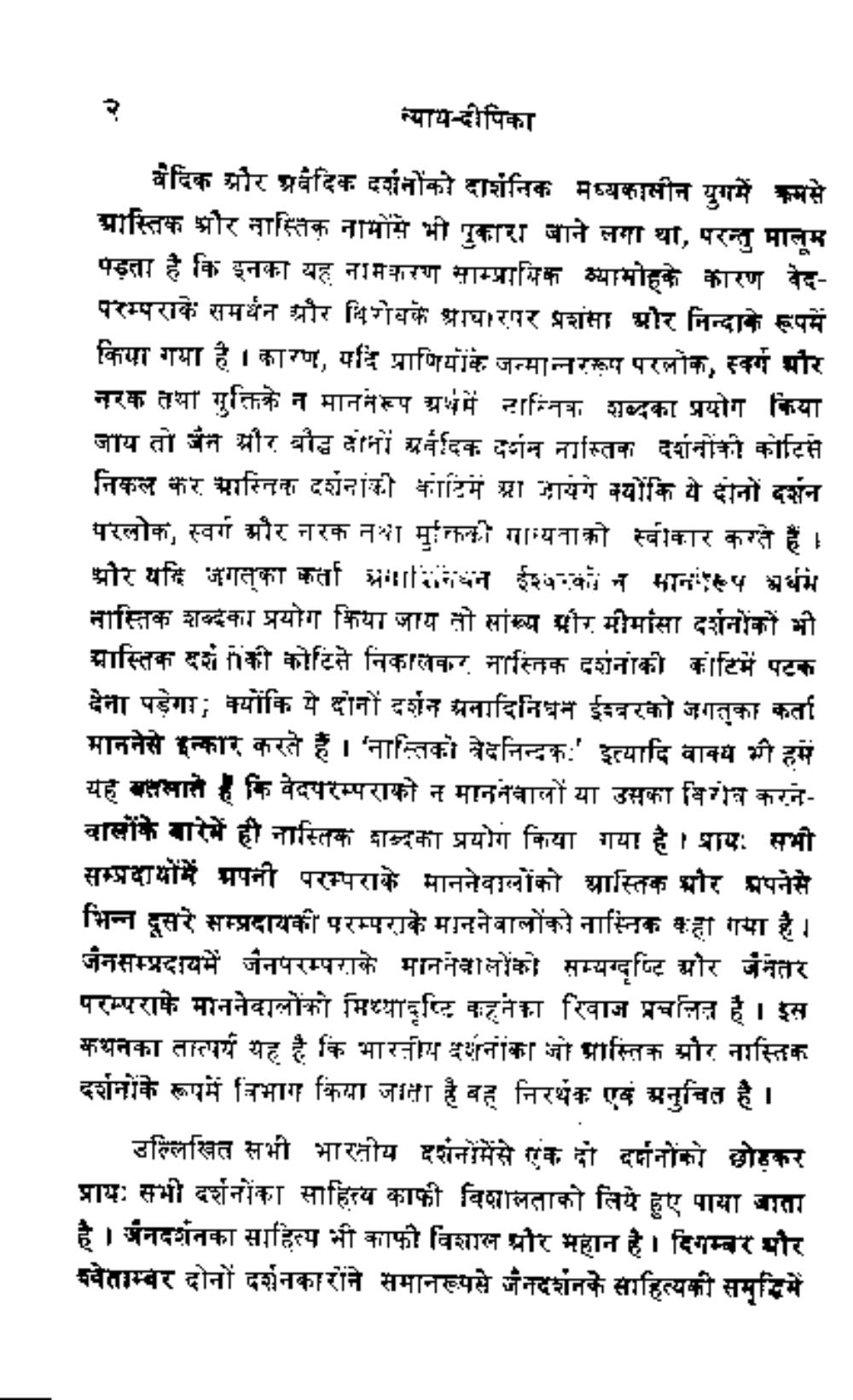________________
न्याय-दीपिका
वैदिक और प्रवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें कमसे आस्तिक और नास्तिक नामोंसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम पड़ता है कि इनका यह नामकरण साम्प्राषिक श्यामोहके कारण वेदपरम्पराके समर्थन और विगेवके अाघारपर प्रशंसा और निन्दाके रूपमें किया गया है । कारण, पदि प्राणियोंके जन्मानररूप परलोक, स्वर्ग मोर नरक तथा मुक्तिके न माननरूप अर्थ में नाम्नित्र शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन और बौद्ध दोनों अदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिस निकल कर आग्निक दर्शनांकी काटिम प्रा डायगे क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक, स्वर्ग और नरक नया मुक्तकी गायताको स्वीकार करते हैं । और यदि जगत्का कर्ता मानियन ईश्वको न मानरूप अर्धभ नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मीमांसा दर्शनोंकों भी मास्तिक दर्शकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनांकी कोटिमें पटक देना पड़ेगा; क्योंकि ये दोनों दर्शन अनादिनिधन ईश्वरको जगतका कर्ता माननेसे इन्कार करते हैं । 'नास्तिको वेदनिन्दकः' इत्यादि वाक्य भी हम यह बतलाते है कि वेदपरम्पराको न माननेवालों या उसका विरोव करनवालों के बारेमें ही नास्तिक छान्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी सम्प्रदायोंमें अपनी परम्पराके माननेवालोंको प्रास्तिक और अपनेसे भिन्न दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके मानने वालोंको नास्निक कहा गया है। जनसम्प्रदायमें जैनपरम्पराके माननेवालोंको सम्यग्दृष्टि और जनतर परम्पराफे माननेवालोंको मिथ्यावृष्टि कहने का रिवाज प्रचलित है । इस कथनका तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शनाका जो प्रास्तिक और नास्तिक दर्शनोंके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरर्थक एवं अनुचित है।
उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनों में से एक दो दर्शनोंको छोड़कर प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताको लिये हुए पाया जाता है । अनदर्शनका साहित्य भी काफी विशाल और महान है। दिगम्बर मोर श्वेताम्बर दोनों दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यको समृद्धिमें