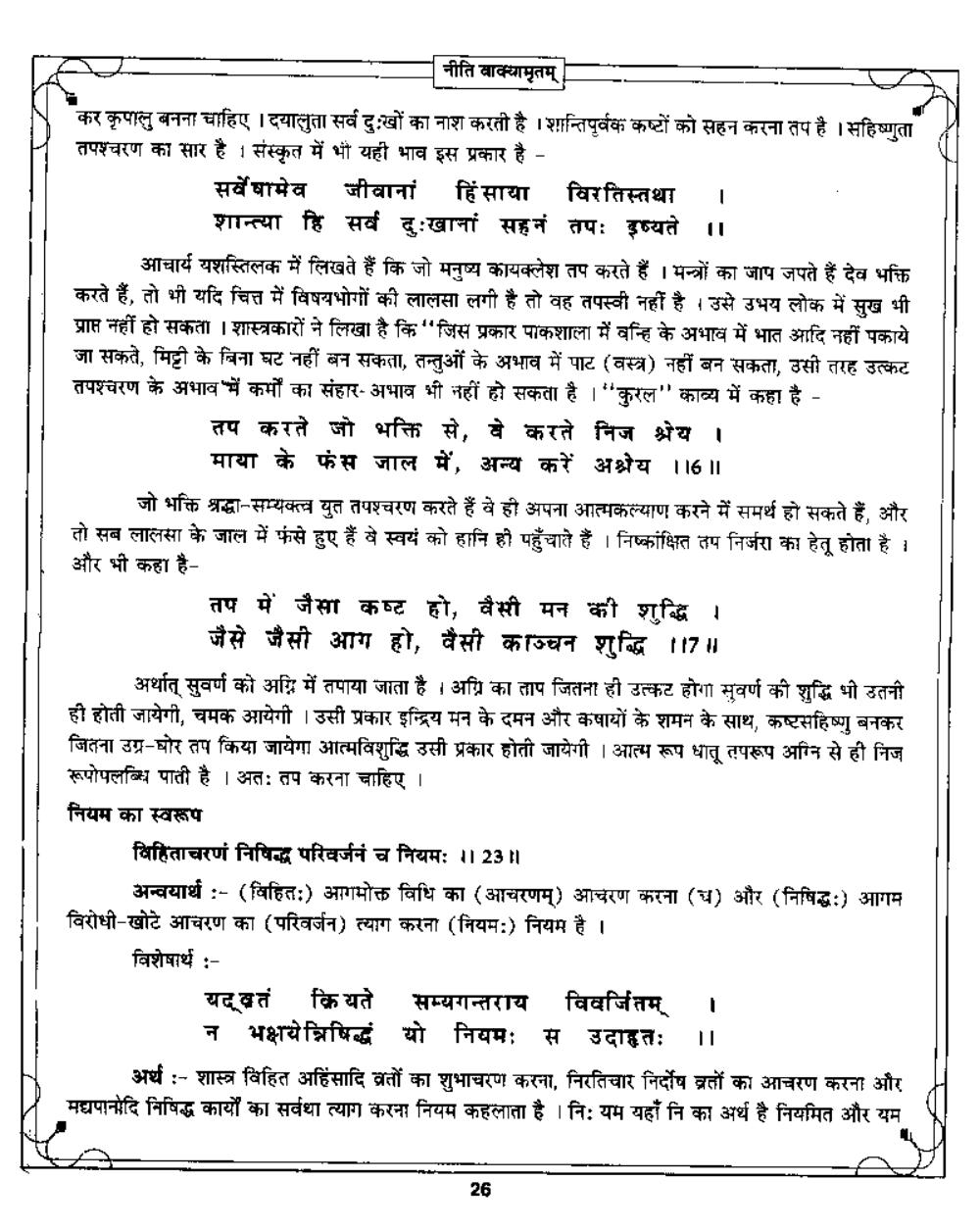________________
नीति वाक्यामृतम् ।
कर कृपालु बनना चाहिए । दयालुता सर्व दुःखों का नाश करती है । शान्तिपूर्वक कष्टों को सहन करना तप है । सहिष्णुता , तपश्चरण का सार है । संस्कृत में भी यही भाव इस प्रकार है -
सर्वेषामेव जीवानां हिंसाया विरतिस्तथा ।
शान्त्या हि सर्व दुःखानां सहनं तपः इष्यते ।। आचार्य यशस्तिलक में लिखते हैं कि जो मनुष्य कायक्लेश तप करते हैं । मन्त्रों का जाप जपते हैं देव भक्ति करते हैं, तो भी यदि चित्त में विषयभोगों की लालसा लगी है तो वह तपस्वी नहीं है । उसे उभय लोक में सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता । शास्त्रकारों ने लिखा है कि "जिस प्रकार पाकशाला में वन्हि के अभाव में भात आदि नहीं पकाये जा सकते, मिट्टी के बिना घट नहीं बन सकता, तन्तुओं के अभाव में पाट (वस्त्र) नहीं बन सकता, उसी तरह उत्कट तपश्चरण के अभाव में कर्मों का संहार- अभाव भी नहीं हो सकता है । "कुरल'' काव्य में कहा है -
तप करते जो भक्ति से, वे करते निज श्रेय ।
माया के फंस जाल में, अन्य करें अश्रेय ।।6॥ जो भक्ति श्रद्धा-सम्यक्त्व युत तपश्चरण करते हैं वे ही अपना आत्मकल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं, और तो सब लालसा के जाल में फंसे हुए हैं वे स्वयं को हानि ही पहुँचाते हैं । निष्कांक्षित तप निर्जरा का हेतू होता है। और भी कहा है
तप में जैसा कष्ट हो, वैसी मन की शुद्धि ।
जैसे जैसी आग हो, वैसी काञ्चन शुद्धि ।।7।। अर्थात् सुवर्ण को अग्नि में तपाया जाता है । अग्नि का ताप जितना ही उत्कट होगा सुवर्ण की शुद्धि भी उतनी ही होती जायेगी, चमक आयेगी । उसी प्रकार इन्द्रिय मन के दमन और कषायों के शमन के साथ, कष्टसहिष्णु बनकर जितना उग्र-घोर तप किया जायेगा आत्मविशुद्धि उसी प्रकार होती जायेगी । आत्म रूप धातू तपरूप अग्नि से ही निज रूपोपलब्धि पाती है । अत: तप करना चाहिए । नियम का स्वरूप
विहिताचरणं निषिद्ध परिवर्जनं च नियमः ॥23॥
अन्वयार्थ :- (विहितः) आगमोक्त विधि का (आचरणम्) आचरण करना (च) और (निषिद्धः) आगम विरोधी-खोटे आचरण का (परिवर्जन) त्याग करना (नियम:) नियम है । विशेषार्थ :
यद्वतं कि यते सम्यगन्तराय विवर्जितम् ।
न भक्षये निषिद्धं यो नियमः स उदाहृतः ।। अर्थ :- शास्त्र विहित अहिंसादि व्रतों का शुभाचरण करना, निरतिचार निर्दोष व्रतों का आचरण करना और H मद्यपानोदि निषिद्ध कार्यों का सर्वथा त्याग करना नियम कहलाता है । नि: यम यहाँ नि का अर्थ है नियमित और यम ५
26