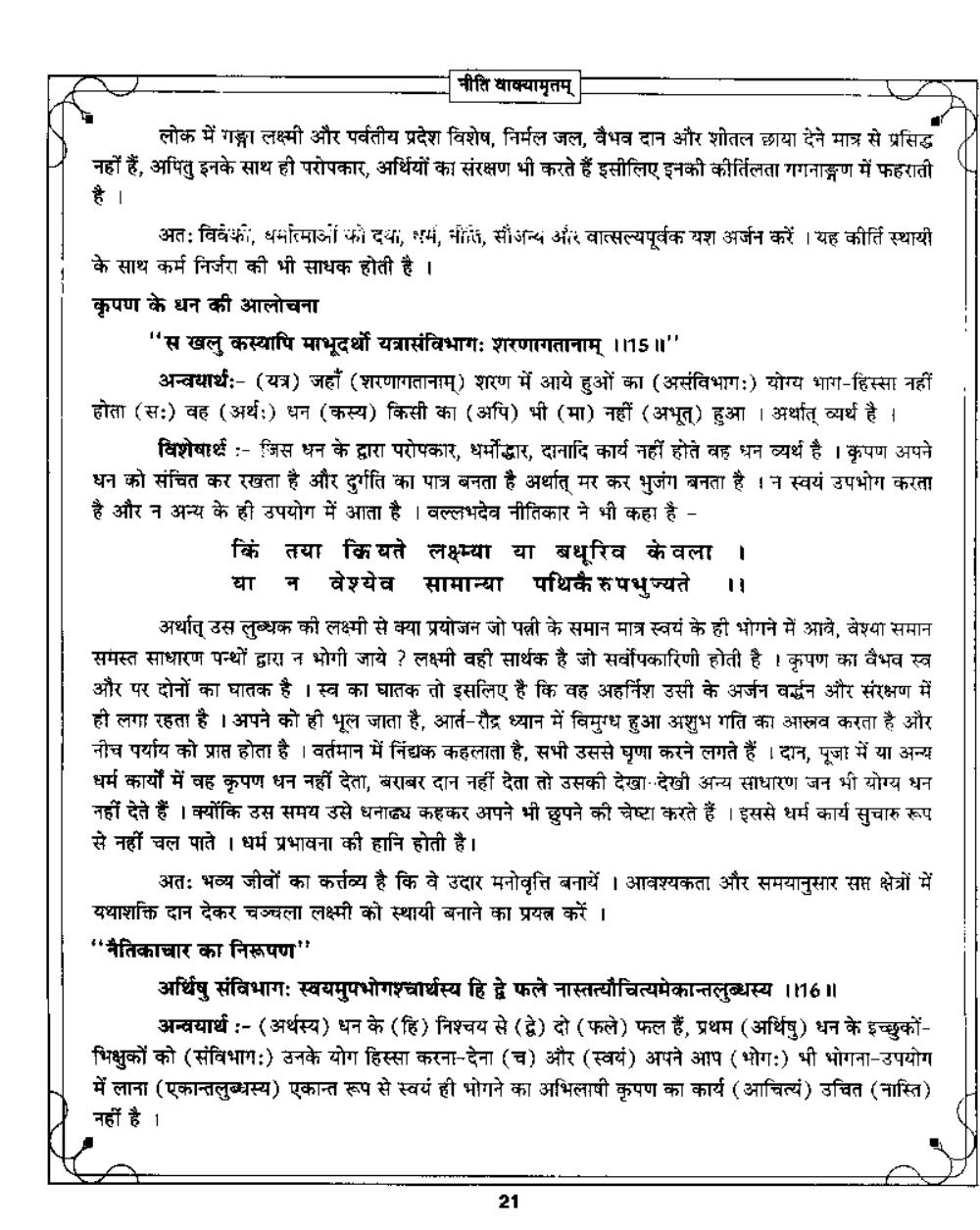________________
नीति वाक्यामृतम्
लोक में गङ्गा लक्ष्मी और पर्वतीय प्रदेश विशेष, निर्मल जल, वैभव दान और शीतल छाया देने मात्र से प्रसिद्ध नहीं हैं, अपितु इनके साथ ही परोपकार, अर्थियों का संरक्षण भी करते हैं इसीलिए इनकी कीर्तिलता गगनाङ्गण में फहराती है ।
अतः विवेकी, धर्मात्माओं को दवा, धर्म, नीति, सौजन्य और वात्सल्यपूर्वक यश अर्जन करें । यह कीर्ति स्थायी के साथ कर्म निर्जरा की भी साधक होती है ।
कृपण के धन की आलोचना
14
'स खलु कस्यापि माभूदर्थो यत्रासंविभागः शरणागतानाम् ॥15॥ "
अन्वयार्थ:- (यत्र) जहाँ (शरणागतानाम् ) शरण में आये हुओं का (असंविभागः ) योग्य भाग- हिस्सा नहीं होता (सः) वह (अर्थ) धन (कस्य) किसी का (अपि) भी (मा) नहीं (अभूत् ) हुआ । अर्थात् व्यर्थ है ।
विशेषार्थ :- जिस धन के द्वारा परोपकार, धर्मोद्धार, दानादि कार्य नहीं होते वह धन व्यर्थ है । कृपण अपने धन को संचित कर रखता है और दुर्गति का पात्र बनता है अर्थात् मर कर भुजंग बनता है । न स्वयं उपभोग करता है और न अन्य के ही उपयोग में आता है । वल्लभदेव नीतिकार ने भी कहा है।
-
किं
या न
तया कि यते वेश्येव
लक्ष्म्या या बधूरिव के वला 1 सामान्या पथिकै रुपभुज्यते
11
अर्थात् उस लुब्धक की लक्ष्मी से क्या प्रयोजन जो पत्नी के समान मात्र स्वयं के ही भोगने में आत्रे, वेश्या समान समस्त साधारण पन्थों द्वारा न भोगी जाये ? लक्ष्मी वही सार्थक है जो सर्वोपकारिणी होती है । कृपण का वैभव स्व और पर दोनों का घातक है । स्व का घातक तो इसलिए है कि वह अहर्निश उसी के अर्जन वर्द्धन और संरक्षण में ही लगा रहता है । अपने को ही भूल जाता है, आर्त- रौद्र ध्यान में विमुग्ध हुआ अशुभ गति का आस्रव करता है और नीच पर्याय को प्राप्त होता है । वर्तमान में निंद्यक कहलाता है, सभी उससे घृणा करने लगते हैं। दान, पूजा में या अन्य धर्म कार्यों में वह कृपण धन नहीं देता, बराबर दान नहीं देता तो उसकी देखा देखी अन्य साधारण जन भी योग्य धन नहीं देते हैं । क्योंकि उस समय उसे धनाढ्य कहकर अपने भी छुपने की चेष्टा करते हैं । इससे धर्म कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाते । धर्म प्रभावना की हानि होती है।
अतः भव्य जीवों का कर्तव्य है कि वे उदार मनोवृत्ति बनायें । आवश्यकता और समयानुसार सप्त क्षेत्रों में यथाशक्ति दान देकर चञ्चला लक्ष्मी को स्थायी बनाने का प्रयत्न करें ।
"नैतिकाचार का निरूपण"
अर्थिषु संविभागः स्वयमुपभोगश्चार्थस्य हि द्वे फले नास्तत्यौचित्यमेकान्तलुब्धस्य 1116 ॥
अन्वयार्थ :- (अर्थस्य) धन के (हि) निश्चय से (द्वे) दो (फले) फल हैं, प्रथम (अर्थिषु) धन के इच्छुकोंभिक्षुकों को (संविभाग :) उनके योग हिस्सा करना-देना (च) और (स्वयं) अपने आप (भोगः) भी भोगना - उपयोग में लाना (एकान्तलुब्धस्य) एकान्त रूप से स्वयं ही भोगने का अभिलाषी कृपण का कार्य (आचित्यं ) उचित (नास्ति ) नहीं है ।
21