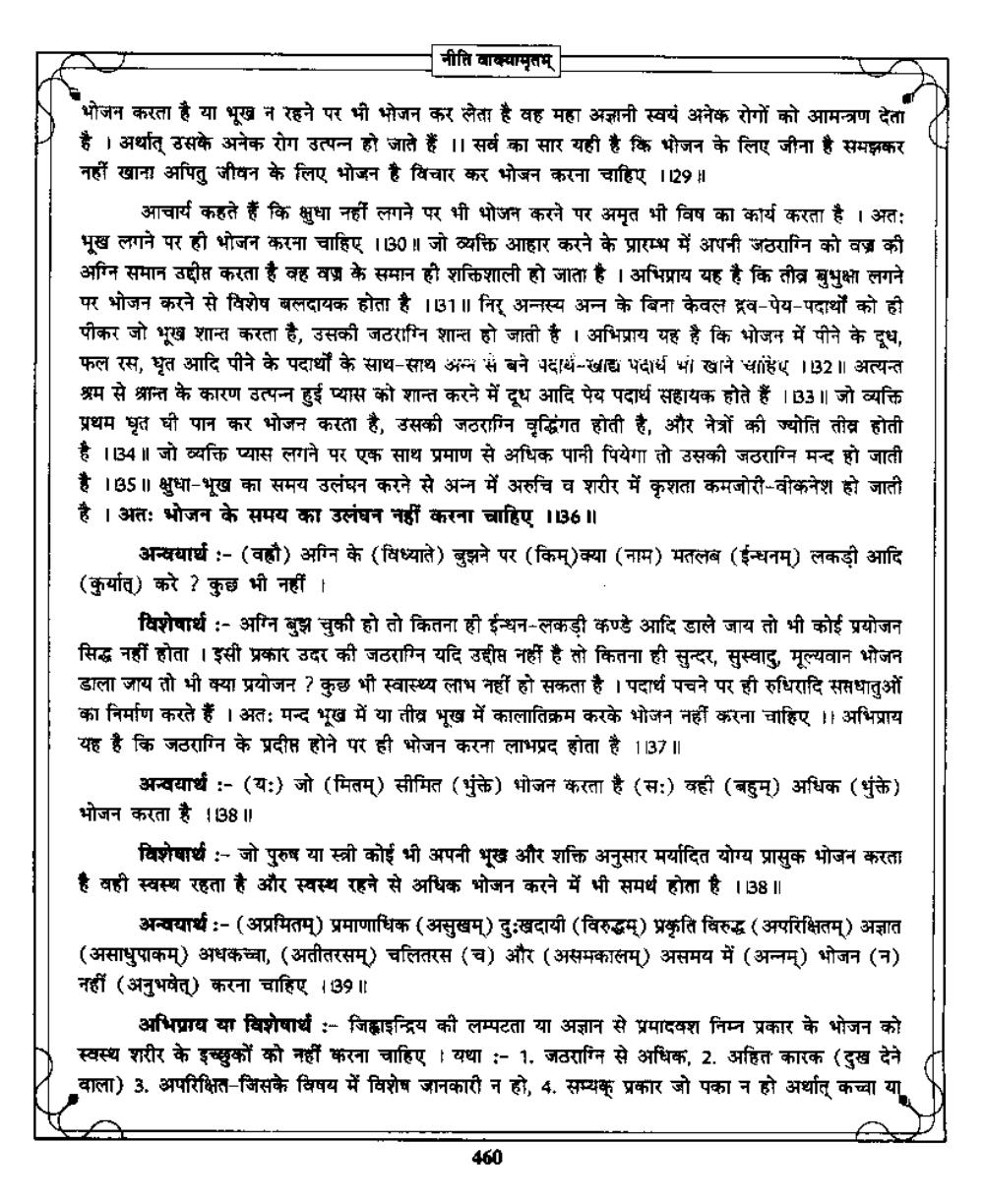________________
-नीति वाक्यामृतम् ।
भोजन करता है या भूख न रहने पर भी भोजन कर लेता है वह महा अज्ञानी स्वयं अनेक रोगों को आमन्त्रण देता है । अर्थात् उसके अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।। सर्व का सार यही है कि भोजन के लिए जीना है समझकर नहीं खाना अपितु जीवन के लिए भोजन है विचार कर भोजन करना चाहिए 1129॥
___आचार्य कहते हैं कि क्षुधा नहीं लगने पर भी भोजन करने पर अमृत भी विष का कार्य करता है । अत: भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए 100 ॥ जो व्यक्ति आहार करने के प्रारम्भ में अपनी जठराग्नि को वज्र की अग्नि समान उद्दीप्त करता है वह वज्र के समान ही शक्तिशाली हो जाता है। अभिप्राय यह है कि तीव्र ब पर भोजन करने से विशेष बलदायक होता है 181|| निर् अन्नस्य अन्न के बिना केवल द्रव-पेय-पदार्थों को ही पीकर जो भूख शान्त करता है, उसकी जठराग्नि शान्त हो जाती है । अभिप्राय यह है कि भोजन में पीने के दूध, फल रस, धृत आदि पीने के पदार्थों के साथ-साथ अन्न से बने पदार्थ खाद्य पदार्थ भी खाने चाहिए 132॥ अत्यन्त श्रम से श्रान्त के कारण उत्पन्न हुई प्यास को शान्त करने में दूध आदि पेय पदार्थ सहायक होते हैं | 3 || जो व्यक्ति प्रथम घृत घी पान कर भोजन करता है, उसकी जठराग्नि वृद्धिंगत होती है, और नेत्रों की ज्योति तीव्र होती है । 24 ॥ जो व्यक्ति प्यास लगने पर एक साथ प्रमाण से अधिक पानी पियेगा तो उसकी जठराग्नि मन्द हो जाती है 185॥ क्षुधा-भूख का समय उलंघन करने से अन्न में अरुचि व शरीर में कृशता कमजोरी-वीकनेश हो जाती है । अतः भोजन के समय का उलंघन नहीं करना चाहिए ॥6॥
अन्वयार्थ :- (वहौ) अग्नि के (विध्याते) बुझने पर (किम्)क्या (नाम) मतलब (ईन्धनम्) लकड़ी आदि (कुर्यात्) करे ? कुछ भी नहीं ।
विशेषार्थ :- अग्नि बुझ चुकी हो तो कितना ही ईन्धन-लकड़ी कण्डे आदि डाले जाय तो भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार उदर की जठराग्नि यदि उद्दीप्त नहीं है तो कितना ही सुन्दर, सुस्वादु, मूल्यवान भोजन डाला जाय तो भी क्या प्रयोजन? कुछ भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता है । पदार्थ पचने पर ही रुधिरादि ससधातुओं का निर्माण करते हैं । अतः मन्द भूख में या तीव्र भूख में कालातिक्रम करके भोजन नहीं करना चाहिए ।। अभिप्राय यह है कि जठराग्नि के प्रदीप्त होने पर ही भोजन करना लाभप्रद होता है 137॥
अन्वयार्थ :- (य:) जो (मितम्) सीमित (भुंक्ते) भोजन करता है (सः) वही (बहुम्) अधिक (भुंक्ते) भोजन करता है 188॥
विशेषार्थ :- जो पुरुष या स्त्री कोई भी अपनी भूख और शक्ति अनुसार मर्यादित योग्य प्रासुक भोजन करता है वही स्वस्थ रहता है और स्वस्थ रहने से अधिक भोजन करने में भी समर्थ होता है । 38 ॥
अन्वयार्थ :- (अप्रमितम्) प्रमाणाधिक (असुखम्) दुःखदायी (विरुद्धम्) प्रकृति विरुद्ध (अपरिक्षितम्) अज्ञात (असाधुपाकम्) अधकच्चा, (अतीतरसम्) चलितरस (च) और (असमकालम्) असमय में (अन्नम्) भोजन (न) नहीं (अनुभवेत्) करना चाहिए 139 ।।
अभिप्राय या विशेषार्थ :- जिह्वाइन्द्रिय की लम्पटता या अज्ञान से प्रमादयश निम्न प्रकार के भोजन को स्वस्थ शरीर के इच्छुकों को नहीं करना चाहिए । यथा :- 1. जठराग्नि से अधिक, 2. अहित कारक (दुख देने वाला) 3. अपरिक्षित-जिसके विषय में विशेष जानकारी न हो, 4. सम्यक् प्रकार जो पका न हो अर्थात् कच्चा या