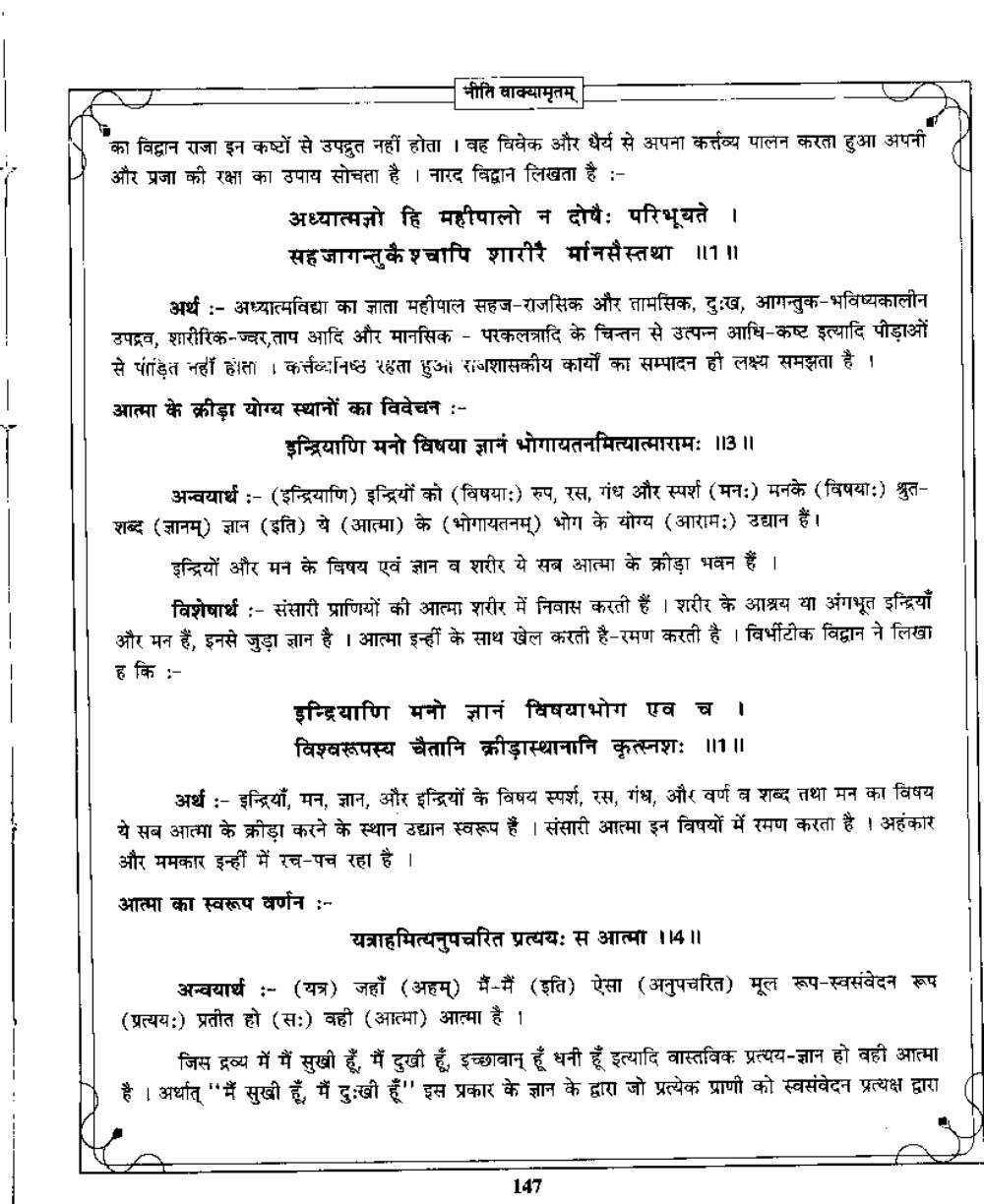________________
नीति वाक्यामृतम् ।
का विद्वान राजा इन कष्टों से उपद्रुत नहीं होता । वह विवेक और धैर्य से अपना कर्तव्य पालन करता हुआ अपनी और प्रजा की रक्षा का उपाय सोचता है । नारद विद्वान लिखता है :
अध्यात्मज्ञो हि महीपालो न दोषैः परिभूयते । सह जागन्तुकै श्चापि शारीरै मनिसैस्तथा ॥1॥
अर्थ :- अध्यात्मविद्या का ज्ञाता महीपाल सहज-राजसिक और तामसिक, दुःख, आगन्तुक-भविष्यकालीन उपद्रव, शारीरिक-ज्वर,ताप आदि और मानसिक - परकलत्रादि के चिन्तन से उत्पन्न आधि-कष्ट इत्यादि पीड़ाओं से पाड़ित नहीं होता । कर्तव्यनिष्ठ रहता हुआ राजशासकीय कार्यों का सम्पादन ही लक्ष्य समझता है । आत्मा के क्रीड़ा योग्य स्थानों का विवेचन :
इन्द्रियाणि मनो विषया ज्ञानं भोगायतनमित्यात्मारामः ॥3॥
अन्वयार्थ :- (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों को (विषयाः) रुप, रस, गंध और स्पर्श (मनः) मनके (विषयाः) श्रुतशब्द (ज्ञानम्) ज्ञान (इति) ये (आत्मा) के (भोगायतनम्) भोग के योग्य (आरामः) उद्यान हैं।
इन्द्रियों और मन के विषय एवं ज्ञान व शरीर ये सब आत्मा के क्रीड़ा भवन हैं ।
विशेषार्थ :- संसारी प्राणियों की आत्मा शरीर में निवास करती हैं । शरीर के आश्रय या अंगभूत इन्द्रियाँ और मन हैं, इनसे जुड़ा ज्ञान है । आत्मा इन्हीं के साथ खेल करती है-रमण करती है । विर्भीटीक विद्वान ने लिखा ह कि :
इन्द्रियाणि मनो ज्ञानं विषयाभोग एव च । विश्वरूपस्य चैतानि क्रीड़ास्थानानि कृत्स्नशः ॥
अर्थ :- इन्द्रियाँ, मन, ज्ञान, और इन्द्रियों के विषय स्पर्श, रस, गंध, और वर्ण व शब्द तथा मन का विषय ये सब आत्मा के क्रीड़ा करने के स्थान उद्यान स्वरूप है । संसारी आत्मा इन विषयों में रमण करता है । अहंकार और ममकार इन्हीं में रच-पच रहा है । आत्मा का स्वरूप वर्णन :
यत्राहमित्यनुपचरित प्रत्ययः स आत्मा ॥4॥ अन्वयार्थ :- (यत्र) जहाँ (अहम्) मैं-मैं (इति) ऐसा (अनुपचरित) मूल रूप-स्वसंवेदन रूप (प्रत्यय:) प्रतीत हो (स:) वही (आत्मा) आत्मा है ।
जिस द्रव्य में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इच्छावान् हूँ धनी हूँ इत्यादि वास्तविक प्रत्यय-ज्ञान हो वही आत्मा है । अर्थात् “मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ" इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा जो प्रत्येक प्राणी को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा
147