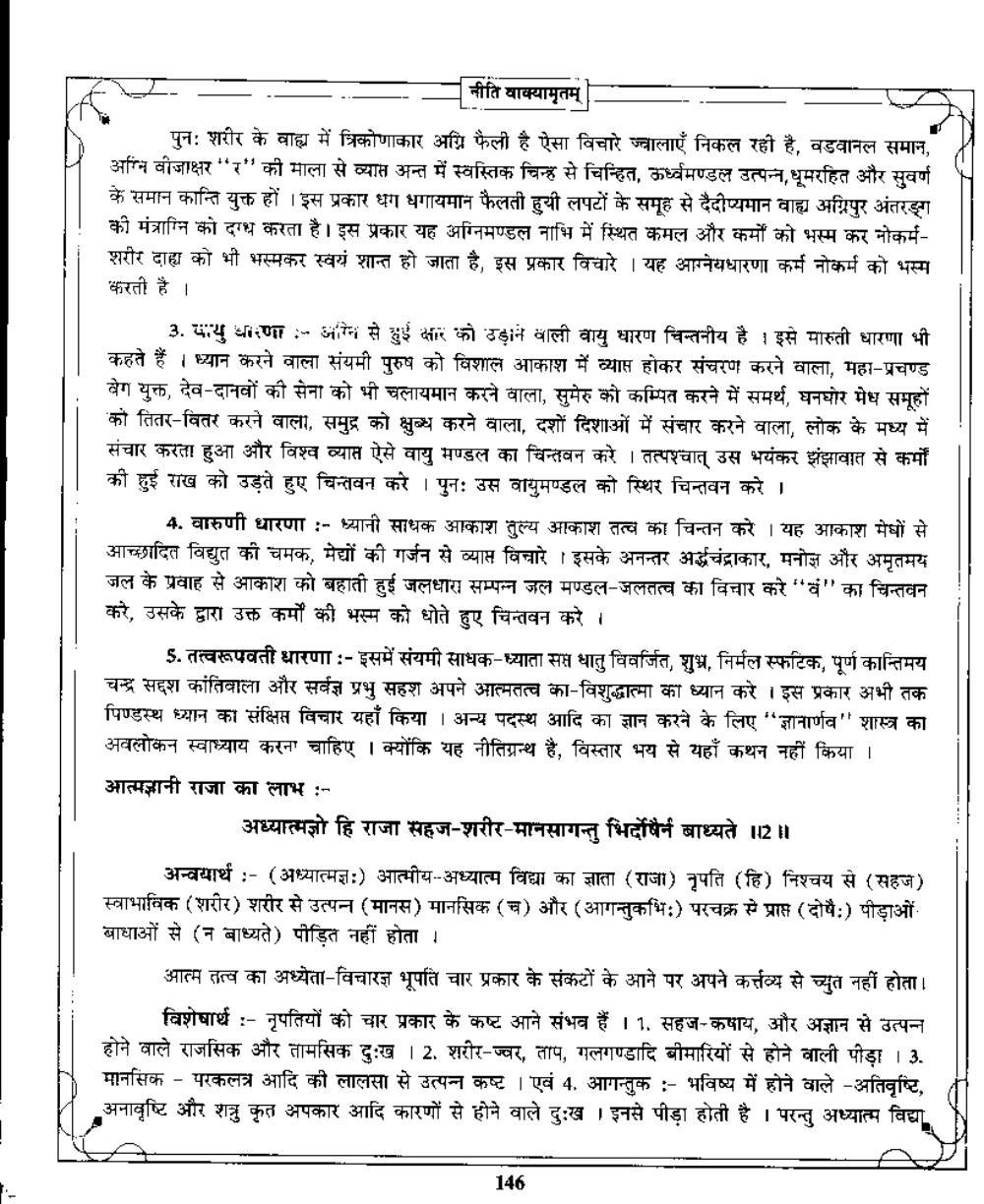________________
---नीति वाक्यामृतम् - पुनः शरीर के वाह्य में त्रिकोणाकार अग्नि फैली है ऐसा विचारे ज्वालाएँ निकल रही है, वडवानल समान, अग्नि वीजाक्षर"र" की माला से व्यास अन्त में स्वस्तिक चिन्ह से चिन्हित, ऊर्ध्वमण्डल उत्पन्न,धूमरहित और सुवर्ण के समान कान्ति युक्त हों । इस प्रकार धग धगायमान फैलती हुयी लपटों के समूह से दैदीप्यमान वाह्य अग्निपुर अंतरा की मंत्राग्नि को दग्ध करता है। इस प्रकार यह अग्निमण्डल नाभि में स्थित कमल और कर्मों को भस्म कर नोकर्मशरीर दाह्य को भी भस्मकर स्वयं शान्त हो जाता है, इस प्रकार विचारे । यह आग्नेयधारणा कर्म नोकर्म को भस्म करती है ।
3. कायु धारणा :- आंगन से हुई क्षार को उड़ाने वाली वायु धारण चिन्तनीय है । इसे मारुती धारणा भी कहते हैं । ध्यान करने वाला संयमी पुरुष को विशाल आकाश में व्याप्त होकर संचरण करने वाला, महा-प्रचण्ड वेग युक्त, देव-दानवों की सेना को भी चलायमान करने वाला, सुमेरु को कम्पित करने में समर्थ, घनघोर मेध समूहों को तितर-वितर करने वाला, समुद्र को क्षुब्ध करने वाला, दशों दिशाओं में संचार करने वाला, लोक के मध्य में संचार करता हुआ और विश्व व्याप्त ऐसे वायु मण्डल का चिन्तवन करे । तत्पश्चात् उस भयंकर झंझावात से कर्मों की हुई राख को उड़ते हुए चिन्तवन करे । पुनः उस वायुमण्डल को स्थिर चिन्तवन करे ।
4. वारुणी धारणा :- ध्यानी साधक आकाश तुल्य आकाश तत्व का चिन्तन करे । यह आकाश मेघों से आच्छादित विद्युत की चमक, मेद्यों की गर्जन से व्याप्त विचारे । इसके अनन्तर अर्द्धचंद्राकार, मनोज्ञ और अमृतमय जल के प्रवाह से आकाश को बहाती हुई जलधारा सम्पन्न जल मण्डल-जलतत्व का विचार करे "वं" का चिन्तवन करे, उसके द्वारा उक्त कर्मों की भस्म को धोते हुए चिन्तवन करे ।
5. तत्वरूपवती धारणा :- इसमें संयमी साधक-ध्याता सप्त धातु विवर्जित, शुभ्र, निर्मल स्फटिक, पूर्ण कान्तिमय चन्द्र सद्दश कांतिवाला और सर्वज्ञ प्रभु सहश अपने आत्मतत्व का-विशुद्धात्मा का ध्यान करे । इस प्रकार अभी तक पिण्डस्थ ध्यान का संक्षिप्त विचार यहाँ किया । अन्य पदस्थ आदि का ज्ञान करने के लिए "ज्ञानार्णव" शास्त्र का अवलोकन स्वाध्याय करना चाहिए । क्योंकि यह नीतिग्रन्थ है, विस्तार भय से यहाँ कथन नहीं किया । आत्मज्ञानी राजा का लाभ :
अध्यात्मज्ञो हि राजा सहज-शरीर-मानसागन्तु भिर्दोषैर्न बाध्यते ॥2॥
अन्वयार्थ :- (अध्यात्मज्ञः) आत्मीय--अध्यात्म विद्या का ज्ञाता (राजा) पति (हि) निश्चय से (सहज) स्वाभाविक (शरीर) शरीर से उत्पन्न (मानस) मानसिक (च) और (आगन्तुकभिः) परचक्र से प्राप्त (दोषैः) पीड़ाओं बाधाओं से (न बाध्यते) पीड़ित नहीं होता ।
आत्म तत्व का अध्येता-विचारज्ञ भूपति चार प्रकार के संकटों के आने पर अपने कर्त्तव्य से च्युत नहीं होता।
विशेषार्थ :- नपतियों को चार प्रकार के कष्ट आने संभव हैं । 1. सहज-कषाय, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले राजसिक और तामसिक दुःख । 2. शरीर-ज्वर, ताप, गलगण्डादि बीमारियों से होने वाली पीड़ा । 3. मानसिक - परकलत्र आदि की लालसा से उत्पन्न कष्ट । एवं 4. आगन्तुक :- भविष्य में होने वाले -अतिवृष्टि, अनावृष्टि और शत्रु कृत अपकार आदि कारणों से होने वाले दुःख । इनसे पीड़ा होती है । परन्तु अध्यात्म विद्या
146