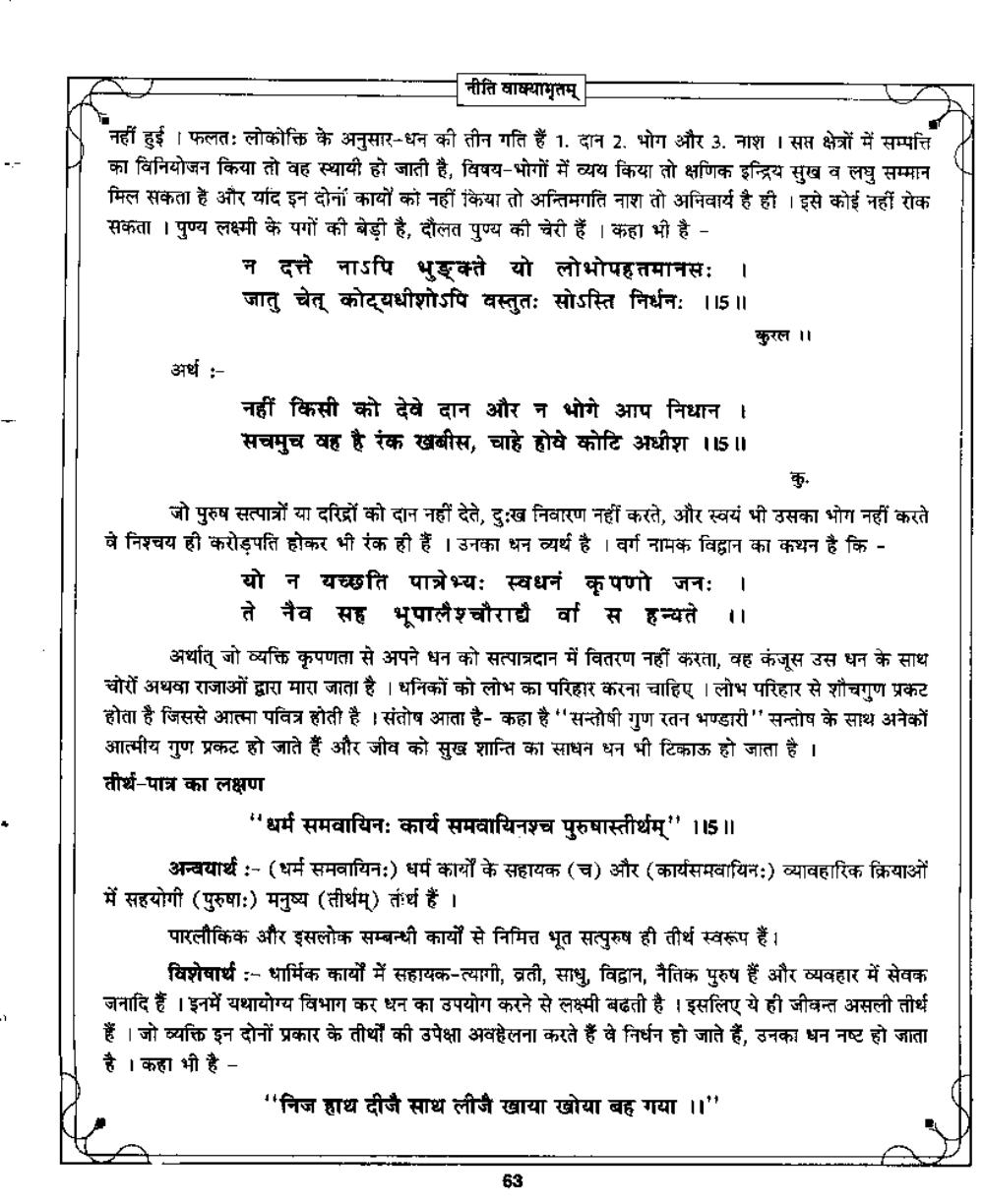________________
नीति वाक्यामृतम्
नहीं हुई । फलतः लोकोक्ति के अनुसार-धन की तीन गति हैं 1. दान 2. भोग और 3. नाश । सप्त क्षेत्रों में सम्पत्ति का विनियोजन किया तो वह स्थायी हो जाती है, विषय-भोगों में व्यय किया तो क्षणिक इन्द्रिय सुख व लघु सम्मान मिल सकता है और यदि इन दोनों कार्यों को नहीं किया तो अन्तिमगति नाश तो अनिवार्य है ही । इसे कोई नहीं रोक सकता । पुण्य लक्ष्मी के पगों की बेड़ी है, दौलत पुण्य की चेरी हैं । कहा भी है -
न दत्ते नाऽपि भुङ्क्ते यो लोभोपहतमानसः । जातु चेत् कोट्यधीशोऽपि वस्तुतः सोऽस्ति निर्धनः ।।5॥
कुरल ॥
अर्थ:
नहीं किसी को देवे दान और न भोगे आप निधान । सचमुच वह है रंक खबीस, चाहे होवे कोटि अधीश ।।5।।
जो पुरुष सत्पात्रों या दरिद्रों को दान नहीं देते, दुःख निवारण नहीं करते, और स्वयं भी उसका भोग नहीं करते वे निश्चय ही करोड़पति होकर भी रंक ही हैं । उनका धन व्यर्थ है । वर्ग नामक विद्वान का कथन है कि -
यो न यच्छति पात्रेभ्यः स्वधनं कृपणो जनः ।
ते नैव सह भूपालैश्चौराद्यै वा स हन्यते ।। अर्थात् जो व्यक्ति कृपणता से अपने धन को सत्पात्रदान में वितरण नहीं करता, वह कंजूस उस धन के साथ चोरों अथवा राजाओं द्वारा मारा जाता है । धनिकों को लोभ का परिहार करना चाहिए । लोभ परिहार से शौचगुण प्रकट होता है जिससे आत्मा पवित्र होती है । संतोष आता है- कहा है "सन्तोषी गुण रतन भण्डारी" सन्तोष के साथ अनेकों आत्मीय गुण प्रकट हो जाते हैं और जीव को सुख शान्ति का साधन धन भी टिकाऊ हो जाता है । तीर्थ-पान का लक्षण
"धर्म समवायिनः कार्य समवायिनश्च पुरुषास्तीर्थम्" ॥5॥ अन्वयार्थ :- (धर्म समवायिनः) धर्म कार्यों के सहायक (च) और (कार्यसमवायिनः) व्यावहारिक क्रियाओं में सहयोगी (पुरुषाः) मनुष्य (तीर्थम्) तीर्थ हैं ।
पारलौकिक और इसलोक सम्बन्धी कार्यों से निमित्त भूत सत्पुरुष ही तीर्थ स्वरूप हैं ।
विशेषार्थ :- धार्मिक कार्यों में सहायक-त्यागी, व्रती, साधु, विद्वान, नैतिक पुरुष हैं और व्यवहार में सेवक जनादि हैं । इनमें यथायोग्य विभाग कर धन का उपयोग करने से लक्ष्मी बढ़ती है । इसलिए ये ही जीवन्त असली तीर्थ हैं । जो व्यक्ति इन दोनों प्रकार के तीर्थों की उपेक्षा अवहेलना करते हैं वे निर्धन हो जाते हैं, उनका धन नष्ट हो जाता है । कहा भी है -
"निज हाथ दीजै साथ लीजै खाया खोया बह गया ।"