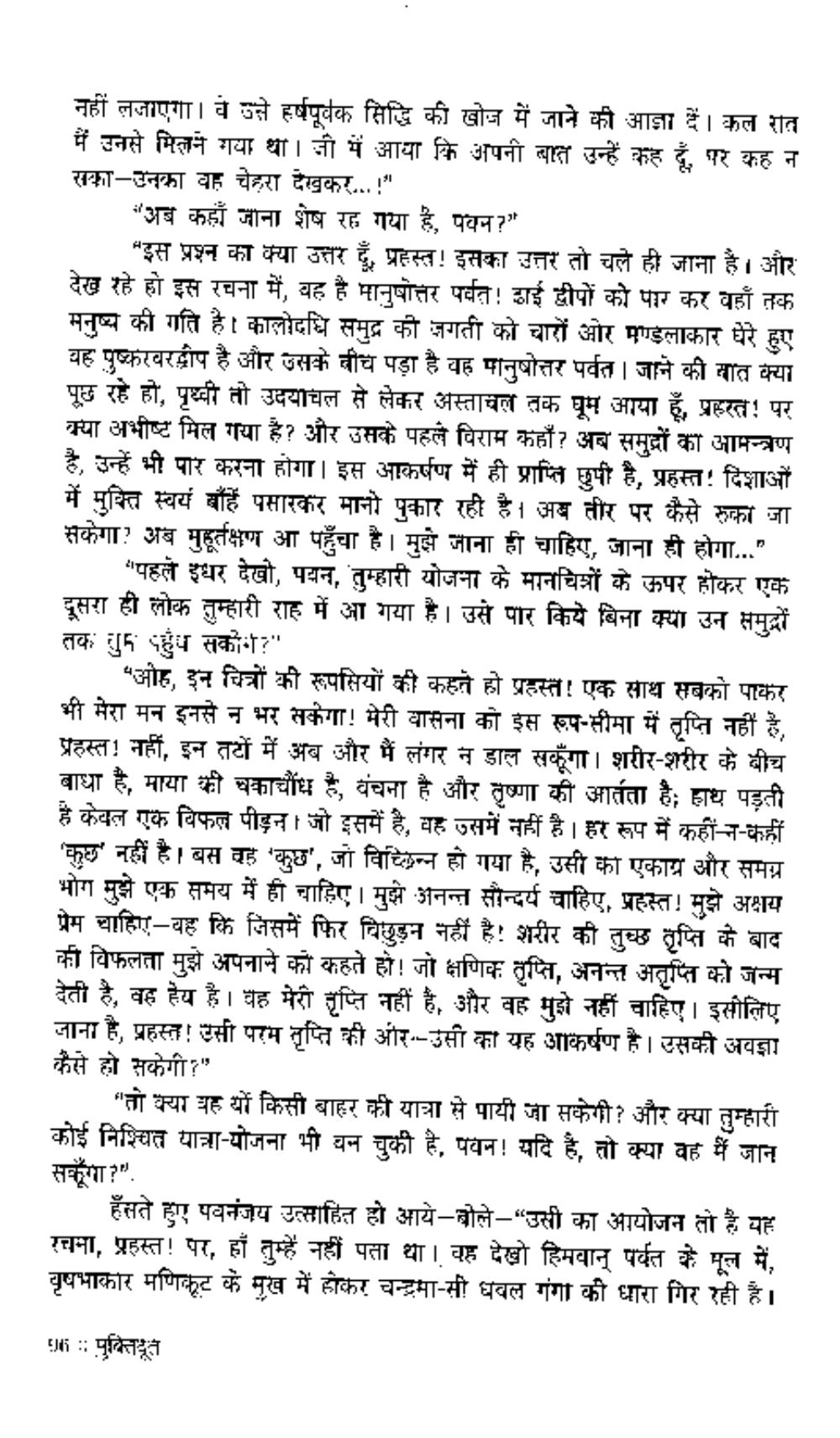________________
नहीं लजाएगा। वे उसे हर्षपूर्वक सिद्धि की खोज में जाने की आज्ञा दें। कल रात मैं उनसे मिलने गया था। जी में आया कि अपनी बात उन्हें कह दूँ, पर कह न सका-उनका वा चेहरा देखकर...!"
"अब कहाँ जाना शेष रह गया है, पवन?" ___ इस प्रश्न का क्या उत्तर द्, प्रहस्त! इसका उत्तर तो चले ही जाना है। और देख रहे हो इस रचना में, वह है मानुषोत्तर पर्वत! डाई द्वीपों को पार कर वहाँ तक मनष्य की गति है। कालोदधि समुद्र की जगती को चारों ओर मण्डलाकार घेरे हुए वह पुष्करवरद्वीप है और उसके बीच पड़ा है वह पानुषोत्तर पर्वत । जाने की बात क्या पूछ रहे हो, पृथ्वी तो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक घूम आया हूँ, प्रहरत! पर क्या अभीष्ट मिल गया है? और उसके पहले विराम कहाँ? अब समुद्रों का आमन्त्रण है, उन्हें भी पार करना होगा। इस आकर्षण में ही प्राप्ति छुपी है, प्रहस्त: दिशाओं में मुक्ति स्वयं बाँहें पसारकर मानो पुकार रही है। अब तीर पर कैसे रुका जा सकेगा? अब मुहूर्तक्षण आ पहुँचा है। मुझे जाना ही चाहिए, जाना ही होगा..."
___ "पहले इधर देखो, पयन, तुम्हारी योजना के मानचित्रों के ऊपर होकर एक दुसरा ही लोक तुम्हारी राह में आ गया है। उसे पार किये बिना क्या उन समुद्री तक तुम पहुँच सकोग?"
ओह. इन चित्रों की रूपसियों की कहते हो प्रहस्त! एक साथ सबको पाकर भी मेरा मन इनसे न भर सकेगा! मेरी वासना को इस रूप-सीमा में तृप्ति नहीं है, प्रहस्त! नहीं, इन तटों में अब और मैं लंगर न डाल सकूँगा। शरीर-शरीर के बीच बाधा है, माया की चकाचौंध है, वंचना है और तष्णा की आर्तता है; हाथ पड़ती है केवल एक विफल पीड़न । जो इसमें है, वह उसमें नहीं है। हर रूप में कहीं-न-कहीं 'कुछ' नहीं है। बस वह 'कुछ', जो विच्छिन्न हो गया है, उसी का एकाग्र और समग्न भोग मुझे एक समय में ही चाहिए। मुझे अनन्त सौन्दर्य चाहिए, प्रहस्त! मुझे अक्षय प्रेम चाहिए-यह कि जिसमें फिर विछड़न नहीं है। शरीर की तुच्छ तप्ति के बाद की विफलता मुझे अपनाने को कहते हो! जो क्षणिक तृप्ति, अनन्त अतृप्ति को जन्म देती है, वह हेय है। वह मेरी तृप्ति नहीं है, और वह मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए जाना है, प्रहस्त ! उसी परम तृप्ति की और-उसी का यह आकर्षण है। उसकी अवज्ञा कैसे हो सकेगी?"
__ "तो क्या यह यों किसी बाहर की यात्रा से पायी जा सकेगी? और क्या तुम्हारी कोई निश्चित यात्रा-योजना भी बन चुकी है, पवन! यदि है, तो क्या वह मैं जान सकूँगा?".
हँसते हा पवनंजय उत्साहित हो आये-बोले-“उसी का आयोजन तो है यह रचमा, प्रहस्त! पर, हाँ तुम्हें नहीं पता था। वह देखो हिमवान् पर्वत के मूल में, वृषभाकार मणिकूट के मुख में होकर चन्द्रमा-सी धवल गंगा की धारा गिर रही हैं।
५] :: पुस्तित