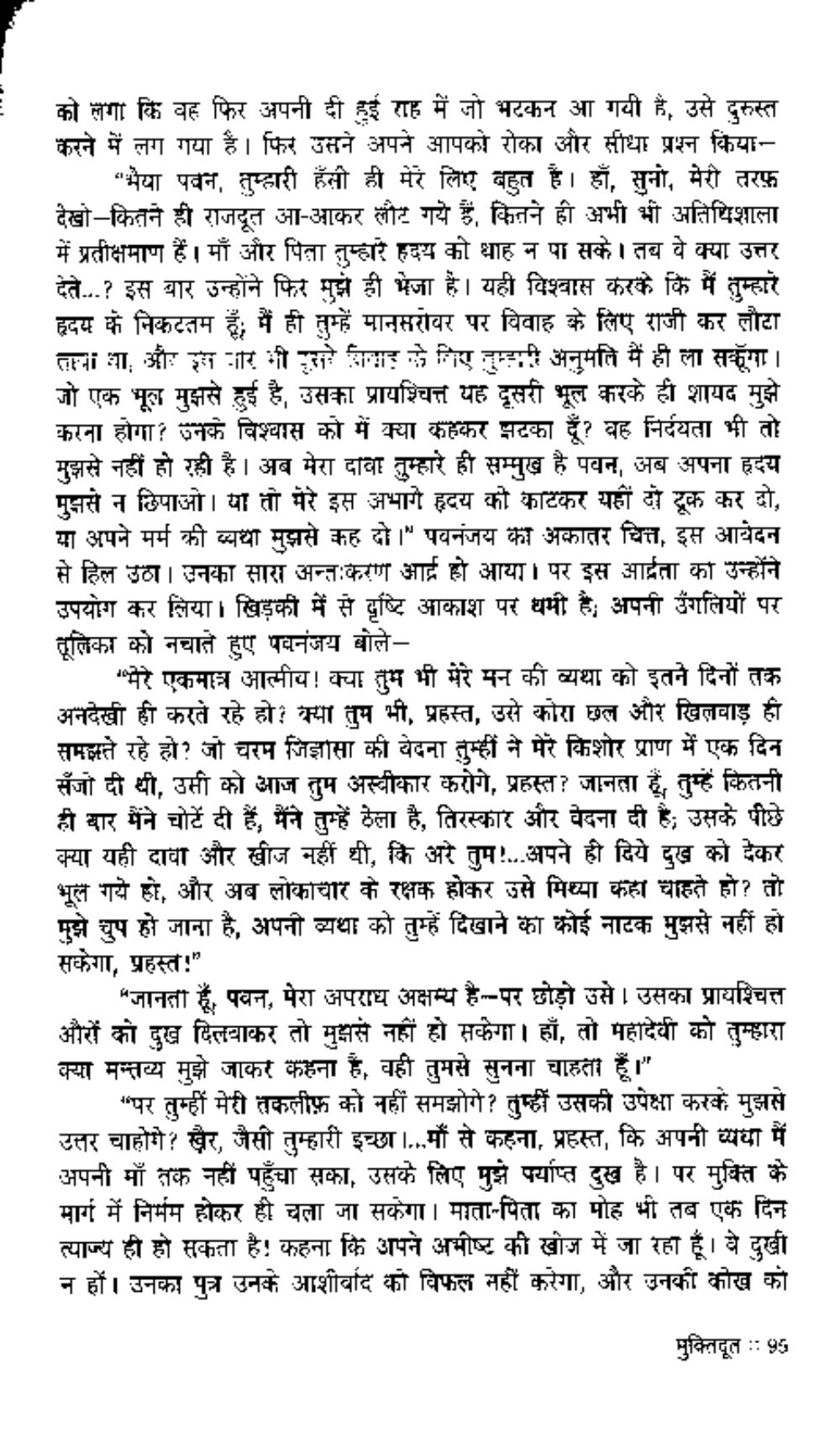________________
को लगा कि वह फिर अपनी दी हुई राह में जो भटकन आ गयी हैं, उसे दुरुस्त करने में लग गया हैं। फिर उसने अपने आपको रोका और सीधा प्रश्न किया“भैया पवन, तुम्हारी हँसी ही मेरे लिए बहुत हैं। हाँ, सुनो, मेरी तरफ़ देखो - कितने ही राजदूत आ- आकर लौट गये हैं, कितने ही अभी भी अतिथिशाला में प्रतीक्षमाण हैं। माँ और पिता तुम्हारे हृदय को धाह न पा सके। तब वे क्या उत्तर देते...? इस बार उन्होंने फिर मुझे ही भेजा है। यही विश्वास करके कि मैं तुम्हारे हृदय के निकटतम हूँ, मैं ही तुम्हें मानसरोवर पर विवाह के लिए राजी कर लौटा ताना था, और इस बार भी विवाह के लिए तुम्हारी अनुमति में ही ला सकूँगा । जो एक भूल मुझसे हुई है, उसका प्रायश्चित्त यह दूसरी भूल करके ही शायद मुझे करना होगा? उनके विश्वास को में क्या कहकर झटका दूँ? वह निर्दयता भी तो मुझसे नहीं हो रही है। अब मेरा दावा तुम्हारे ही सम्मुख है पवन, अब अपना हृदय मुझसे न छिपाओ। या तो मेरे इस अभागे हृदय को काटकर यहीं दो टूक कर दो, या अपने मर्म की व्यथा मुझसे कह दो।" पवनंजय का अकातर चित्त, इस आवेदन से हिल उठा। उनका सारा अन्तःकरण आर्द्र हो आया। पर इस आर्द्रता का उन्होंने उपयोग कर लिया। खिड़की में से दृष्टि आकाश पर धमी हैं अपनी उँगलियों पर तूलिका को नचाते हुए पवनंजय बोले
"मेरे एकमात्र आत्मीय ! क्या तुम भी मेरे मन की व्यथा को इतने दिनों तक अनदेखी ही करते रहे हो? क्या तुम भी, प्रहस्त, उसे कोरा छल और खिलवाड़ ही समझते रहे हो? जो चरम जिज्ञासा की बेदना तुम्हीं ने मेरे किशोर प्राण में एक दिन सँजो दी थी, उसी को आज तुम अस्वीकार करोगे, प्रहस्त ? जानता हूँ, तुम्हें कितनी ही बार मैंने चोटें दी हैं, मैंने तुम्हें ठेला है, तिरस्कार और वेदना दी है; उसके पीछे क्या यही दावा और खीज नहीं थी, कि अरे तुम !... अपने ही दिये दुख को देकर भूल गये हो, और अब लोकाचार के रक्षक होकर उसे मिथ्या कहा चाहते हो? तो मुझे चुप हो जाना है, अपनी व्यथा को तुम्हें दिखाने का कोई नाटक मुझसे नहीं हो सकेगा, प्रहस्त!”
"जानता हूँ, पवन, मेरा अपराध अक्षम्य है--पर छोड़ो उसे उसका प्रायश्चित्त औरों को दुख दिलवाकर तो मुझसे नहीं हो सकेगा । हाँ, तो महादेवी को तुम्हारा क्या मन्तव्य मुझे जाकर कहना हैं, वही तुमसे सुनना चाहता हूँ।"
"पर तुम्हीं मेरी तकलीफ़ को नहीं समझोगे ? तुम्हीं उसकी उपेक्षा करके मुझसे उत्तर चाहोगे? खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा।... माँ से कहना, प्रहस्त, कि अपनी व्यथा मैं अपनी माँ तक नहीं पहुँचा सका, उसके लिए मुझे पर्याप्त दुख है। पर मुक्ति के मार्ग में निर्मम होकर ही चला जा सकेगा। माता-पिता का मोह भी तब एक दिन त्याज्य ही हो सकता है ! कहना कि अपने अभीष्ट की खोज में जा रहा हूँ। वे दुखी न हों। उनका पुत्र उनके आशीर्वाद को विफल नहीं करेगा, और उनकी कोख को
मुक्तिदूत : ४७