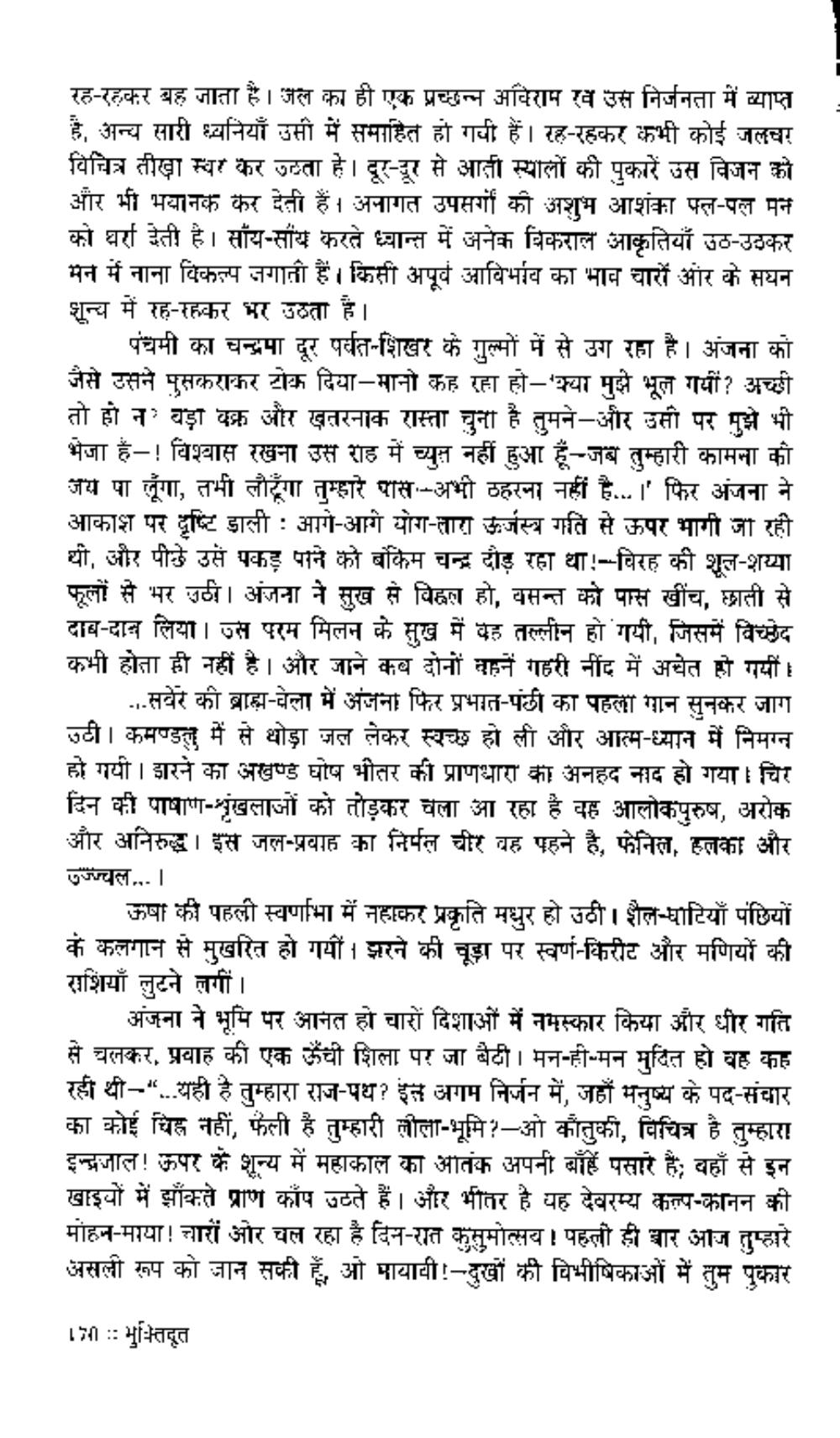________________
रह-रहकर बह जाता है। जल का ही एक प्रच्छन्न अविराम ख उस निर्जनता में व्याप्त है, अन्य सारी ध्वनियाँ उसी में समाहित हो गयी हैं। रह-रहकर कभी कोई जलचर विचित्र तीखा स्वर कर उठता है । दूर-दूर से आती स्यालों की पुकारें उस विजन को
और भी भयानक कर देती हैं। अनागत उपसर्गों की अशुभ आशंका पल-पल मन को घर देती है। सांय-सीय करते ध्यान्त में अनेक विकराल आकृतियाँ उठ-उठकर मन में नाना विकल्प जगाती हैं। किसी अपूर्व आविर्भाव का भान चारों ओर के सघन शून्य में रह-रहकर भर उठता है।
पंचमी का चन्द्रपा दूर पर्वत-शिखर के गुल्मों में से उग रहा है। अंजना को जैसे उसने पुसकराकर टोक दिया-मानो कह रहा हो-'श्या मुझे भूल गयीं? अच्छी तो हो न’ बड़ा वक्र और खतरनाक रास्ता चुना है तुमने-और उसी पर मुझे भी भेजा हैं-! विश्वास रखना उस राह में च्यन्त नहीं हुआ हूँ-जब तुम्हारी कामना को जय पा लूँगा, तभी लौटूंगा तुम्हारे पास-अभी ठहरना नहीं है...।' फिर अंजना ने आकाश पर दृष्टि डाली : आगे-आगे योग-तारा ऊर्जस्व गति से ऊपर भागी जा रही थी, और पीछे उसे पकड़ पाने को बोकम चन्द्र दौड़ रहा था!-चिरह की शूल-शय्या फूलों से भर उठी। अंजना ने सुख से विह्वल हो, वसन्त को पास खींच, छाती से दाब-दाब लिया। उस परम मिलन के सुख में वह तल्लीन हो गयी, जिसमें विच्छेद कभी होता ही नहीं है। और जाने कब दोनों बहनें गहरी नींद में अचेत हो गयीं।
...सवेरे की ब्राह्म-वेला में अंजना फिर प्रभात-पंछी का पहला गान सुनकर जाग उठी। कमण्डलु में से थोड़ा जल लेकर स्वच्छ हो ली और आत्म-ध्यान में निमग्न हो गयी। झारने का अखण्ड घोष भीतर की प्राणधारा का अनहद नाद हो गया। चिर दिन की पाषाण-शृंखलाजों को तोड़कर चला आ रहा है वह आलोकपुरुष, अरोक
और अनिरुद्ध । इस जल-प्रवाह का निर्मल चीर वह पहने है, फेनिल, हलका और उज्ज्व ल...|
ऊषा की पहली स्वर्णाभा में नहाकर प्रकृति मधुर हो उठी। शैल-घाटियाँ पंछियों के कलगान से मुखरित हो गयौं । झरने की चूड़ा पर स्वर्ण-किरीट और मणियों की राशियाँ लुटने लगीं। ____अंजना ने भूमि पर आनत हो चारों दिशाओं में नमस्कार किया और धीर गति से चलकर, प्रवाह की एक ऊँची शिला पर जा बैठी। मन-ही-मन मुदित हो वह कह रही थी-“...यही है तुम्हारा राज-पथ? इस अगम निर्जन में, जहाँ मनुष्य के पद-संचार का कोई चिह्न नहीं, फैली है तुम्हारी लीला-भूमि?-ओ कौतुकी, विचित्र है तुम्हारा इन्द्रजाल! ऊपर के शुन्य में महाकाल का आतंक अपनी बाँहें पसारे है; वहाँ से इन खाइयों में झाँकते प्राण काँप उटते हैं। और भीतर है यह देवरम्य कल्प-कानन की मोहन-माया! चारों ओर चल रहा है दिन-रात कुसुमोत्सब। पहली ही चार आज तुम्हारे असली रूप को जान सकी हूँ, ओ मायावी!-दुखों की विभीषिकाओं में तुम पुकार
130 :: भुक्तिदूत