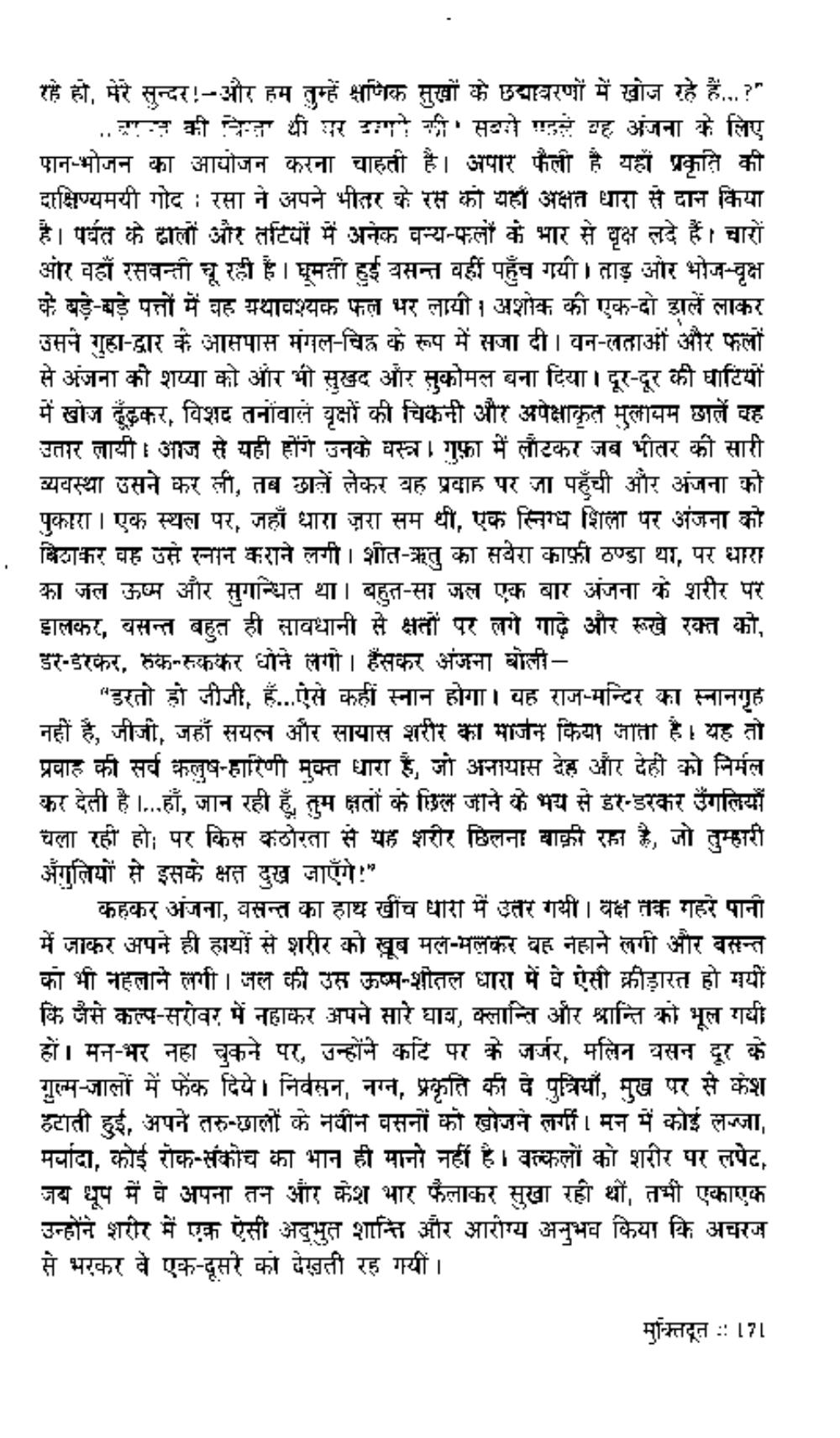________________
1
.
1
रहे हो, मेरे सुन्दर! और हम तुम्हें क्षणिक सुखों के छद्मावरणों में खोज रहे हैं...?" कीािथी घर की सबसे पहले यह अंजना के लिए पान-भोजन का आयोजन करना चाहती है। अपार फैली है यहाँ प्रकृति की दाक्षिण्यमयी गोद रसा ने अपने भीतर के रस को यहाँ अक्षत धारा से दान किया है । पर्वत के ढालों और तटियों में अनेक वन्य-फलों के भार से वृक्ष लदे हैं। चारों और वहाँ रसवन्ती चू रही है। घूमती हुई बसन्त वहीं पहुँच गयी। ताड़ ओर भोज-वृक्ष के बड़े-बड़े पत्तों में वह यथावश्यक फल भर लायी अशोक की एक-दो डालें लाकर उसने गुहा द्वार के आसपास मंगल - चिह्न के रूप में सजा दी । वन-लताओं और फलों से अंजना को शय्या को और भी सुखद और सुकोमल बना दिया। दूर-दूर की घाटियों में खोज ढूँढकर, विशद तनोंवाले वृक्षों की चिकनी और अपेक्षाकृत मुलायम छालें वह उतार लायी। आज से यही होंगे उनके वस्त्र गुफ़ा में लौटकर जब भीतर की सारी व्यवस्था उसने कर ली, तब छालें लेकर बह प्रवाह पर जा पहुँची और अंजना को पुकारा । एक स्थल पर जहाँ धारा ज़रा सम थी, एक स्निग्ध शिला पर अंजना को बिठाकर वह उसे स्नान कराने लगी। शीत ऋतु का सवेरा काफ़ी ठण्डा था, पर धारा का जल ऊष्म और सुगन्धित था। बहुत-सा जल एक बार अंजना के शरीर पर डालकर, बसन्त बहुत ही सावधानी से क्षतों पर लगे गाढ़े और रूखे रक्त को, डर-डरकर, रुक-रुककर धोने लगी। हँसकर अंजना बोली
"डरतो हो जीजी हैं... ऐसे कहीं स्नान होगा। यह राज मन्दिर का स्नानगृह नहीं है, जीजी, जहाँ सयत्न और सायास शरीर का भार्जन किया जाता है। यह तो प्रवाह की सर्व कलुष हारिणी मुक्त धारा हैं, जो अनायास देह और देही को निर्मल कर देती है ।...हाँ, जान रही हूँ, तुम क्षतों के छिल जाने के भय से डर-डरकर उँगलियाँ 'चला रही हो। पर किस कठोरता से यह शरीर छिलना बाकी रहा है, जो तुम्हारी अँगुलियों से इसके क्षत दुख जाएँगे!"
कहकर अंजना, वसन्त का हाथ खींच धारा में उतर गयी। वक्ष तक गहरे पानी में जाकर अपने ही हाथों से शरीर को खूब मल-मलकर वह नहाने लगी और वसन्त को भी नहलाने लगी। जल की उस ऊष्म-शीतल धारा में वे ऐसी क्रीड़ारत हो गयीं कि जैसे कल्प-सरोवर में नहाकर अपने सारे घाव, क्लान्ति और श्रान्ति को भूल गयी हों । मन भर नहा चुकने पर उन्होंने कटि पर के जर्जर, मलिन बसन दूर के गुल्म- जालों में फेंक दिये। निर्वसन, नग्न, प्रकृति की वे पुत्रियों, मुख पर से केश हटाती हुई, अपने तरु-छालों के नवीन वसनों को खोजने लगीं। मन में कोई लज्जा, मर्यादा, कोई रोक- संकोच का भान ही मानो नहीं है। वल्कलों को शरीर पर लपेट, जब धूप में वे अपना तन और केश भार फैलाकर सुखा रही थीं, तभी एकाएक उन्होंने शरीर में एक ऐसी अद्भुत शान्ति और आरोग्य अनुभव किया कि अचरज से भरकर वे एक-दूसरे को देखती रह गयीं ।
मुक्तिदूत ::171