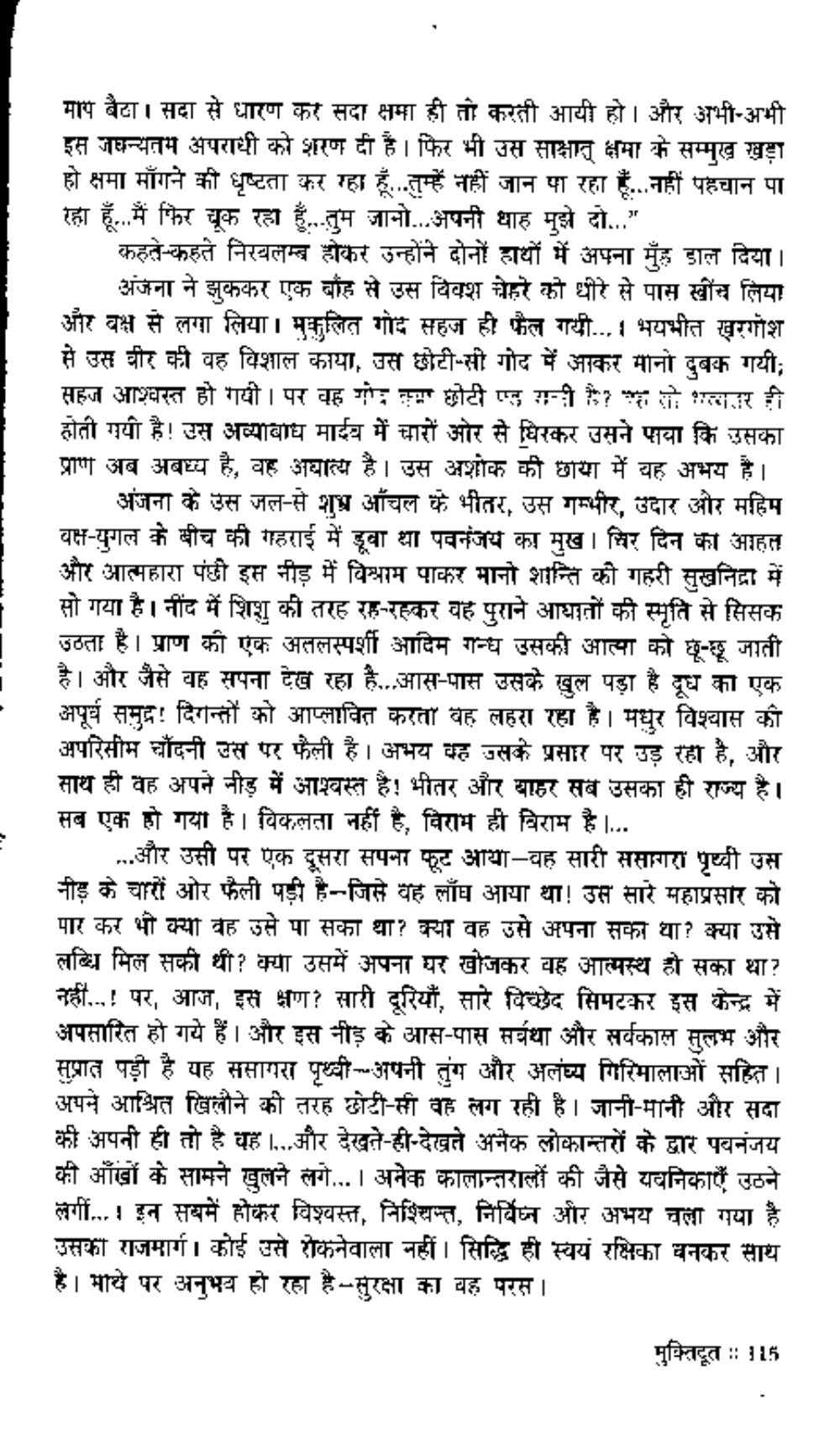________________
माप बैटा। सदा से धारण कर सदा क्षमा ड़ी तो करती आयी हो। और अभी-अभी इस जघन्यतम अपराधी को शरण दी हैं। फिर भी उस साक्षात् क्षमा के सम्मुख खड़ा हो क्षमा माँगने की धृष्टता कर रहा हूँ...तुम्हें नहीं जान पा रहा हूँ...नहीं पहचान पा रहा हूँ...मैं फिर चूक रहा हूँ...तुम जानो...अपनी थाह मुझे दो..."
कहते-कहते निरबलम्ब होकर उन्होंने दोनों हाथों में अपना मुँह डाल दिया।
अंजना ने झुककर एक बाँह से उस विवश चेहरे को धीरे से पास खींच लिया और वक्ष से लगा लिया। मलित गोद सहज ही फैल गयी...। भयभीत खरगोश से उस वीर की वह विशाल काया, उस छोटी-सी गोद में आकर मानो दुबक गयी; सहज आश्वस्त हो गयी। पर वह गोदकमा छोटी प्न गन्दी ? आत्मार ही होती गयी है! उस अव्याबाध मार्दव में चारों ओर से घिरकर उसने पाया कि उसका प्राण अब अबध्य है, वह अपात्य है। उस अशोक की छाया में यह अभय है।
अंजना के उस जल-से शन्न आँचल के भीतर, उस गम्भीर, उदार और महिम वक्ष-युगल के बीच की गहराई में डूवा था पवनंजय का मुख। चिर दिन का आहत
और आत्महारा पंछी इस नीड़ में विश्राम पाकर मानो शान्ति की गहरी सखनिद्रा में सो गया है। नींद में शिशु की तरह रह-रहकर वह पुराने आघातों की स्मृति से सिसक उठता है। प्राण की एक अतलस्पर्शी आदिम गन्ध उसकी आत्मा को छू-छू जाती है। और जैसे वह सपना देख रहा है...आस-पास उसके खुल पड़ा है दूध का एक अपूर्व समुद्र! दिगन्तों को आप्लावित करता वह लहरा रहा है। मधुर विश्वास की अपरिसीम चौदनी उस पर फैली है। अभय वह उसके प्रसार पर उड़ रहा है, और साथ ही वह अपने नीड़ में आश्वस्त है। भीतर और बाहर सब उसका ही राज्य है। सब एक हो गया है। विकलता नहीं है, विराम ही विराम है।...
...और उसी पर एक दुसरा सपना फूट आया-वह सारी ससागरा पृथ्वी उस नीड़ के चारों ओर फैली पड़ी है-जिसे वह लाँघ आया था! उस सारे महाप्रसार को पार कर भी क्या वह उसे पा सका था? क्या वह उसे अपना सका था? क्या उसे लब्धि मिल सकी थी? क्या उसमें अपना घर खोजकर वह आत्मस्थ हो सका था? नही...! पर, आज, इस क्षण? सारी दूरियों, सारे विच्छेद सिमटकर इस केन्द्र में अपसारित हो गये हैं। और इस नीड़ के आस-पास सर्वथा और सर्वकाल सुलभ और सुप्रात पड़ी है यह ससागरा पृथ्वी अपनी तुंग और अलंघ्य गिरिमालाओं सहित । अपने आश्रित खिलौने की तरह छोटी-सी वह लग रही है। जानी-मानी और सदा की अपनी ही तो है वह।...और देखते-ही-देखते अनेक लोकान्तरों के द्वार पवनंजय की आँखों के सामने खुलने लगे...। अनेक कालान्तरालों की जैसे यवनिकाएँ उठने लगी...। इन सबमें होकर विश्वस्त, निश्यिन्त, निर्विघ्न और अभय चला गया है उसका राजमार्ग। कोई उसे रोकनेवाला नहीं। सिद्धि ही स्वयं रक्षिका धनकर साथ है। माथे पर अनुभव हो रहा है-सुरक्षा का यह परस ।
मुक्तिदूत : 15