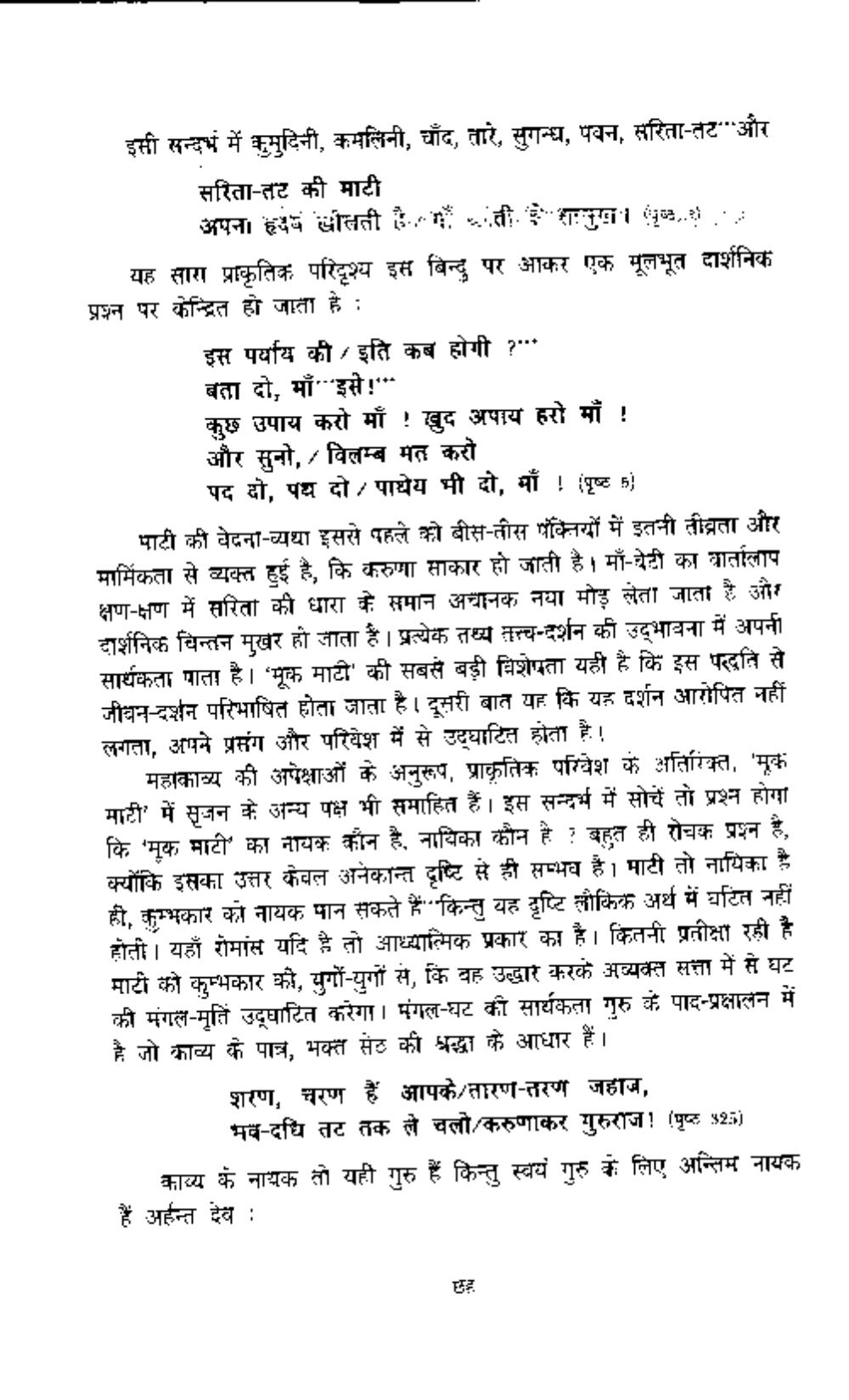________________
इसी सन्दर्भ में कुमुदिनी, कमलिनी, चाँद, तारे, सुगन्ध, पवन, सरिता-तट और
सरिता-तट की माटी
अपना हवं खोलती है तो सामुमा । ७५, .. : यह सारा प्राकृतिक परिदृश्य इस बिन्दु पर आकर एक मूलभूत दार्शनिक प्रश्न पर केन्द्रित हो जाता है :
इस पर्याय की । इति कब होगी ?" बता दो, माँ इसे ! कुछ उपाय करो माँ ! खुद अपाय हरो माँ !
और सनो,/ विलम्ब मत करो
पद दो, पथ दो / पाथेय भी दो, माँ ! पृष्ठ 5 पाटी की वेदना-व्यथा इससे पहले को बीस-तीस पक्तियों में इतनी तीव्रता और मार्मिकता से व्यक्त हुई है, कि करुणा साकार हो जाती है। माँ-बेटी का वार्तालाप क्षण-क्षण में सरिता की धारा के समान अचानक नया मोड़ लेता जाता है, और दार्शनिक चिन्तन मुखर हो जाता हैं। प्रत्येक तथ्य तत्च-दर्शन की उद्भावना में अपनी सार्थकता पाता है। 'मूक माटी' की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस पद्धति से जीवन-दर्शन परिभाषित होता जाता है। दूसरी बात यह कि यह दर्शन आरोपित नहीं लगता, अपने प्रसंग और परिवेश में से उद्घाटित होता है।
महाकाव्य की अपेक्षाओं के अनुरूप, प्राकृतिक परिवेश के अतिरिक्त, 'मूक माटी' में सजन के अन्य पक्ष भी समाहित हैं। इस सन्दर्भ में सोचें तो प्रश्न होगा कि 'मुक माटी' का नायक कौन है, नायिका कौन है ? बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर केवल अनेकान्त दृष्टि से ही सम्भव है। माटी तो नायिका है ही, कुम्भकार को नायक पान सकते हैं किन्तु यह दृष्टि लौकिक अर्थ में घटित नहीं होती। यहाँ रोमांस यदि है तो आध्यात्मिक प्रकार का है। कितनी प्रतीक्षा रही है माटी को कुम्भकार को, युगों-युगों से, कि वह उद्धार करके अव्यक्त सत्ता में से घट की मंगल-मृति उद्घाटित करेगा। मंगल-घट की सार्थकता गुरु के पाद-प्रक्षालन में है जो काव्य के पात्र, भक्त संठ की श्रद्धा के आधार हैं।
शरण, चरण हैं आपके/तारण-तरण जहाज,
भव-दधि तट तक ले चलो करुणाकर गुरुराज! [पृष्ठ 925) काव्य के नायक तो यहीं गुरु हैं किन्तु स्वयं गुरु के लिए अन्तिम नायक हैं अर्हन्त देव :
छह