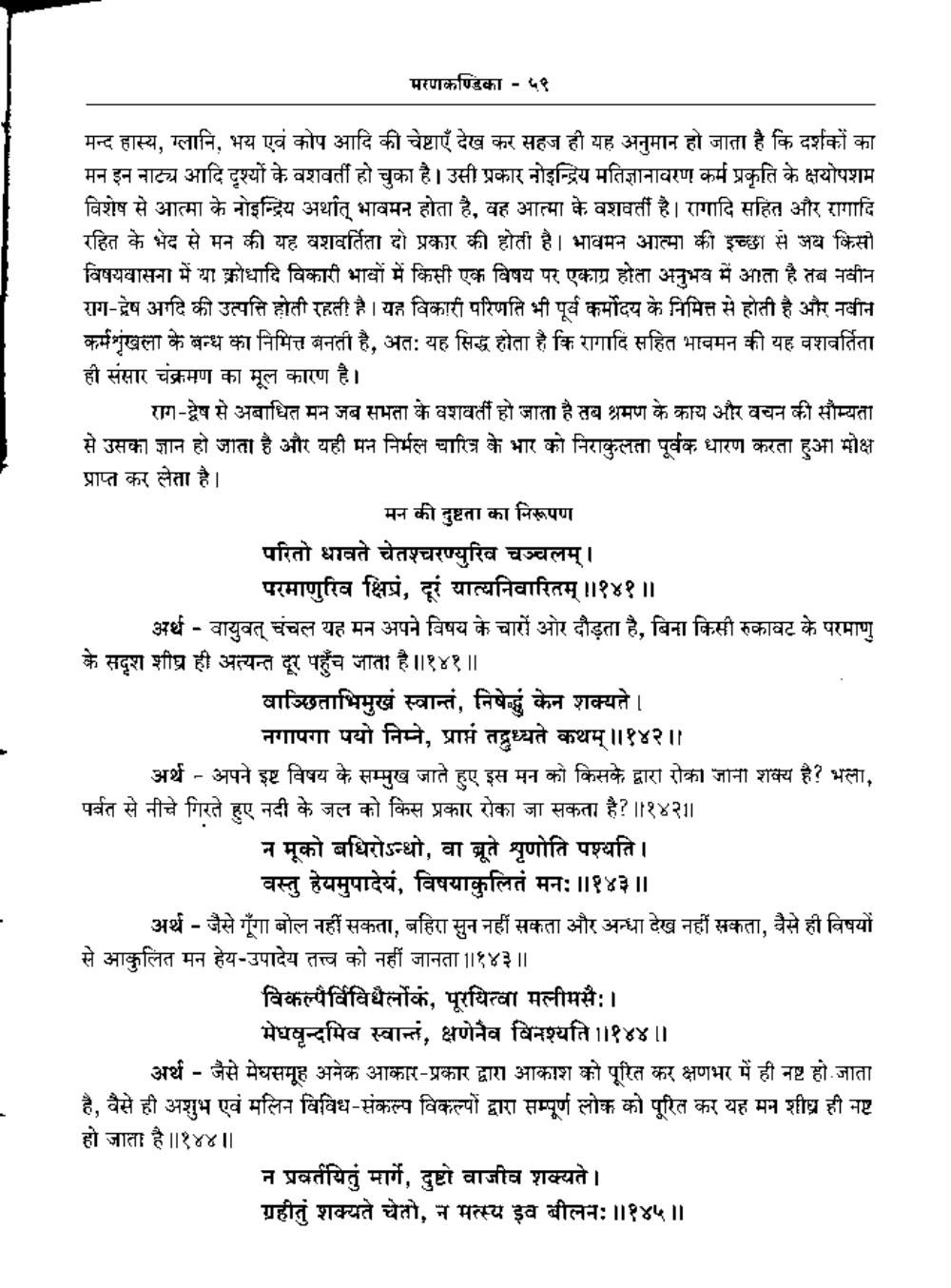________________
मरणकण्डिका - ५९
मन्द हास्य, ग्लानि, भय एवं कोप आदि की चेष्टाएँ देख कर सहज ही यह अनुमान हो जाता है कि दर्शकों का मन इन नाट्य आदि दृश्यों के वशवर्ती हो चुका है। उसी प्रकार नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण कर्म प्रकृति के क्षयोपशम विशेष से आत्मा के नोइन्द्रिय अर्थात् भावमन होता है, वह आत्मा के वशवर्ती है। रागादि सहित और रागादि रहित के भेद से मन की यह वशवर्तिता दो प्रकार की होती है। भावमन आत्मा की इच्छा से अब किसी विषयवासना में या क्रोधादि विकारी भावों में किसी एक विषय पर एकाग्र होता अनुभव में आता है तब नवीन राग-द्वेष अदि की उत्पत्ति होती रहती है । यह विकारी परिणति भी पूर्व कर्मोदय के निमित्त से होती है और नवीन कर्मशृंखला के बन्ध का निमित्त बनती है, अत: यह सिद्ध होता है कि रागादि सहित भावमन की यह वशवर्तिता ही संसार चंक्रमण का मूल कारण है।
राग-द्वेष से अबाधित मन जब सभता के वशवर्ती हो जाता है तब श्रमण के काय और वचन की सौम्यता से उसका ज्ञान हो जाता है और यही मन निर्मल चारित्र के भार को निराकुलता पूर्वक धारण करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
मन की दुष्टता का निरूपण परितो धावते चेतश्चरण्युरिव चञ्चलम् ।
परमाणुरिव क्षिप्रं, दूरं यात्यनिवारितम् ॥१४१॥ अर्थ - वायुवत् चंचल यह मन अपने विषय के चारों ओर दौड़ता है, बिना किसी रुकावट के परमाणु के सदृश शीघ्र ही अत्यन्त दूर पहुँच जाता है ।।१४१ ।।
वाञ्छिताभिमुखं स्वान्तं, निषेधुं केन शक्यते ।
नगापगा पयो निम्ने, प्राप्तं तद्रुध्यते कथम् ॥१४२ ।। ___ अर्थ - अपने इष्ट विषय के सम्मुख जाते हुए इस मन को किसके द्वारा रोका जाना शक्य है? भला, पर्वत से नीचे गिरते हुए नदी के जल को किस प्रकार रोका जा सकता है? ||१४२।।
न मूको बधिरोऽन्धो, वा ब्रूते शृणोति पश्यति ।
वस्तु हेयमुपादेयं, विषयाकुलितं मनः ।।१४३ ॥ अर्थ - जैसे गूंगा बोल नहीं सकता, बहिरा सुन नहीं सकता और अन्धा देख नहीं सकता, वैसे ही विषयों से आकुलित मन हेय-उपादेय तत्त्व को नहीं जानता ।।१४३ ।।
विकल्पैर्विविधैर्लोक, पूरयित्वा मलीमसैः।
मेघवृन्दमिव स्वान्तं, क्षणेनैव विनश्यति ।।१४४ ।। अर्थ - जैसे मेघसमूह अनेक आकार-प्रकार द्वारा आकाश को पूरित कर क्षणभर में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही अशुभ एवं मलिन विविध-संकल्प विकल्पों द्वारा सम्पूर्ण लोक को पूरित कर यह मन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।।१४४॥
न प्रवर्तयितुं मार्गे, दुष्टो वाजीव शक्यते। ग्रहीतुं शक्यते चेतो, न मत्स्य इव बीलनः॥१४५ ॥