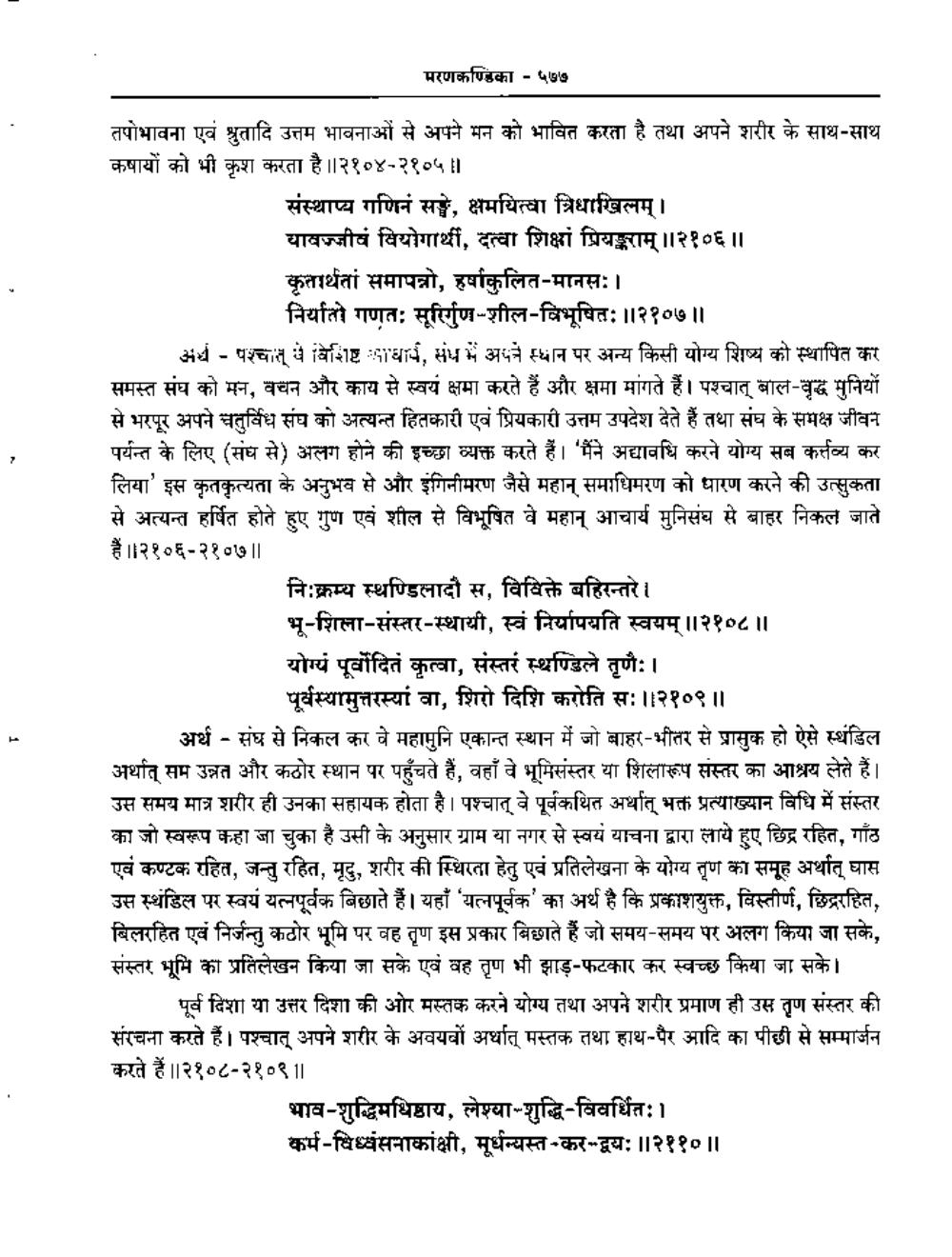________________
मरणकण्डिका- ५७७
तपोभावना एवं श्रुतादि उत्तम भावनाओं से अपने मन को भावित करता है तथा अपने शरीर के साथ-साथ कषायों को भी कृश करता है ।। २१०४-२१०५ ॥
संस्थाप्य गणिनं सङ्के, क्षमयित्वा त्रिधाखिलम् । यावज्जीवं वियोगार्थी, दत्वा शिक्षां प्रियङ्कराम् ।। २१०६ ।।
कृतार्थतां समापन, हर्षाकुलित-मानसः ।
निर्यात गणत: सूरिर्गुण-शील- विभूषितः ।। २१०७ ॥
अर्थ - पश्चात् विशिष्ट धार्य, संघ में अपने स्थान पर अन्य किसी योग्य शिष्य को स्थापित कर समस्त संघ को मन, वचन और काय से स्वयं क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। पश्चात् बाल-वृद्ध मुनियों से भरपूर अपने चतुर्विध संघ को अत्यन्त हितकारी एवं प्रियकारी उत्तम उपदेश देते हैं तथा संघ के समक्ष जीवन पर्यन्त के लिए (संघ से ) अलग होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। 'मैंने अद्यावधि करने योग्य सब कर्तव्य कर लिया' इस कृतकृत्यता के अनुभव से और इंगिनीमरण जैसे महान् समाधिमरण को धारण करने की उत्सुकता से अत्यन्त हर्षित होते हुए गुण एवं शील से विभूषित वे महान् आचार्य मुनिसंघ से बाहर निकल जाते हैं ।।२१०६-२१०७ ॥
निःक्रम्य स्थण्डिलादौ स, विविक्ते बहिरन्तरे ।
भू- शिला - संस्तर - स्थायी, स्वं निर्यापयति स्वयम् ।। २१०८ ।।
योग्यं पूर्वोदितं कृत्वा, संस्तरं स्थण्डिले तृणै: । पूर्वस्यामुत्तरस्यां वा, शिरो दिशि करोति सः ।। २१०९ ।।
अर्थ- संघ से निकल कर वे महामुनि एकान्त स्थान में जो बाहर भीतर से प्रासुक हो ऐसे स्थंडिल अर्थात् सम उन्नत और कठोर स्थान पर पहुँचते हैं, वहाँ वे भूमिसंस्तर या शिलारूप संस्तर का आश्रय लेते हैं। उस समय मात्र शरीर ही उनका सहायक होता है। पश्चात् वे पूर्वकथित अर्थात् भक्त प्रत्याख्यान विधि में संस्तर का जो स्वरूप कहा जा चुका है उसी के अनुसार ग्राम या नगर से स्वयं याचना द्वारा लाये हुए छिद्र रहित, गाँठ एवं कण्टक रहित, जन्तु रहित, मृदु, शरीर की स्थिरता हेतु एवं प्रतिलेखना के योग्य तृण का समूह अर्थात् घास उस स्थंडिल पर स्वयं यत्नपूर्वक बिछाते हैं। यहाँ 'यत्नपूर्वक' का अर्थ है कि प्रकाशयुक्त, विस्तीर्ण, छिद्ररहित, बिलरहित एवं निर्जन्तु कठोर भूमि पर वह तृण इस प्रकार बिछाते हैं जो समय-समय पर अलग किया जा सके, संस्तर भूमि का प्रतिलेखन किया जा सके एवं वह तृण भी झाड़-फटकार कर स्वच्छ किया जा सके।
पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मस्तक करने योग्य तथा अपने शरीर प्रमाण ही उस तृण संस्तर की संरचना करते हैं। पश्चात् अपने शरीर के अवयवों अर्थात् मस्तक तथा हाथ-पैर आदि का पीछी से सम्मार्जन करते हैं ।। २१०८-२१०९॥
भाव -शुद्धिमधिष्ठाय, लेश्या -शुद्धि-विवर्धित: ।
कर्म विध्वंसाकांक्षी, मूर्धन्यस्त- - कर-द्वयः ।।२११० ॥