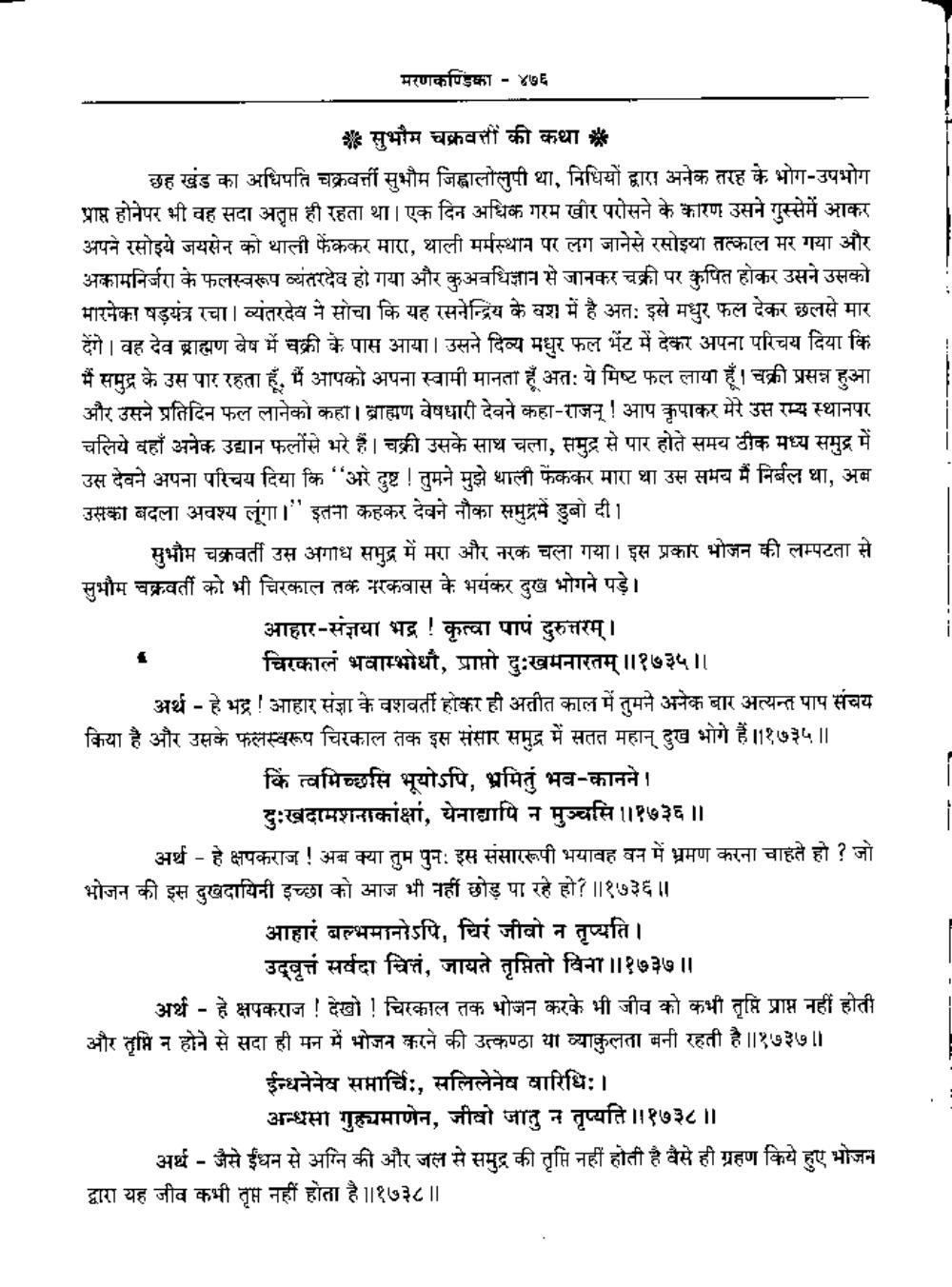________________
मरणकण्डिका - ४७६
* सुभौम चक्रवत्ती की कथा * छह खंड का अधिपति चक्रवर्ती सुभौम जिह्वालोलुपी था, निधियों द्वारा अनेक तरह के भोग-उपभोग प्राप्त होनेपर भी वह सदा अतृप्त ही रहता था। एक दिन अधिक गरम खीर परोसने के कारण उसने गुस्सेमें आकर अपने रसोइये जयसेन को थाली फेंककर मारा, थाली मर्मस्थान पर लग जानेसे रसोइया तत्काल मर गया और अकामनिर्जरा के फलस्वरूप व्यंतरदेव हो गया और कुअवधिज्ञान से जानकर चक्री पर कुपित होकर उसने उसको मारनेका षड़यंत्र रचा | व्यंतरदेव ने सोचा कि यह रसनेन्द्रिय के वश में है अतः इसे मधुर फल देकर छलसे मार देंगे । वह देव ब्राह्मण वेष में चक्री के पास आया। उसने दिव्य मधुर फल भेंट में देकर अपना परिचय दिया कि मैं समुद्र के उस पार रहता हूँ, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ अतः ये मिष्ट फल लाया हूँ। चक्री प्रसन्न हुआ और उसने प्रतिदिन फल लानेको कहा। ब्राह्मण वेषधारी देवने कहा-राजन् ! आप कृपाकर मेरे उस रम्य स्थानपर चलिये वहाँ अनेक उद्यान फलोंसे भरे हैं। चक्री उसके साथ चला, समुद्र से पार होते समय ठीक मध्य समुद्र में उस देवने अपना परिचय दिया कि "अरे दुष्ट ! तुमने मुझे थाली फेंककर मारा था उस समय मैं निर्बल था, अब उसका बदला अवश्य लूंगा।" इतना कहकर देवने नौका समुद्रमें डुबो दी।
सुभौम चक्रवर्ती उस अगाध समुद्र में मरा और नरक चला गया। इस प्रकार भोजन की लम्पटता से सुभौम चक्रवर्ती को भी चिरकाल तक नरकवास के भयंकर दुख भोगने पड़े।
आहार-संज्ञया भद्र ! कृत्वा पापं दुरुत्तरम्।
चिरकालं भवाम्भोधौ, प्राप्तो दुःखमनारतम् ।।१७३५ ।। अर्थ - हे भद्र ! आहार संज्ञा के वशवर्ती होकर ही अतीत काल में तुमने अनेक बार अत्यन्त पाप संचय किया है और उसके फलस्वरूप चिरकाल तक इस संसार समुद्र में सतत महान् दुख भोगे हैं।।१७३५ ।।
किं त्वमिच्छसि भूयोऽपि, भ्रमितुं भव-कानने।।
दुःखदामशनाकांक्षा, येनाधापि न मुञ्चसि ।।१७३६ ॥ अर्थ - हे क्षपकराज ! अब क्या तुम पुनः इस संसाररूपी भयावह वन में भ्रमण करना चाहते हो ? जो भोजन की इस दुखदायिनी इच्छा को आज भी नहीं छोड़ पा रहे हो? ||१७३६ ।।
आहारं बल्भमानरेऽपि, चिरं जीवो न तृप्यति ।
उद्वृत्तं सर्वदा चित्तं, जायते तृप्तितो विना ॥१७३७ ।। अर्थ - हे क्षपकराज ! देखो ! चिरकाल तक भोजन करके भी जीव को कभी तृप्ति प्राप्त नहीं होती और तृप्ति न होने से सदा ही मन में भोजन करने की उत्कण्ठा या व्याकुलता बनी रहती है।।१७३७ ।।
ईन्धनेनेव सप्तार्चिः, सलिलेनेव वारिधिः।
अन्धसा गुह्यमाणेन, जीवो जातु न तृप्यति ।।१७३८ ॥ अर्थ - जैसे ईंधन से अग्नि की और जल से समुद्र की तृप्ति नहीं होती है वैसे ही ग्रहण किये हुए भोजन द्वारा यह जीव कभी तृप्त नहीं होता है ||१७३८ ।।