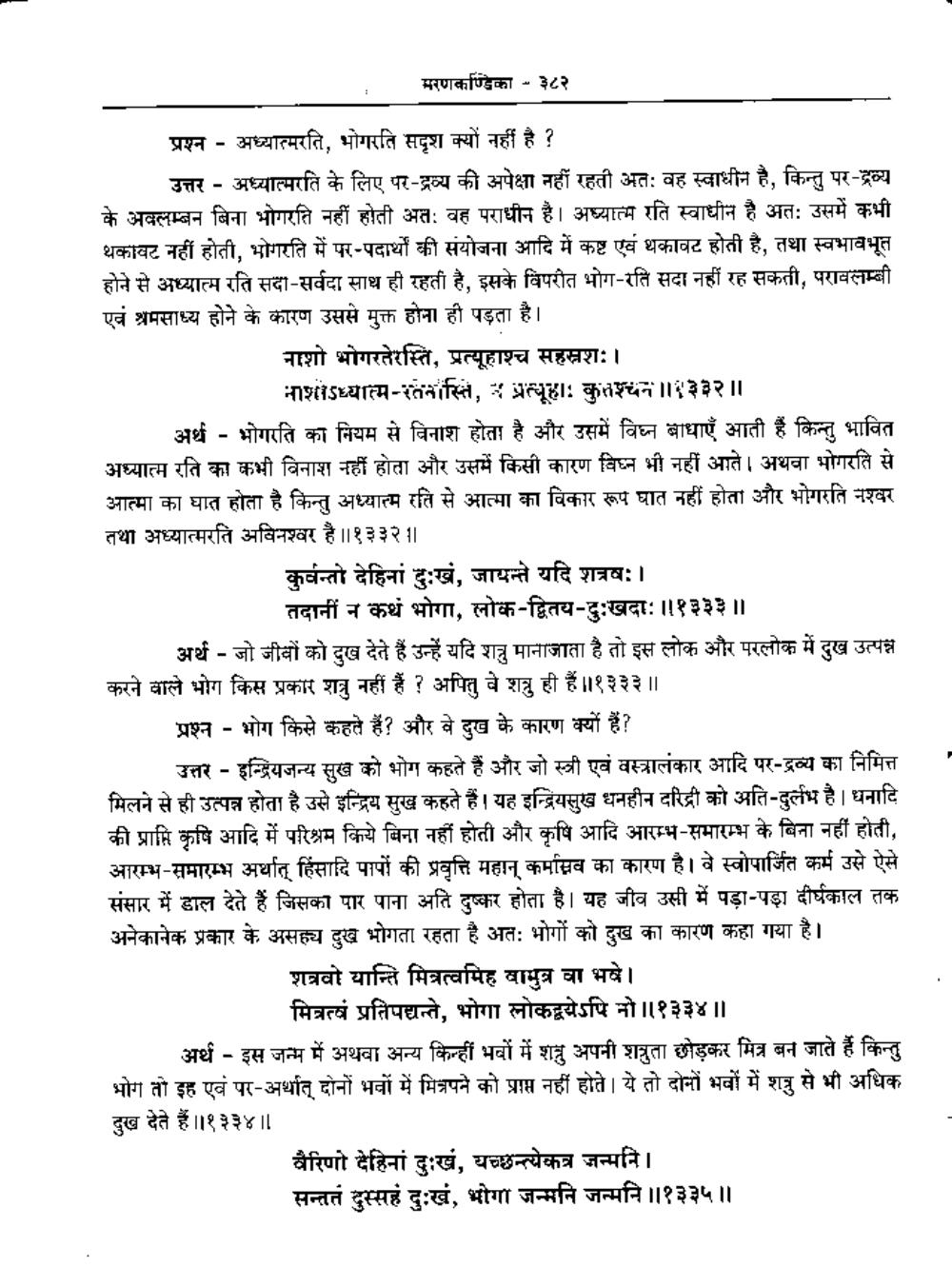________________
मरणकण्डिका - ३८२
प्रश्न - अध्यात्मरति, भोगरति सदृश क्यों नहीं है ?
उत्तर - अध्यात्मरति के लिए पर-द्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती अतः वह स्वाधीन है, किन्तु पर-द्रव्य के अवलम्बन बिना भोगरति नहीं होती अतः वह पराधीन है। अध्यात्म रति स्वाधीन है अतः उसमें कभी थकावट नहीं होती, भोगरति में पर-पदार्थों की संयोजना आदि में कष्ट एवं थकावट होती है, तथा स्वभावभूत होने से अध्यात्म रति सदा-सर्वदा साथ ही रहती है, इसके विपरीत भोग-रति सदा नहीं रह सकती, परावलम्बी एवं श्रमसाध्य होने के कारण उससे मुक्त होना ही पड़ता है।
नाशो भोगरतेरस्ति, प्रत्यूहाश्च सहस्रशः।
नाशाsध्यात्म-तनास्ति, अप्रत्यूहा: कुतश्चन ॥३३२ ।। अर्थ - भोगरति का नियम से विनाश होता है और उसमें विघ्न बाधाएँ आती हैं किन्तु भावित अध्यात्म रति का कभी विनाश नहीं होता और उसमें किसी कारण विघ्न भी नहीं आते। अथवा भोगरति से आत्मा का घात होता है किन्तु अध्यात्म रति से आत्मा का विकार रूप घात नहीं होता और भोगरति नश्वर तथा अध्यात्मरति अविनश्वर है।।१३३२।।
कुर्वन्तो देहिनां दुःखं, जायन्ते यदि शत्रषः।
तदानीं न कथं भोगा, लोक-द्वितय-दुःखदाः ।।१३३३॥ अर्थ - जो जीवों को दुख देते हैं उन्हें यदि शत्रु मानाजाता है तो इस लोक और परलोक में दुख उत्पन्न करने वाले भोग किस प्रकार शत्रु नहीं हैं ? अपितु वे शत्रु ही हैं॥१३३३ ॥
प्रश्न - भोग किसे कहते हैं? और वे दुख के कारण क्यों हैं?
उत्तर - इन्द्रियजन्य सुख को भोग कहते हैं और जो स्त्री एवं वस्त्रालंकार आदि पर-द्रव्य का निमित्त मिलने से ही उत्पन्न होता है उसे इन्द्रिय सुख कहते हैं। यह इन्द्रियसुख धनहीन दरिद्री को अति-दुर्लभ है। धनादि की प्रामि कृषि आदि में परिश्रम किये बिना नहीं होती और कृषि आदि आरम्भ-समारम्भ के बिना नहीं होती, आरम्भ-समारम्भ अर्थात् हिंसादि पापों की प्रवृत्ति महान् कर्मानव का कारण है। वे स्वोपार्जित कर्म उसे ऐसे संसार में डाल देते हैं जिसका पार पाना अति दुष्कर होता है। यह जीव उसी में पड़ा-पड़ा दीर्घकाल तक अनेकानेक प्रकार के असह्य दुख भोगता रहता है अतः भोगों को दुख का कारण कहा गया है।
शत्रवो यान्ति मित्रत्वमिह वामुत्र वा भषे।
मित्रत्वं प्रतिपद्यन्ते, भोगा लोकद्वयेऽपि नो।।१३३४ ॥ अर्थ - इस जन्म में अथवा अन्य किन्हीं भवों में शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर मित्र बन जाते हैं किन्तु भोग तो इह एवं पर-अर्थात् दोनों भवों में मित्रपने को प्राप्त नहीं होते। ये तो दोनों भवों में शत्रु से भी अधिक दुख देते हैं॥१३३४॥
वैरिणो देहिनां दुःखं, यच्छन्त्येकत्र जन्मनि । सन्ततं दुस्सहं दुःखं, भोगा जन्मनि जन्मनि ॥१३३५॥