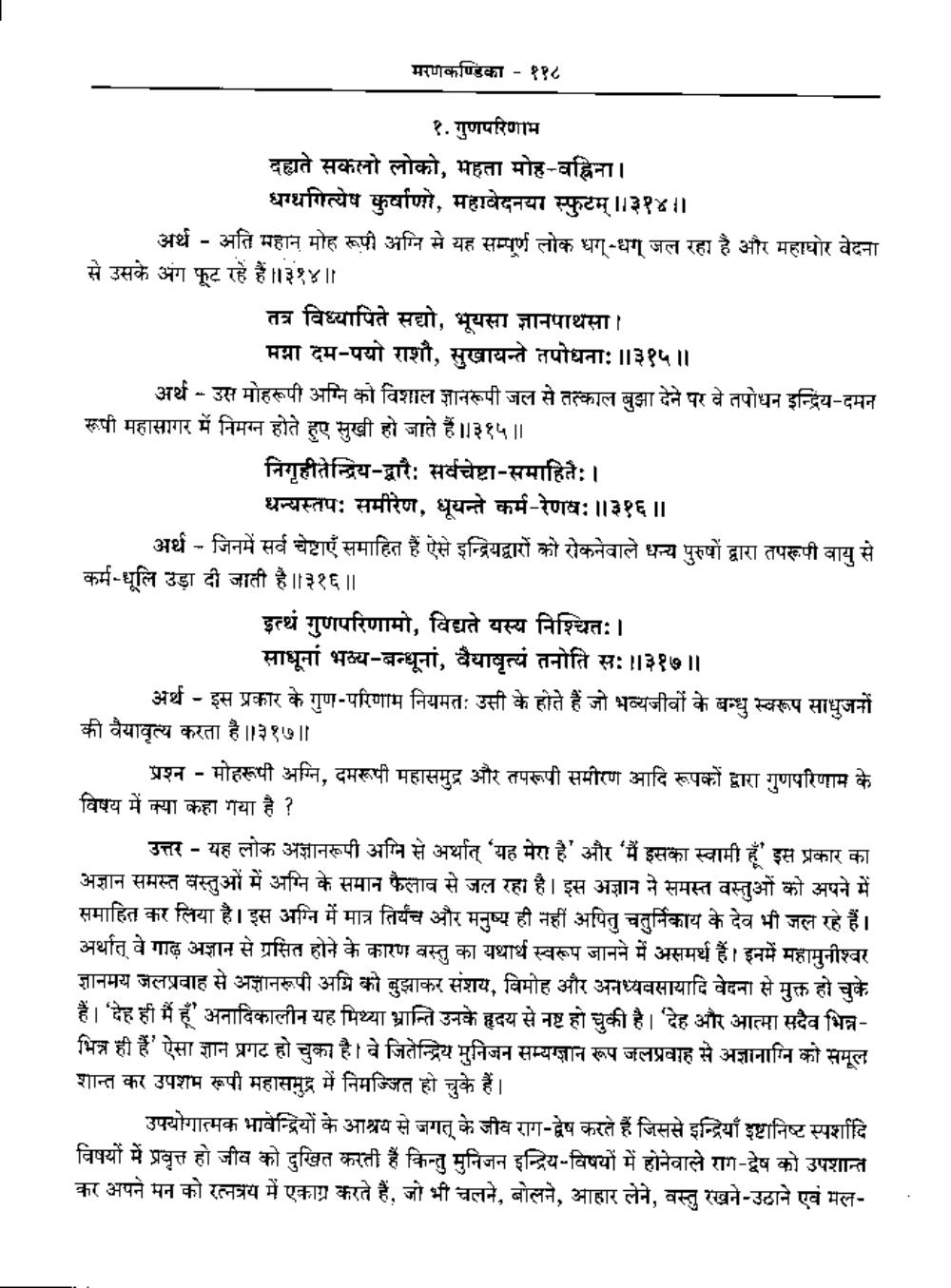________________
मरणकण्डिका - ११८
१. गुणपरिणाम
दाते सकलो लोको, महता मोह - वह्निना । धग्धगित्येष कुर्वाणो, महावेदनया स्फुटम् ।।३१४॥
अर्थ - अति महान मोह रूपी अग्नि से यह सम्पूर्ण लोक धग धग् जल रहा हैं और महाघोर वेदना से उसके अंग फूट रहें हैं ।। ३९४ ॥
तत्र विध्यापिते सद्यो, भूयसा ज्ञानपाथसा ।
मना दम-पयो राशौ, सुखायन्ते तपोधनाः ॥३१५॥
अर्थ - उस मोहरूपी अग्नि को विशाल ज्ञानरूपी जल से तत्काल बुझा देने पर वे तपोधन इन्द्रिय-दमन रूपी महासागर में निमग्न होते हुए सुखी हो जाते हैं॥ ३९५ ॥
निगृहीतेन्द्रिय-द्वारैः सर्वचेष्टा - समाहितैः ।
धन्यस्तपः समीरण, धूयन्ते कर्म - रेणवः ॥ ३१६ ॥
अर्थ - जिनमें सर्व चेष्टाएँ समाहित हैं ऐसे इन्द्रियद्वारों को रोकनेवाले धन्य पुरुषों द्वारा तपरूपी कर्म - धूलि उड़ा दी जाती है ॥ ३१६ ॥
इत्थं गुणपरिणामो, विद्यते यस्य निश्चित: ।
साधूनां भव्य बन्धूनां वैयावृत्यं तनोति सः ॥ ३१७ ॥
'वायु
से
अर्थ - इस प्रकार के गुण परिणाम नियमतः उसी के होते हैं जो भव्यजीवों के बन्धु स्वरूप साधुजनों की वैयावृत्य करता है ॥ ३१७ ॥
प्रश्न - मोहरूपी अग्नि, दमरूपी महासमुद्र और तपरूपी समीरण आदि रूपकों द्वारा गुणपरिणाम के विषय में क्या कहा गया है।
उत्तर
- यह लोक अज्ञानरूपी अग्नि से अर्थात् 'यह मेरा है' और 'मैं इसका स्वामी हूँ' इस प्रकार का अज्ञान समस्त वस्तुओं में अग्नि के समान फैलाव से जल रहा है। इस अज्ञान ने समस्त वस्तुओं को अपने में समाहित कर लिया है। इस अग्नि में मात्र तिर्यंच और मनुष्य ही नहीं अपितु चतुर्निकाय के देव भी जल रहे हैं। अर्थात् वे गाढ़ अज्ञान से ग्रसित होने के कारण वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने में असमर्थ हैं। इनमें महामुनीश्वर ज्ञानमय जलप्रवाह से अज्ञानरूपी अग्रि को बुझाकर संशय, विमोह और अनध्यवसायादि वेदना से मुक्त हो चुके हैं। 'देह ही मैं हूँ' अनादिकालीन यह मिथ्या भ्रान्ति उनके हृदय से नष्ट हो चुकी है। 'देह और आत्मा सदैव भिन्नभिन्न ही हैं' ऐसा ज्ञान प्रगट हो चुका है। वे जितेन्द्रिय मुनिजन सम्यग्ज्ञान रूप जलप्रवाह से अज्ञानाग्नि को समूल शान्त कर उपशम रूपी महासमुद्र में निमज्जित हो चुके हैं।
उपयोगात्मक भावेन्द्रियों के आश्रय से जगत् के जीव राग-द्वेष करते हैं जिससे इन्द्रियाँ इष्टानिष्ट स्पर्शादि विषयों में प्रवृत्त हो जीव को दुखित करती हैं किन्तु मुनिजन इन्द्रिय-विषयों में होनेवाले राग-द्वेष को उपशान्त कर अपने मन को रत्नत्रय में एकाग्र करते हैं, जो भी चलने, बोलने, आहार लेने, वस्तु रखने उठाने एवं मल