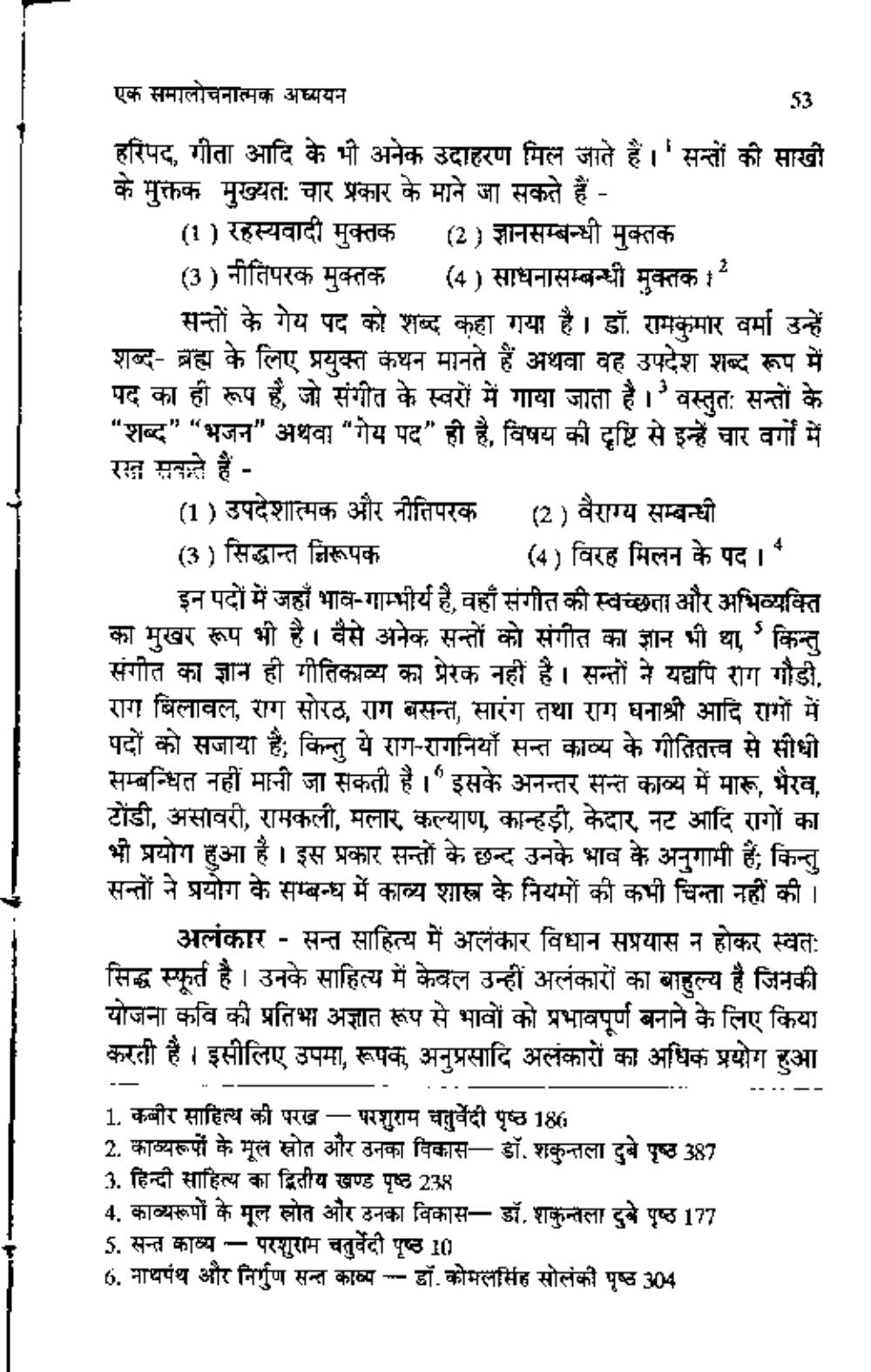________________
एक समालोचनात्मक अध्ययन
हरिपद, गीता आदि के भी अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। ' सन्तों की साखी के मुक्तक मुख्यत: चार प्रकार के माने जा सकते हैं -
(1 ) रहस्यवादी मुक्तक (2) ज्ञानसम्बन्धी मुक्तक (3 ) नीतिपरक मुक्तक (4) साधनासम्बन्धी मुक्तक
सन्तों के गेय पद को शब्द कहा गया है। डॉ. रामकुमार वर्मा उन्हें शब्द- ब्रह्म के लिए प्रयुक्त कथन मानते हैं अथवा वह उपदेश शब्द रूप में पद का ही रूप है, जो संगीत के स्वरों में गाया जाता है। वस्तुत: सन्तों के "शब्द" "भजन" अथवा "गेय पद" ही है, विषय की दृष्टि से इन्हें चार वर्गों में रस्त सकते हैं -
(1) उपदेशात्मक और नीतिपरक (2) वैराग्य सम्बन्धी (3 ) सिद्धान्त निरूपक (4) विरह मिलन के पद । ५
इन पदों में जहाँ भाव-गाम्भीर्य है, वहाँ संगीत की स्वच्छता और अभिव्यक्ति का मुखर रूप भी है। वैसे अनेक सन्तों को संगीत का ज्ञान भी था, किन्तु संगीत का ज्ञान ही गीतिकाव्य का प्रेरक नहीं है। सन्तों ने यद्यपि राग गौडी, राग बिलावल, राग सोरठ, राग बसन्त, सारंग तथा राग धनाश्री आदि रागों में पदों को सजाया है; किन्तु ये राग-रागनियाँ सन्त काव्य के गीतितत्व से सीधी सम्बन्धित नहीं मानी जा सकती है ।" इसके अनन्तर सन्त काव्य में मारू, भैरव, टोंडी, असावरी, रामकली, मलार, कल्याण, कान्हड़ी, केदार, नट आदि रागों का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार सन्तों के छन्द उनके भाव के अनुगामी हैं; किन्तु सन्तों ने प्रयोग के सम्बन्ध में कान्य शास्त्र के नियमों की कभी चिन्ता नहीं की।
अलंकार - सन्त साहित्य में अलंकार विधान सप्रयास न होकर स्वतः सिद्ध स्फूर्त है। उनके साहित्य में केवल उन्हीं अलंकारों का बाहुल्य है जिनकी योजना कवि की प्रतिभा अज्ञात रूप से भावों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया करती है । इसीलिए उपमा, रूपक, अनुप्रसादि अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ
1. कबीर साहित्य की परख – परशुराम चतुर्वेदी पृष्ठ 186 2. काव्यरूपों के मूल स्रोत और उनका विकास- डॉ. शकुन्तला दुबे पृष्ठ 387 3. हिन्दी साहित्य का द्वितीय खण्ड पृष्ठ 238 4. काव्यरूपों के मूल स्रोत और उनका विकास- डॉ. शकुन्तला दुबे पृष्ठ 177 5. सन्त काध्य - परशुराम चतुर्वेदी पृष्ठ 10 6. नाथपंथ और निर्गुण सन्त काव्य -- डॉ. कोमलसिंह सोलंकी पृष्ठ 304