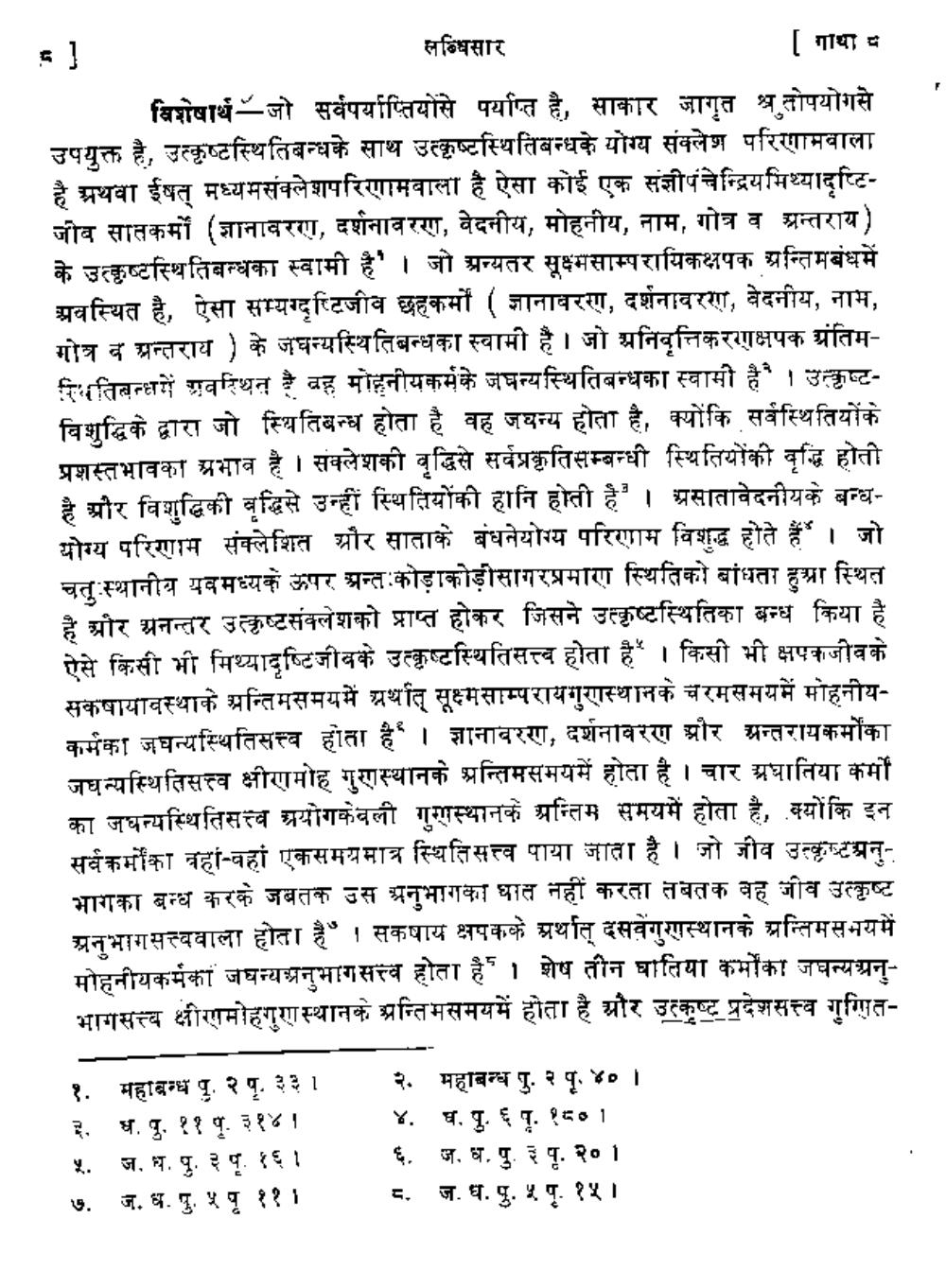________________
लब्धिसार
[ गाथा विशेषार्थ-जो सर्वपर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, उत्कृष्टस्थितिबन्धके साथ उत्कृष्टस्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामवाला है अथवा ईषत् मध्यमसंक्लेशपरिणामबाला है ऐसा कोई एक संज्ञीपंचेन्द्रियमिथ्यादृष्टिजीब सातकों (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र व अन्तराय) के उत्कृष्टस्थितिबन्धका स्वामी है' । जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्परायिकक्षपक अन्तिमबंधमें अवस्थित है, ऐसा सम्यग्दृष्टिजीव छहकर्मों ( ज्ञानाबरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र व अन्तराय ) के जघन्यस्थितिबन्धका स्वामी है। जो अनिवृत्तिकरणक्षपक अंतिमविपतिबन्ध में प्रवरिथन है वह मोहनीयकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । उत्कृष्टविशुद्धिके द्वारा जो स्थितिबन्ध होता है वह जघन्य होता है, क्योंकि सर्वस्थितियों के प्रशस्तभावका अभाव है । संक्लेशकी वृद्धिसे सर्वप्रकृतिसम्बन्धी स्थितियोंकी वृद्धि होती है और विशुद्धिकी वृद्धिसे उन्हीं स्थितियोंकी हानि होती है । असातावेदनीयके बन्धयोग्य परिणाम संक्लेशित और साताके बंधनेयोग्य परिणाम विशुद्ध होते हैं । जो चत स्थानीय यवमध्यके ऊपर अन्तःकोडाकोड़ीसागरप्रमाण स्थितिको बांधता हुआ स्थित है और अनन्तर उत्कृष्टसंक्लेशको प्राप्त होकर जिसने उत्कृष्टस्थितिका बन्ध किया है ऐसे किसी भी मिथ्यादष्टिजीवके उत्कृष्टस्थितिसत्त्व होता है । किसी भी क्षपकजीवके सकषायावस्थाके अन्तिमसमयमें अर्थात् सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानके चरमसमय में मोहनीयकर्मका जघन्यस्थितिसत्त्व होता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मोका जघन्यस्थितिसत्त्व क्षीणमोह गुणस्थानके अन्तिमसमयमें होता है । चार अघातिया कर्मों का जघन्यस्थितिसत्त्व अयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है, क्योंकि इन सर्वकर्मोंका वहां-वहां एकसमय मात्र स्थिति सत्त्व पाया जाता है । जो जीव उत्कृष्टअनभागका बन्ध करके जबतक उस अनुभागका घात नहीं करता तबतक वह जीव उत्कृष्ट अनभागसत्त्ववाला होता है । सकषाय क्षपकके अर्थात् दसवेंगुणस्थानके अन्तिमसमयमें मोहनीयकर्मका जघन्यअनुभागसत्त्व होता है। शेष तीन घातिया कर्मोका जघन्यअन्भागसत्त्व क्षीरगमोहगुणस्थानके अन्तिमसमयमें होता है और उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व गणित
१. महाबन्ध पु. २ पृ. ३३ । ३. ध. पु. ११ पृ. ३१४ । ५. ज. प. पु. ३ पृ. १६ । ७. ज.ध. पु. ५ पृ ११।
२. महाबन्ध पु. २ पृ.४० । ४. घ. पु. ६ पृ. १८० ६. ज. प. पु. ३ पृ. २०1 ८. ज.ध. पु. ५ पृ. १५ ।