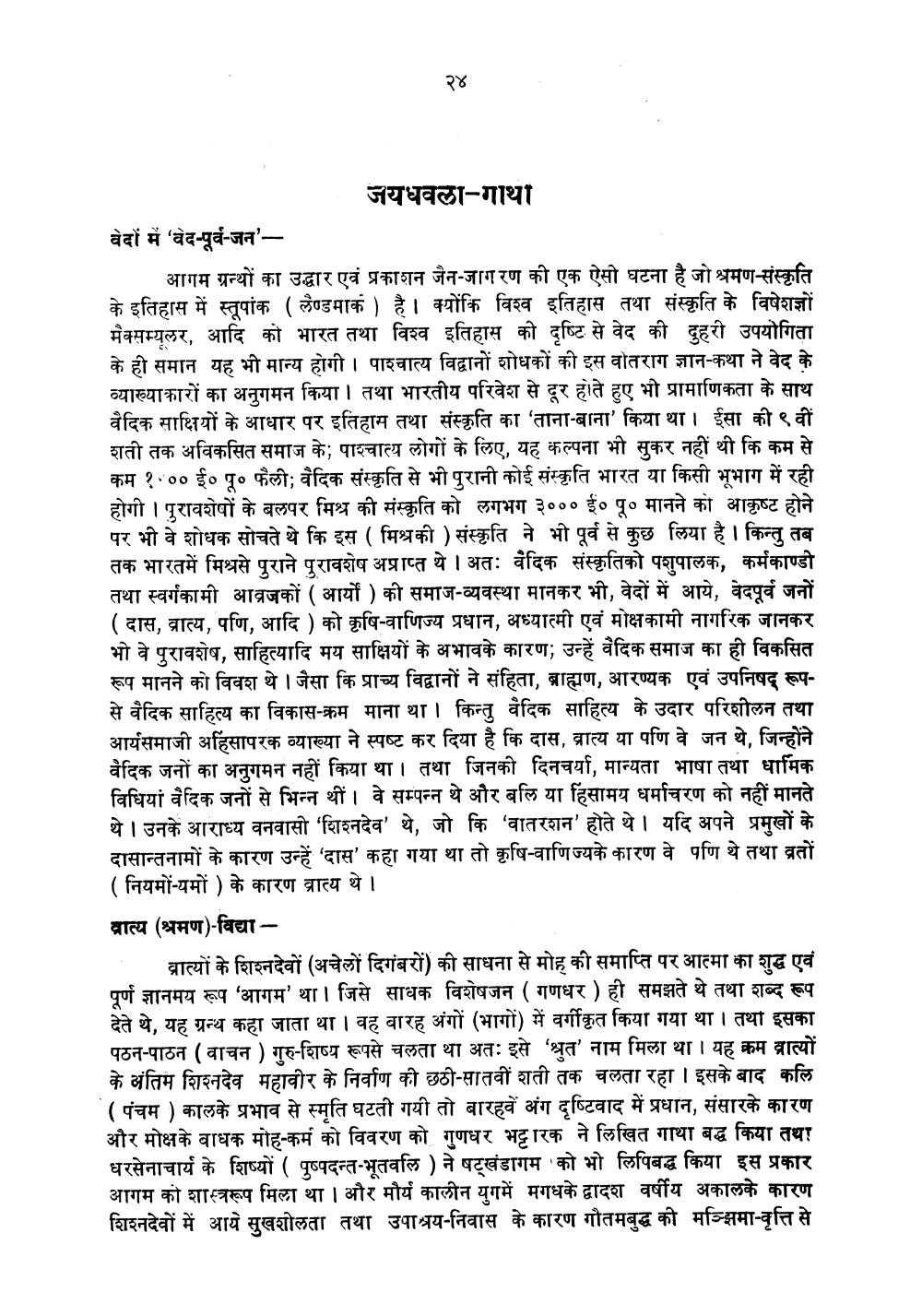________________
२४
जयधवला-गाथा वेदों में 'वेद-पूर्व-जन'
आगम ग्रन्थों का उद्धार एवं प्रकाशन जैन-जागरण की एक ऐसी घटना है जो श्रमण-संस्कृति के इतिहास में स्तूपांक ( लैण्डमाकं ) है। क्योंकि विश्व इतिहास तथा संस्कृति के विषेशज्ञों मैक्सम्युलर, आदि को भारत तथा विश्व इतिहास को दृष्टि से वेद की दुहरी उपयोगिता के ही समान यह भी मान्य होगी। पाश्चात्य विद्वानों शोधकों की इस वीतराग ज्ञान-कथा ने वेद के व्याख्याकारों का अनुगमन किया। तथा भारतीय परिवेश से दूर होते हुए भी प्रामाणिकता के साथ वैदिक साक्षियों के आधार पर इतिहास तथा संस्कृति का ताना-बाना' किया था। ईसा की ९ वीं शती तक अविकसित समाज के; पाश्चात्य लोगों के लिए, यह कल्पना भी सूकर नहीं थी कि कम से कम १.०० ई० पू० फैली; वैदिक संस्कृति से भी पुरानी कोई संस्कृति भारत या किसी भूभाग में रही होगी । पुरावशेषों के बलपर मिश्र की संस्कृति को लगभग ३००० ई० पू० मानने को आकृष्ट होने पर भी वे शोधक सोचते थे कि इस ( मिश्रकी ) संस्कृति ने भी पूर्व से कुछ लिया है । किन्तु तब तक भारतमें मिश्रसे पुराने पुरावशेष अप्राप्त थे । अतः वैदिक संस्कृतिको पशुपालक, कर्मकाण्डी तथा स्वर्गकामी आव्रजकों ( आर्यों ) की समाज-व्यवस्था मानकर भी, वेदों में आये, वेदपूर्व जनों ( दास, व्रात्य, पणि, आदि ) को कृषि-वाणिज्य प्रधान, अध्यात्मी एवं मोक्षकामी नागरिक जानकर भो वे पुरावशेष, साहित्यादि मय साक्षियों के अभावके कारण; उन्हें वैदिक समाज का ही विकसित रूप मानने को विवश थे । जैसा कि प्राच्य विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् रूपसे वैदिक साहित्य का विकास-क्रम माना था। किन्तु वैदिक साहित्य के उदार परिशीलन तथा आर्यसमाजी अहिंसापरक व्याख्या ने स्पष्ट कर दिया है कि दास, व्रात्य या पणि वे जन थे, जिन्होंने वैदिक जनों का अनुगमन नहीं किया था। तथा जिनकी दिनचर्या, मान्यता भाषा तथा धार्मिक विधियां वैदिक जनों से भिन्न थीं। वे सम्पन्न थे और बलि या हिंसामय धर्माचरण को नहीं मानते थे । उनके आराध्य वनवासी 'शिश्नदेव' थे, जो कि 'वातरशन' होते थे। यदि अपने प्रमुखों के दासान्तनामों के कारण उन्हें 'दास' कहा गया था तो कृषि-वाणिज्यके कारण वे पणि थे तथा व्रतों (नियमों-यमों) के कारण व्रात्य थे। व्रात्य (श्रमण)-विद्या
व्रात्यों के शिश्नदेवों (अचेलों दिगंबरों) की साधना से मोह की समाप्ति पर आत्मा का शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानमय रूप 'आगम' था। जिसे साधक विशेषजन ( गणधर ) ही समझते थे तथा शब्द रूप देते थे, यह ग्रन्थ कहा जाता था । वह बारह अंगों (भागों) में वर्गीकृत किया गया था। तथा इसका पठन-पाठन (वाचन ) गुरु-शिष्य रूपसे चलता था अतः इसे 'श्रुत' नाम मिला था। यह क्रम व्रात्यों के अंतिम शिश्नदेव महावीर के निर्वाण की छठी-सातवीं शती तक चलता रहा । इसके बाद कलि (पंचम ) कालके प्रभाव से स्मृति घटती गयी तो बारहवें अंग दृष्टिवाद में प्रधान, संसारके कारण और मोक्षके वाधक मोह-कर्म को विवरण को गुणधर भट्टारक ने लिखित गाथा बद्ध किया तथा धरसेनाचार्य के शिष्यों ( पुष्पदन्त-भूतवलि ) ने षट्खंडागम को भो लिपिबद्ध किया इस प्रकार आगम को शास्त्ररूप मिला था । और मौर्य कालीन युगमें मगधके द्वादश वर्षीय अकालके कारण शिश्नदेवों में आये सुखशोलता तथा उपाश्रय-निवास के कारण गौतमबुद्ध की मञ्झिमा-वृत्ति से