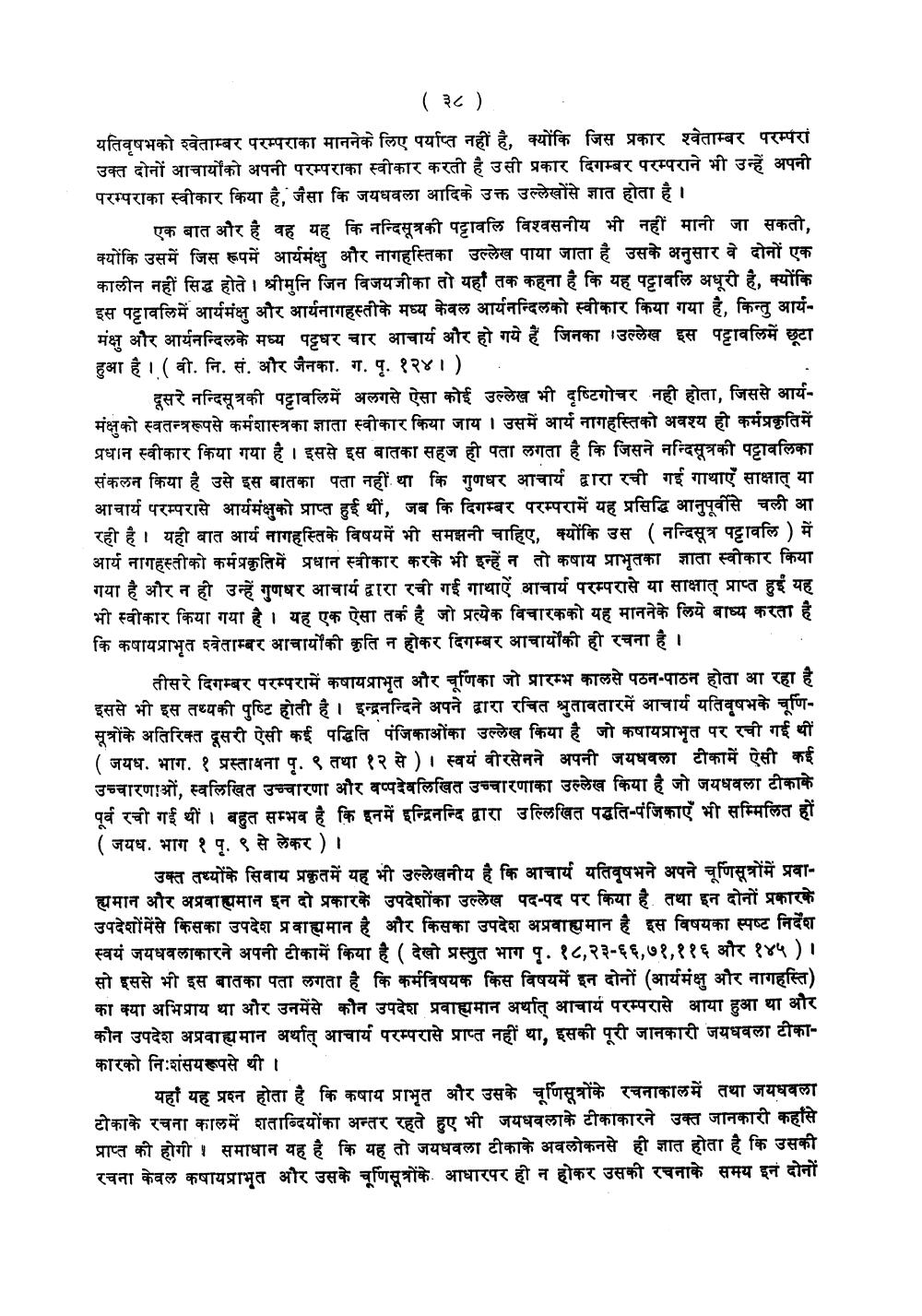________________
( ३८ )
यतिवृषभको श्वेताम्बर परम्पराका माननेके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा उक्त दोनों आचार्योंको अपनी परम्पराका स्वीकार करती है उसी प्रकार दिगम्बर परम्पराने भी उन्हें अपनी परम्पराका स्वीकार किया है, जैसा कि जयधवला आदिके उक्त उल्लेखोंसे ज्ञात होता है।
एक बात और है वह यह कि नन्दिसूत्रकी पट्टावलि विश्वसनीय भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसमें जिस रूपमें आर्यमंक्षु और नागहस्तिका उल्लेख पाया जाता है उसके अनुसार वे दोनों एक कालीन नहीं सिद्ध होते। श्रीमुनि जिन विजयजीका तो यहां तक कहना है कि यह पट्टावलि अधूरी है, क्योंकि इस पट्टावलिमें आर्यमंक्षु और आर्यनागहस्तीके मध्य केवल आर्यनन्दिलको स्वीकार किया गया है, किन्तु आर्यमंक्षु और आर्यनन्दिलके मध्य पट्टधर चार आचार्य और हो गये हैं जिनका ।उल्लेख इस पट्टावलिमें छुटा हुआ है । ( वी. नि. सं. और जैनका. ग. पृ. १२४ । ) .
दूसरे नन्दिसूत्रकी पट्टावलिमें अलगसे ऐसा कोई उल्लेख भी दृष्टिगोचर नही होता, जिससे आर्यमंक्षुको स्वतन्त्ररूपसे कर्मशास्त्रका ज्ञाता स्वीकार किया जाय । उसमें आर्य नागहस्तिको अवश्य ही कर्मप्रकृतिमें प्रधान स्वीकार किया गया है । इससे इस बातका सहज ही पता लगता है कि जिसने नन्दिसूत्रकी पट्टावलिका संकलन किया है उसे इस बातका पता नहीं था कि गणधर आचार्य द्वारा रची गई गाथाएँ सा आचार्य परम्परासे आर्यमंक्षुको प्राप्त हुई थीं, जब कि दिगम्बर परम्परामें यह प्रसिद्धि आनुपूर्वीसे चली आ रही है। यही बात आर्य नागहस्तिके विषयमें भी समझनी चाहिए, क्योंकि उस ( नन्दिसूत्र पट्टावलि ) में आर्य नागहस्तीको कर्मप्रकृति में प्रधान स्वीकार करके भी इन्हें न तो कषाय प्राभृतका ज्ञाता स्वीकार किया गया है और न ही उन्हें गुणधर आचार्य द्वारा रची गई गाथाएँ आचार्य परम्परासे या साक्षात् प्राप्त हुई यह भी स्वीकार किया गया है। यह एक ऐसा तर्क है जो प्रत्येक विचारकको यह माननेके लिये बाध्य करता है कि कषायप्राभृत श्वेताम्बर आचार्योंकी कृति न होकर दिगम्बर आचार्योंकी ही रचना है ।
तीसरे दिगम्बर परम्परामें कषायप्राभूत और चूर्णिका जो प्रारम्भ कालसे पठन-पाठन होता आ रहा है इससे भी इस तथ्यकी पुष्टि होती है। इन्द्रनन्दिने अपने द्वारा रचित श्रुतावतारमें आचार्य यतिवृषभके चूणिसूत्रोंके अतिरिक्त दूसरी ऐसी कई पद्धिति पंजिकाओंका उल्लेख किया है जो कषायप्राभूत पर रची गई थीं (जयध. भाग. १ प्रस्तावना पू. ९ तथा १२ से)। स्वयं वीरसेनने अपनी जयधवला टीकामें ऐसी कई उच्चारणाओं, स्वलिखित उच्चारणा और वप्पदेवलिखित उच्चारणाका उल्लेख किया है जो जयधवला टीकाके पूर्व रची गई थीं। बहुत सम्भव है कि इनमें इन्द्रिनन्दि द्वारा उल्लिखित पद्धति-पंजिकाएँ भी सम्मिलित हों ( जयध. भाग १ पृ. ९ से लेकर )।
उक्त तथ्योंके सिवाय प्रकृतमें यह भी उल्लेखनीय है कि आचार्य यतिवृषभने अपने चूर्णिसूत्रोंमें प्रवाह्यमान और अप्रवाहमान इन दो प्रकारके उपदेशोंका उल्लेख पद-पद पर किया है. तथा इन दोनों प्रकारके उपदेशोंसे किसका उपदेश प्रवाहमान है और किसका उपदेश अप्रवाहमान है इस विषयका स्पष्ट निर्देश स्वयं जयधवलाकारने अपनी टीकामें किया है ( देखो प्रस्तुत भाग पृ. १८,२३-६६,७१,११६ और १४५)। सो इससे भी इस बातका पता लगता है कि कर्मविषयक किस विषयमें इन दोनों (आर्यमंक्षु और नागहस्ति) का क्या अभिप्राय था और उनमेंसे कौन उपदेश प्रवाहमान अर्थात् आचार्य परम्परासे आया हुआ था और कौन उपदेश अप्रवाह्य मान अर्थात् आचार्य परम्परासे प्राप्त नहीं था, इसकी पूरी जानकारी जयधवला टीकाकारको निःशंसयरूपसे थी।
यहाँ यह प्रश्न होता है कि कषाय प्राभूत और उसके चूणिसूत्रोंके रचनाकालमें तथा जयधवला टोकाके रचना कालमें शताब्दियोंका अन्तर रहते हुए भी जयधवलाके टीकाकारने उक्त जानकारी कहाँसे प्राप्त की होगी। समाधान यह है कि यह तो जयधवला टीकाके अवलोकनसे ही ज्ञात होता है कि उसकी रचना केवल कषायप्राभूत और उसके चणिसूत्रोंके. आधारपर ही न होकर उसकी रचनाके समय इन दोनों