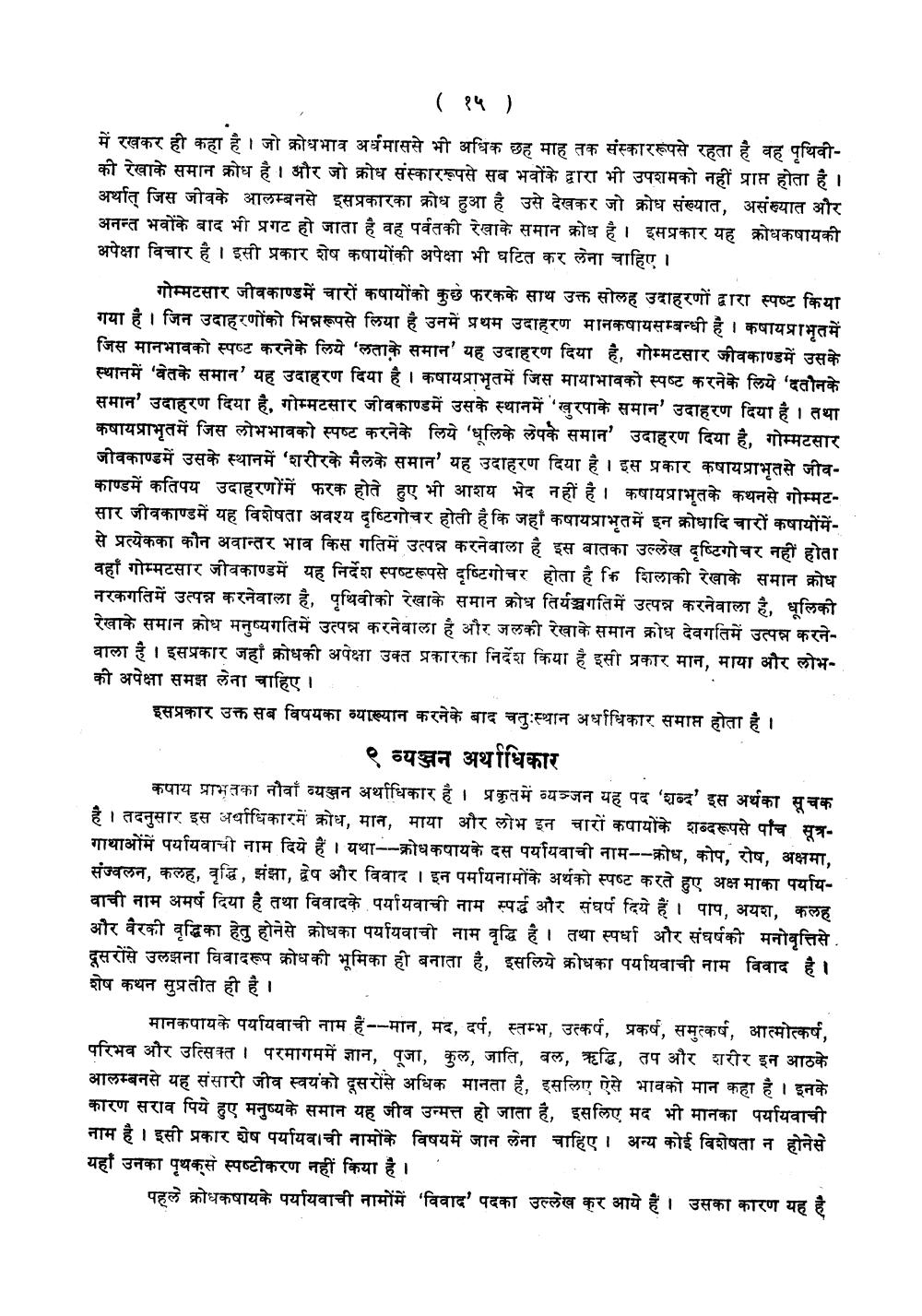________________
( १५ )
में रखकर ही कहा है। जो क्रोधभाव अर्धमाससे भी अधिक छह माह तक संस्काररूपसे रहता है वह पृथिवी - की रेखाके समान क्रोध है । और जो क्रोध संस्काररूपसे सब भवोंके द्वारा भी उपशमको नहीं प्राप्त होता है । अर्थात् जिस जीवके आलम्बनसे इसप्रकारका क्रोध हुआ है उसे देखकर जो क्रोध संख्यात, असंख्यात और अनन्त भवोंके बाद भी प्रगट हो जाता है वह पर्वतकी रेखाके समान क्रोध है । इसप्रकार यह क्रोधकषायकी अपेक्षा विचार है । इसी प्रकार शेष कषायोंकी अपेक्षा भी घटित कर लेना चाहिए |
गोम्मटसार जीवकाण्ड में चारों कषायोंको कुछे फरकके साथ उक्त सोलह उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है । जिन उदाहरणोंको भिन्नरूपसे लिया है उनमें प्रथम उदाहरण मानकषायसम्बन्धी है । कषायप्राभृतमें जिस मानभावको स्पष्ट करनेके लिये 'लताके समान' यह उदाहरण दिया है, गोम्मटसार जीवकाण्डमें उसके स्थानमें 'वेतके समान' यह उदाहरण दिया है। कषायप्राभृतमें जिस मायाभावको स्पष्ट करनेके लिये 'दतौनके समान' उदाहरण दिया है, गोम्मटसार जीवकाण्डमें उसके स्थानमें 'खुरपाके समान' उदाहरण दिया है। तथा कषायप्राभृत में जिस लोभभावको स्पष्ट करनेके लिये 'धूलिके लेपके समान' उदाहरण दिया है, गोम्मटसार जीवकाण्डमें उसके स्थान में 'शरीरके मैलके समान' यह उदाहरण दिया है। इस प्रकार कषायप्राभृतसे जीवकाण्डमें कतिपय उदाहरणों में फरक होते हुए भी आशय भेद नहीं है । कषायप्राभृतके कथनसे गोम्मटसार जीवकाण्ड में यह विशेषता अवश्य दृष्टिगोचर होती है कि जहाँ कषायप्राभृत में इन क्रोधादि चारों कषायोंमेंसे प्रत्येकका कौन अवान्तर भाव किस गतिमें उत्पन्न करनेवाला है इस बातका उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता वहाँ गोम्मटसार जीवकाण्डमें यह निर्देश स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर होता है कि शिलाकी रेखाके समान क्रोध नरकगति में उत्पन्न करनेवाला है, पृथिवीको रेखाके समान क्रोध तिर्यञ्च गति में उत्पन्न करनेवाला है, धूलिकी रेखाके समान क्रोध मनुष्यगति में उत्पन्न करनेवाला है और जलकी रेखाके समान क्रोध देवगतिमें उत्पन्न करनेवाला है । इसप्रकार जहाँ क्रोधकी अपेक्षा उक्त प्रकारका निर्देश किया है इसी प्रकार मान, माया और लोभकी अपेक्षा समझ लेना चाहिए ।
इस प्रकार उक्त सब विषयका व्याख्यान करनेके बाद चतुःस्थान अर्धाधिकार समाप्त होता है ।
९ व्यञ्जन अर्थाधिकार
कषाय प्राभूतका नौवाँ व्यञ्जन अर्थाधिकार है । प्रकृत में व्यञ्जन यह पद 'शब्द' इस अर्थका सूचक
है । तदनुसार इस अर्धाधिकारमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायोंके शब्दरूपसे पाँच सूत्रगाथाओं में पर्यायवाची नाम दिये हैं । यथा -- क्रोधकषायके दस पर्यायवाची नाम-क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, वृद्धि, झंझा, द्वेष और विवाद । इन पर्मायनामोंके अर्थको स्पष्ट करते हुए अक्ष माका पर्यायवाची नाम अमर्ष दिया है तथा विवादके पर्यायवाची नाम स्पर्द्ध और संघर्ष दिये हैं । पाप, अयश, कलह और वैरकी वृद्धिका हेतु होनेसे क्रोधका पर्यायवाची नाम वृद्धि है । तथा स्पर्धा और संघर्षकी मनोवृत्तिसे. दूसरोंसे उलझना विवादरूप क्रोध की भूमिका ही बनाता है, इसलिये क्रोधका पर्यायवाची नाम विवाद है । शेष कथन सुप्रतीत ही है ।
स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष,
मानकपाय के पर्यायवाची नाम हैं--मान, मद, दर्प, परिभव और उत्सिक्त । परमागममें ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, आलम्बनसे यह संसारी जीव स्वयंको दूसरोंसे अधिक मानता है, कारण सराव पिये हुए मनुष्य के समान यह जीव उन्मत्त हो जाता है, नाम है । इसी प्रकार शेष पर्यायवाची नामोंके विषय में जान लेना चाहिए । अन्य कोई विशेषता न होने से यहाँ उनका पृथक्से स्पष्टीकरण नहीं किया है।
बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके इसलिए ऐसे भावको मान कहा है । इनके इसलिए मद भी मानका पर्यायवाची
पहले क्रोधकषायके पर्यायवाची नामोंमें 'विवाद' पदका उल्लेख कर आये हैं । उसका कारण यह है