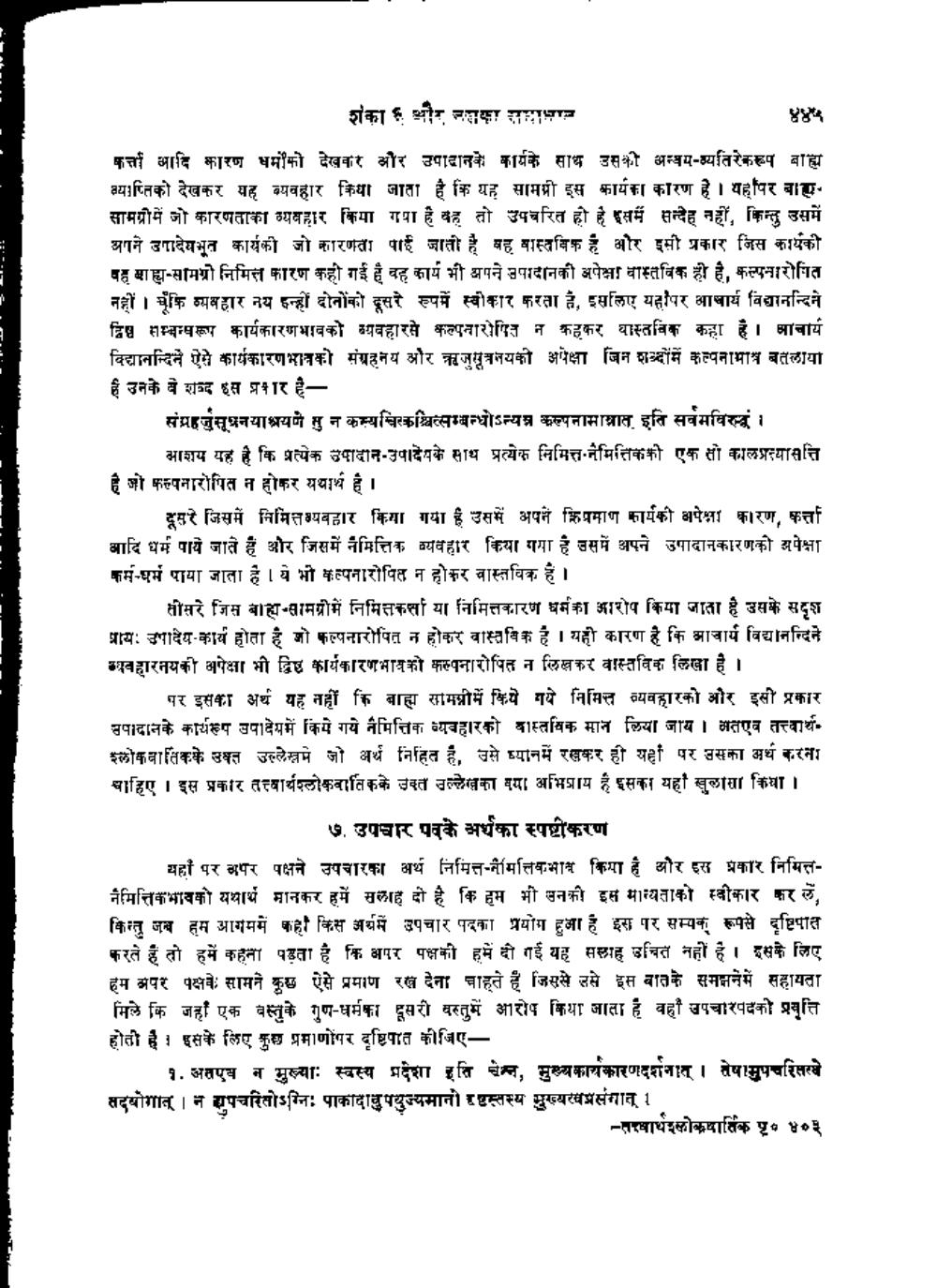________________
शंका और नाका सभा
कर्ता आदि कारण धर्माको देखकर और उपादानके कार्यके साथ उसकी अन्षय-व्यतिरेकरूप बाह्य व्याप्तिको देखकर यह व्यवहार किया जाता है कि यह सामग्री इस कार्यका कारण है। यहाँपर बाए. सामग्री में जो कारणताका व्यवहार किया गया है वह तो उपचरित हो है इसमें सन्देह नहीं, किन्तु उसमें अपने उपादेयभूत कार्यकी जो कारणता पाई जाती है वह वास्तविक है और इसी प्रकार जिस कार्यकी वह बाह्य-सामग्री निमित्त कारण कही गई है वह कार्य भी अपने उपादानकी अपेक्षा वास्तविक ही है, कल्पनारोनित नहीं। चूंकि व्यवहार नय इन्हीं दोनोंको दूसरे रूपमें स्वीकार करता है, इसलिए यहाँपर भाचार्य विद्यानन्दिने द्विष्ठ सम्बन्ध रूप कार्यकारणभावको व्यवहारसे कल्पनारोपित न कहकर घास्तविक कहा है। प्राचार्य विद्यानन्दिने ऐसे कार्यकारणभात्रको संग्रहनय और ऋजसूत्रनयको अपेक्षा जिन शब्दों में कल्पनामात्र बतलाया है उनके वे शब्द इस प्रकार है
संग्रहर्जुसूप्रनयाश्रयणे मु न कस्यविस्कश्चित्सम्बन्धोऽन्यन्न कल्पनामानात इति सर्वमविस्वं ।
आशय यह है कि प्रत्येक उपादान-उपादेयके साथ प्रत्येक निमित्त-नैमित्तिकको एक तो कालप्रत्यासत्ति है जो कल्पनारोपित न होकर यथार्थ है।
दूसरे जिसमें निमित्तव्यबहार किया गया है उसमें अपने क्रिप्रमाण कार्यको अपेक्षा कारण, कर्ता आदि धर्म पाये जाते है और जिसमें नैमित्तिक व्यवहार किया गया है उसमें अपने उपादानकारणको अपेक्षा कर्म-धर्म पाया जाता है । ये भी कल्पनारोपित न होकर वास्तविक है।
तीसरे जिस बाहा-सामग्रीमें निमित्तका या निमित्तकारण धर्म का आरोप किया जाता है उसके सदृश प्रायः उपादिय-कार्य होता है जो कल्पनारोपित न होकर वास्तविक है। यही कारण है कि आचार्य विद्यानन्दिने यवहारमयकी अपेक्षा भी द्विष्ठ कार्यकारणभावको कल्पनारोपित न लिखकर वास्तविक लिखा है।
पर इसका अर्थ यह नहीं कि बाह्म सामग्री में किये गये निमित्त व्यवहारको और इसी प्रकार अपादानके कार्यरूप उपादेयमें किये गये नैमित्तिक व्यवहारको वास्तविक मान लिया जाय । अतएव तत्त्वार्थश्लोकवातिकके उषत उल्लेनमे जो अर्थ निहित है, उसे ध्यान में रखकर ही यहां पर उसका अर्थ करना चाहिए । इस प्रकार तत्त्वार्थश्लोकवाति कके उक्त उल्लेखका क्या अभिप्राय है इसका यहाँ खुलासा किया।
७. उपचार पक्के अर्थका स्पष्टीकरण यहाँ पर अपर पक्षने उपचारका अर्थ निमित्त-नमित्तिवाभाव किया है और इस प्रकार निमित्तनैमित्तिकभावको यथार्थ मानकर हमें सलाह दी है कि हम भी उनकी इस मान्यताको स्वीकार कर लें, किन्तु जब हम आगममें कहो किस अर्थमें उपचार पदका प्रयोग हुआ है इस पर सम्पक रूपसे दृष्टिपात करते है तो हमें कहना पड़ता है कि अपर पक्षकी हमें दी गई यह सलाह उचित नहीं है। इसके नि हम अपर पक्षके सामने कुछ ऐसे प्रमाण रख देना चाहते हैं जिससे उसे इस बात समझने में सहायता मिले कि जहाँ एक बस्तुके गुण-धर्मका दूसरी वस्तुमें आरोप किया जाता है वहाँ उपचारपदको प्रवृत्ति होती है। इसके लिए कुछ प्रमाणोंपर दृष्टिपात कीजिए
१. असएष न मुख्याः स्वस्य प्रदेशा इति चेन्न, मुख्यकार्यकारणदर्शनात् । तेषामुपचरितरखे सदयोगात् । न गुपचरितोऽग्निः पाकादानुपयुज्यमानी रष्टस्तस्य मुख्यरवप्रसंगात ।
-तरवार्थश्लोकवार्तिक पृ० ४.३