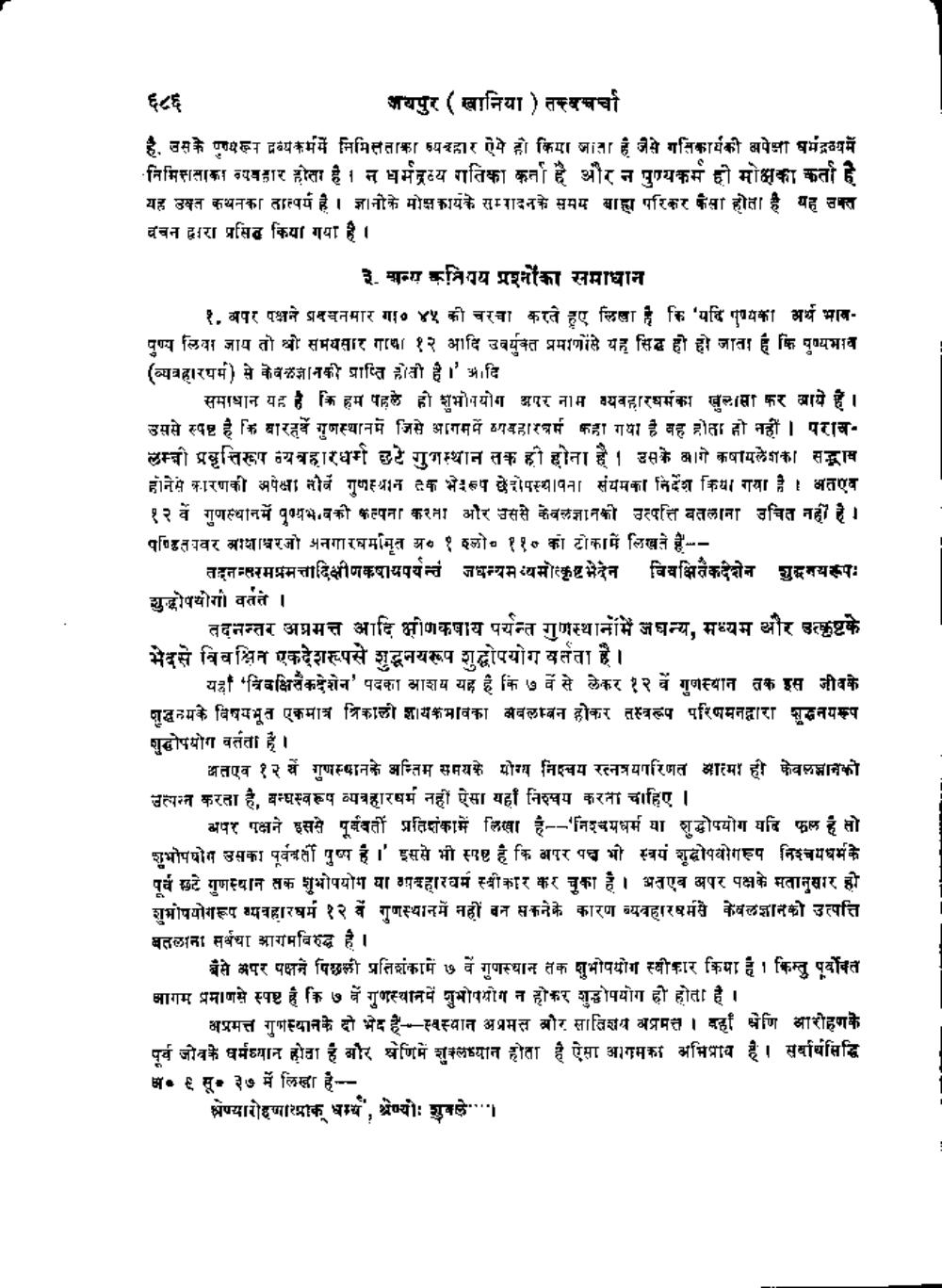________________
६८६
जयपुर (खानिया ) तर्चा
है. उसके पुण्यरून द्रव्यकर्ममें निमितताका व्यवहार ऐसे ही किया जाता है जैसे गतिकार्यको अपेक्षा द्रव्यमें मिलाका व्यवहार होता है । न धर्मद्रव्य गतिका कर्ता है और न पुण्यकर्म हो मोक्षका कर्ता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । ज्ञानके मोक्षकार्यके सम्पादन के समय बाह्य परिकर कैसा होता है यह समत वचन द्वारा प्रसिद्ध किया गया है।
३. मान्य कतिपय प्रश्नोंका समाधान
१. अपर पचने प्रवचनमार गा० ४५ की चरचा करते हुए लिखा है कि 'यदि पुण्यका अर्थ भावपुण्य लिया जाय तो श्रो समयसार गाथा १२ आदि उपर्युक्त प्रमाणों यह सिद्ध हो हो जाता है कि पुण्यभाव ( व्यवहारधर्म) से केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है।' आदि
समाधान यह है कि हम पहले हो शुभोगयोग अपर नाम व्यवहारधर्मका खुलासा कर खाये है। उससे स्पष्ट है कि बारहवें गुणस्थानमें जिसे आगम में व्यवहारचर्म कहा गया है वह होता हो नहीं । परावलम्बी प्रवृत्तिरूप व्यवहारधर्म छटे गुणस्थान तक ही होता है । उसके आगे कषायलेशका सद्भाव हॉनेस कारणकी अपेक्षा नोर्वे गुणस्थान तक भेरूप छेोपस्थापना संयमका निर्देश किया गया है। अतएव १२ वे गुणस्थान में दुष्प्रभाव की कल्पना करना और उससे केवलज्ञानको उत्पत्ति बतलाना उचित नहीं है । पण्डितवर अश्शावरजो अनगारधर्मामृत अ० १ श्लो० ११० को टोका में लिखते हैं-तदनन्तरमप्रमत्तादिक्षीणकषायपर्यन्तं जघन्यमव्यमोत्कृष्टभेदेन
विवक्षितैकदेशेन शुद्धमयरूपः
शुद्धोपयोगी वर्तते ।
तदनन्तर अप्रमत्त आदि क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थानों में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदविवक्षित एकदेशरूपसे शुद्धनयरूप शुद्धोपयोग वर्तता है।
यहाँ 'त्रिक्षिकदेशेन ' पदका आशय यह है कि ७ वें से लेकर १२ वें गुणस्थान तक इस जीवके शुन्यके विषयभूत एकमात्र त्रिकाली शायकमावका अवलम्बन होकर तस्त्ररूप परिणमनद्वारा शुद्धनयरूप शुद्धोपयोग वर्तता है।
अतएव १२ में गुणस्थानके अन्तिम समयके योग्य निश्चय रत्नत्रयपरिणत आत्मा ही केवलज्ञानको उत्पन्न करता है, बन्धस्वरूप व्यवहारधर्म नहीं ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए ।
अपर पक्ष इससे पूर्ववर्ती प्रतिशंकामें लिखा है- 'निश्चयधर्म या शुद्धोपयोग यदि फल है तो शुभयोग उसका पूर्ववर्ती पुष्प है।' इससे भी स्पष्ट है कि अपर पक्ष भी स्वयं वृद्धोपयोगरूप निश्चयधर्म के पूर्व छटे गुणस्थान तक शुभोपयोग या आहारवर्म स्वीकार कर चुका है। अतएव अपर पक्ष के मतानुसार हो शुभयोगरूप व्यवहारमं १२ में गुणस्थानमें नहीं बन सकने के कारण व्यवहारमंसे केवलज्ञानको उत्पत्ति बतलाना सर्वथा आगमविरुद्ध है ।
जैसे अपर पक्षने पिछली प्रतिशंकामे ७ वे गुणस्थान तक शुभोपयोग स्वीकार किया है । किन्तु पूर्वोक्त आागम प्रमाणसे स्पष्ट है कि ७ वे गुणस्थानमें शुभोपयोग न होकर शुद्धोपयोग हो होता है ।
अप्रमत्त गुणस्थानके दो भेद हैं--- स्वस्थान अप्रमत और सातिशय अप्रमत्त। वहीं श्रेणि आरोहण के पूर्व जीवके धर्मध्यान होता है और श्रेणिमें शुक्लध्यान होता है ऐसा आगमका अभिप्राय है । सर्वार्थसिद्धि असू. २७ में लिखा है-
श्रेण्यारोहणास्प्राक् धर्म्यं श्रेण्योः शुक्ले"।