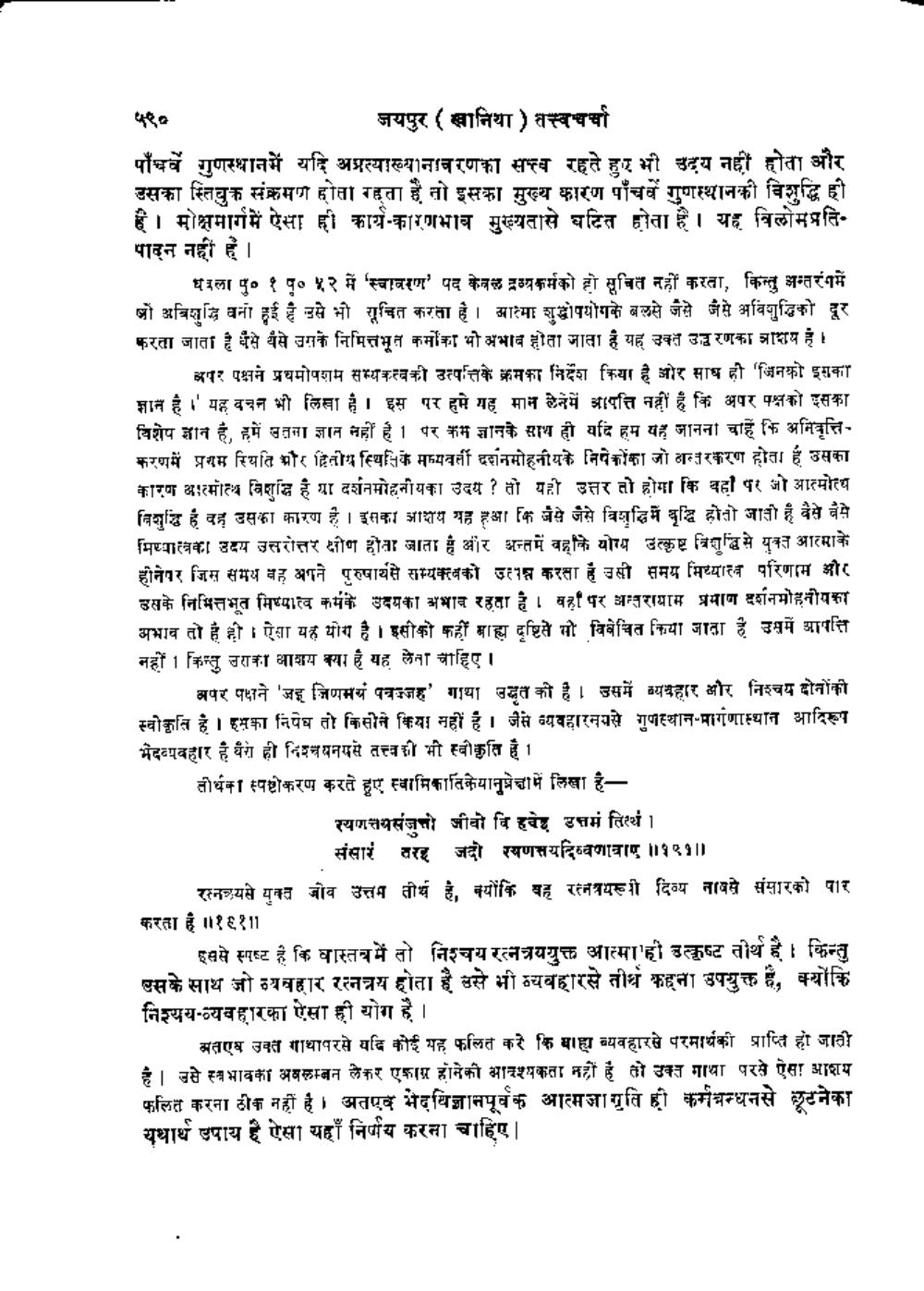________________
जयपुर (खानिया) तत्वचर्चा पाँचवे गुणस्थानमें यदि अप्रत्याख्यानाचरणका सत्व रहते हुए भी उदय नहीं होता और उसका स्तिबुक संक्रमण होता रहता है तो इसका मुख्य कारण पाँचवें गुणस्थानकी विशुद्धि हो है। मोक्षमार्गमें ऐसा ही कार्य-कारणभाव मुख्यतासे घटित होता है। यह विलोमप्रतिपादन नहीं है।
धवला पु० १ पृ० ५.२ में 'स्वावरण' पद केवल द्रव्यकर्मको हो सूचित नहीं करता, किन्तु अन्तरंगमें सो अबिशुद्धि बनी हुई है उसे भी गूचित करता है। आत्मा शुद्धोपयोगके बलसे जैसे जैसे अविशुद्धिको दूर करता जाता है धैसे वैसे उसके निमित्तभूत कर्मों का भो अभाव होता जाता है यह उक्त उवरणका त्राशय है।
अपर पक्षने प्रथमोपशम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके क्रमका निर्देश किया है और साथ ही जिनको इसका मान है।' यह वचन भी लिखा है। इस पर हमे यह मान लेनमें आपत्ति नहीं है कि अपर पक्षको इसका विशेष ज्ञान है, हमें उतना ज्ञान नहीं है । पर कम ज्ञानके साथ ही यदि हम यह जानना चाहें कि अनिवृत्तिकरणमें प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति के मध्यवर्ती ददानमोहनीयके निषकोंका जो अन्तरकरण होता है उसका कारण आत्मोत्व विशुद्धि है या दर्शनमोहनीयका उदय ? तो यही उत्तर तो होगा कि वहां पर जो आत्मोत्थ विशुद्धि है वह उसका कारण है । इसका आशय यह हआ कि जैसे जैसे विद्धि में वृद्धि होतो जाती है वैसे वैसे मिथ्यात्त्रका उदय उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है और अन्तमें वाँके योग्य उत्कृष्ट विशुद्धि से युक्त आत्माके होनेपर जिस समय वह अपने पुरुषार्थसे सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है उसी समय मिथ्यात्न परिणाम और उसके निमित्तभूत मिथ्यात्व कर्मके उदयका अभाव रहता है। वहीं पर अन्तरायाम प्रमाण दर्शनमोहनीयका अभाव तो है ही। ऐशा यह योग है । इसीको कहीं बाह्य दृष्टि से मो विवेचित किया जाता है उसमें आपत्ति नहीं । किन्तु उराका आशय क्या है यह लेना चाहिए ।
___ अपर पक्षने 'जह जिष्णमयं पवजह' गाथा उद्धत को है। उसमें व्यवहार और निश्चय दोनोंकी स्वीकृति है। इसका निषेध तो किसीने किया नहीं है। जैसे व्यवहारमयसे गुणस्थान-मागणास्थान आदिरूप भेदपवहार है घेरा ही निश्च यनयसे तत्त्व की भी स्वीकृति है। तीर्थका स्पष्टीकरण करते हुए स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है
स्यगत्तयसंजत्तो जीवो वि हवेई उसमं तिथं ।
संसार तरह जदो रयणसयदिव्वणावाए ॥११॥ रत्नन्यसे युक्त जीव उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह रत्नत्रयरूपी दिव्य नाषसे संसारको पार करता है ॥१६॥
इससे स्पष्ट है कि वास्तव में तो निश्चय रत्नत्रययुक्त आत्मा'ही उत्कृष्ट तीर्थ है। किन्तु उसके साथ जो व्यवहार रत्नत्रय होता है उसे भी व्यवहारसे तीर्थ कहना उपयुक्त है, क्योंकि निश्यय व्यवहारका ऐसा ही योग है।
अतएव उक्त गाथापरसे यदि कोई यह फलित करे कि बाह्य व्यवहारसे परमार्थकी प्राप्ति हो जाती है। उसे स्त्र भावका अबलम्बन लेकर एकान होने की आवश्यकता नहीं है तो उक्त माथा परसे ऐसा आशय फलित करना ठीक नहीं है । अतएव भेद विज्ञानपूर्वक आत्मजा गृति ही कर्मबन्धनसे छूटनेका यथार्थ उपाय है ऐसा यहाँ निर्णय करना चाहिए |