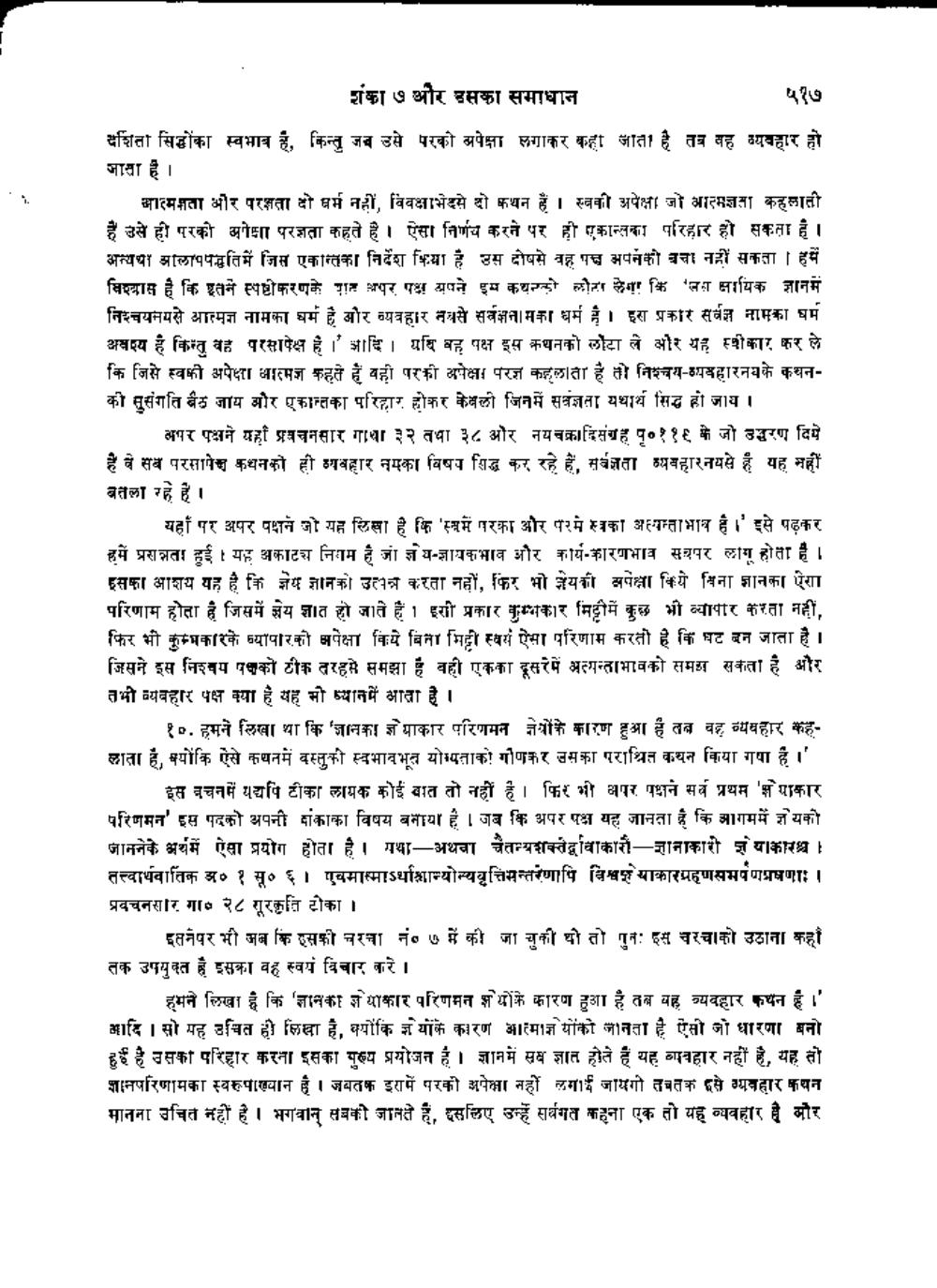________________
शंका ७ और उसका समाधान दशिता सिद्धोंका स्वभाव है, किन्तु जब उसे परको अपेक्षा लगाकर कहा जाता है तब वह व्यवहार हो जाता है।
आत्ममता और परमता दो धर्म नहीं, विवक्षाभेदसे दो कथन हैं। स्ववी अपेक्षा जो आत्मज्ञसा कहलाती है उसे ही परको अक्षा परज्ञता कहते है। ऐसा निर्णय करने पर ही एकान्लन्दा परिहार हो सकता है। अन्यथा आलापपद्धति में जिस एकान्तका निर्देश किया है उस दोषसे वह पम्म अपनको बचा नहीं सकता । हमें विश्वास है कि इतने स्पष्टीकरणके बाट अपर पक्ष अपने इस कथरलो लौटा लेगा कि 'सामायिक ज्ञानमें निश्चयनयसे आत्मज्ञ नामका धर्म है और व्यवहार नबसे सर्वनामका धर्म है। इस प्रकार सर्वज्ञ नामका धर्म अवश्य है किन्तु वह परसापेक्ष है।' आदि। यदि वह पक्ष इस कथनको लोटा ले और यह स्वीकार कर ले कि जिसे स्वकी अपेक्षा आत्मज्ञ कहते हैं वही परकी अपेक्षा परज्ञ कहलाता है तो निश्चय-व्यवहारनय के कथनकी सुसंगति बैठ जाय और एकान्तका परिहार होकर केवली जिनमें सर्वज्ञता यथार्थ सिद्ध हो जाय ।
अपर पक्षने यहाँ प्रवचनसार गाथा ३२ तथा ३८ और नय चक्रादिसंग्रह पृ०११६ के जो उसरण दिये है वे सब परसापेक्ष कथनको ही व्यवहार नयका विषय सिद्ध कर रहे हैं, सर्वज्ञता व्यवहारनयसे है यह नहीं बतला रहे है।
यहाँ पर अपर पक्षने जो यह लिखा है कि 'स्त्र में परका और परम स्वका अत्यन्ताभाव है।' इसे पढ़कर हमें प्रसन्नता हुई। यह अकाट्य निगम है जो ज्ञ य-ज्ञायकभाव और कार्य-कारणभाव सबपर लाग होता है। इसका आशय यह है कि ज्ञेय ज्ञानको उत्पन्न करता नहीं, फिर भी शेयकी अपेक्षा किये विना ज्ञान का ऐसा परिणाम होता है जिसमें ज्ञेय ज्ञात हो जाते है। इसी प्रकार उम्मकार मिट्टी में कुछ भी व्यापार करता नहीं, फिर भी कुम्भकारके व्यापारको अपेक्षा किये बिना मिट्टी स्वयं ऐसा परिणाम करती है कि घट बन जाता है ।
इस निश्चय पक्षको ठीक तरहसे समझा वही एकका दूसरे में अत्यन्ताभावको समठा सकता है और तभी व्यवहार पक्ष क्या है यह भी ध्यानमें आता है ।।
१०. हमने लिखा था कि 'ज्ञानका ज्ञाकार परिणमन शेयोंके कारण हुआ है तब वह व्यवहार कहलाता है, क्योंकि ऐसे कथनमें वस्तुको स्वभावभूत योग्यताको गौणकर उसका पराश्रित कथन किया गया है।'
इस वचन में यद्यपिटीका लायक कोई बात तो नहीं है। फिर भी अपर पशन सर्व प्रथम 'सयाकार परिणमन' इस पदको अपनी बाकाका विषय बनाया है । जब कि अपर पक्ष यह जानता है कि आगममें ज्ञेयको जाननेके अर्थ में ऐसा प्रयोग होता है। यथा-अथवा चैतन्यशक्तावाकारी-ज्ञानाकारी ज्ञयाकारश्च । तत्त्वार्थवातिक अ.१ स०६। एवमात्माऽश्चिान्योन्यवृत्तिसन्तरेणापि विश्वयाकारग्रहणसमणप्रषणाः । प्रवचनसार गा०२८ सूरकृति टोका।
इतनपर भी जब कि इसकी चरचा नं०७ में की जा चुकी थो तो पुन: इस चरचाको उठाना कहाँ तक उपयुक्त है इसका वह स्वयं विचार करे ।
हमने लिखा है कि 'ज्ञानका याकार परिणमन झयों के कारण हुआ है तब वह व्यवहार कथन है।' आदि । सो यह उचित हो लिखा है, क्योंकि ज्ञ याके कारण आत्माज्ञ योंको जानता है ऐसी जो धारणा बनो हुई है उसका परिहार करना इसका यख्य प्रयोजन है। ज्ञान में सब ज्ञात होते हैं यह बावहार नहीं है, यह तो ज्ञानपरिणामका स्वरूपाख्यान है। जबतक इरामें परकी अपेक्षा नहीं लगाई जायगो तबतक इसे व्यवहार कथन मानना उचित नहीं है । भगवान् सबको जानते हैं, इसलिए उन्हें सर्वगत कहना एक तो यह व्यवहार है और