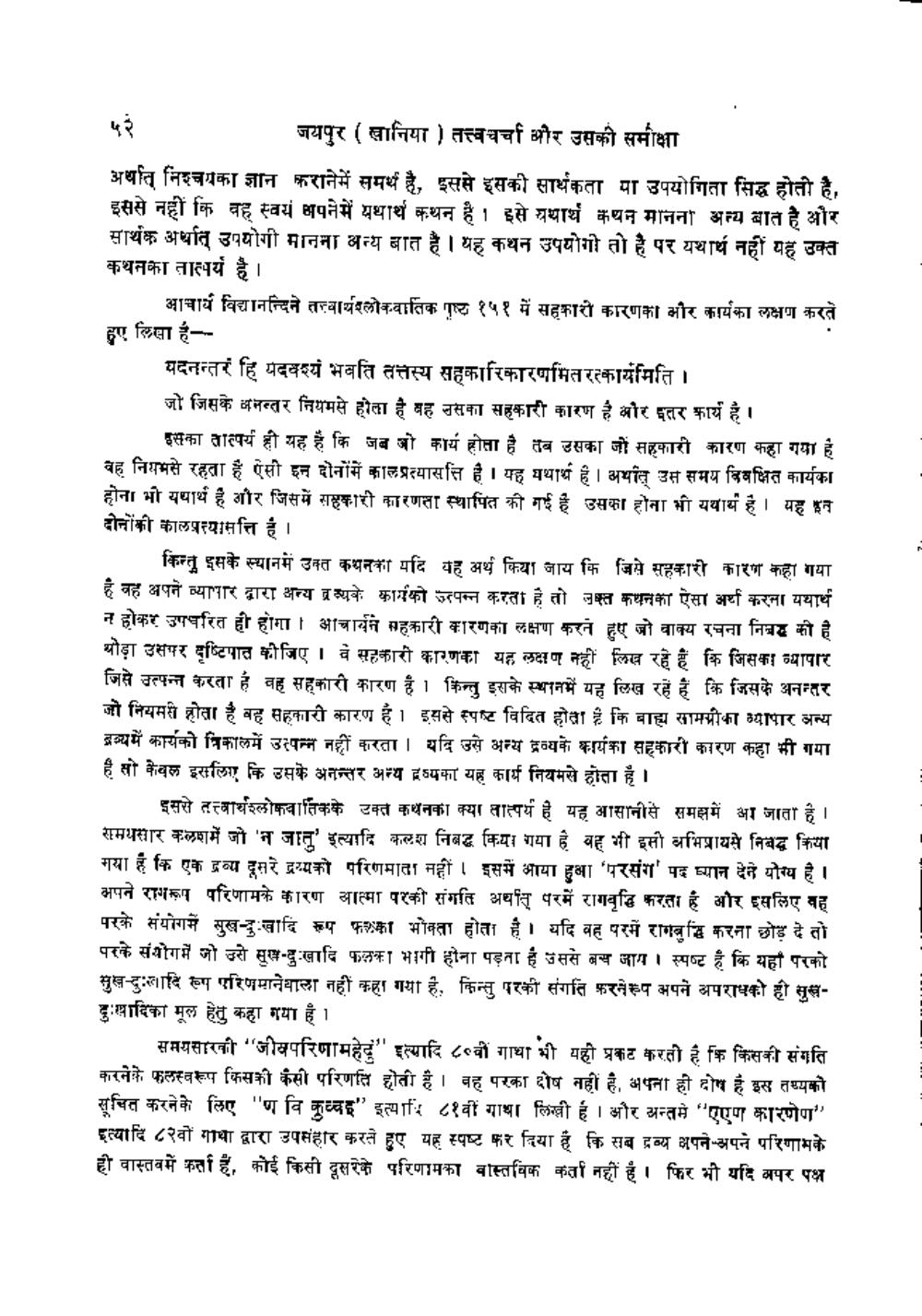________________
५२
जयपुर ( खानिया ) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा
अर्थात् निश्चयका ज्ञान करानेमें समर्थ है, इससे इसकी सार्थकता या उपयोगिता सिद्ध होती है, इससे नहीं कि वह स्वयं अपने में यथार्थ कथन हैं। इसे यथार्थं कथन मानना अन्य बात है और सार्थक अर्थात् उपयोगी मानना अन्य बात है । यह कथन उपयोगी तो है पर यथार्थ नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।
आचार्य विद्यानन्दिने तत्त्वार्थश्लोकवातिक पृष्ठ १५१ में सहकारी कारणका और कार्यका लक्षण करते लिसा है-
हुए
यदनन्तरं हि यदवश्यं भवति तत्तस्य सहकारिकारणमितरत्कार्यमिति ।
जो जिसके अनन्तर नियमसे होता है वह उसका सहकारी कारण है और इतर कार्य है ।
इसका तात्पर्य ही यह है कि जब जो कार्य होता है तब उसका जो सहकारी कारण कहा गया है। वह नियमसे रहता हैं ऐसी इन दोनों में कालप्रत्यासत्ति है । यह यथार्थ है । अर्थात् उस समय विवक्षित कार्यका होना भी यथार्थ है और जिसमें सहकारी कारणता स्थापित की गई है उसका होना भी यथार्थ है । यह ह दोनोंकी कालप्रत्यासत्ति हूँ ।
किन्तु इसके स्थान में उक्त कथनका यदि यह अर्थ किया जाय कि जिसे सहकारी कारण कहा गया है वह अपने व्यापार द्वारा अन्य द्रव्यके कार्यको उत्पन्न करता है तो उक्त कथनका ऐसा अर्थ करना यथार्थ न होकर उपचारित ही होगा। आचार्यने सहकारी कारणका लक्षण करते हुए जो वाक्य रचना निबद्ध की है थोड़ा उसपर दृष्टिपात कीजिए। वे सहकारी कारणका यह लक्षण नहीं लिख रहे हैं कि जिसका व्यापार जिसे उत्पन्न करता है वह सहकारी कारण है । किन्तु इसके स्थान में यह लिख रहें हैं कि जिसके अनन्तर जो नियम होता है वह सहकारी कारण है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि बाह्य सामग्रीका व्यापार अन्य ब्रव्य में कार्यको त्रिकालमें उत्पन्न नहीं करता यदि उसे अन्य द्रव्यके कार्यका सहकारी कारण कहा भी गया हैं तो केवल इसलिए कि उसके अनन्तर अन्य द्रव्यका यह कार्य नियमसे होता है ।
।
समझ में आ जाता है ।
इससे तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकके उक्त कथनका क्या तात्पर्य है यह आसानी से समयसार कलश में जो 'न जातु' इत्यादि कलश निबद्ध किया गया है वह भी इसी अभिप्रायसे निवद्ध किया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रयमको परिणमाता नहीं। इसमें आया हुआ 'परसंग' पद ध्यान देने योग्य है । अपने रामरूप परिणामके कारण आत्मा परकी संगति अर्थात् परमें रागवृद्धि करता है और इसलिए वह परके संयोग में सुख-दुःखादि रूप फरक्का भोक्ता होता है। यदि वह परमें रामबुद्धि करना छोड़ दे तो परके संयोग में जो उसे सुख-दुःखादि फलका भागी होना पड़ता है उससे अन्य जाय । स्पष्ट है कि यहाँ परको सुख-दुःखादि रूप परिणमानेवाला नहीं कहा गया है, किन्तु परकी संगति करनेरूप अपने अपराधको ही सुखदुःखादिका मूल हेतु कहा गया है ।
समयसारको “जीवपरिणामहेदु" इत्यादि ८०वी गाथा भी यही प्रकट करती है कि किसकी संगति करने के फलस्वरूप किसकी कैसी परिणति होती है। वह परका दोष नहीं है, अपना ही दोष है इस तथ्यको सूचित करने के लिए "ण वि कुध्वद्द" इत्यादि ८१वीं गाथा लिखी है । और अन्त में "एएण कारणेण " इत्यादि ८२वीं गाथा द्वारा उपसंहार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सब द्रव्य अपने-अपने परिणाम के ही वास्तव में कर्ता हैं, कोई किसी दूसरेके परिणामका वास्तविक कर्ता नहीं है । फिर भी यदि अपर पक्ष