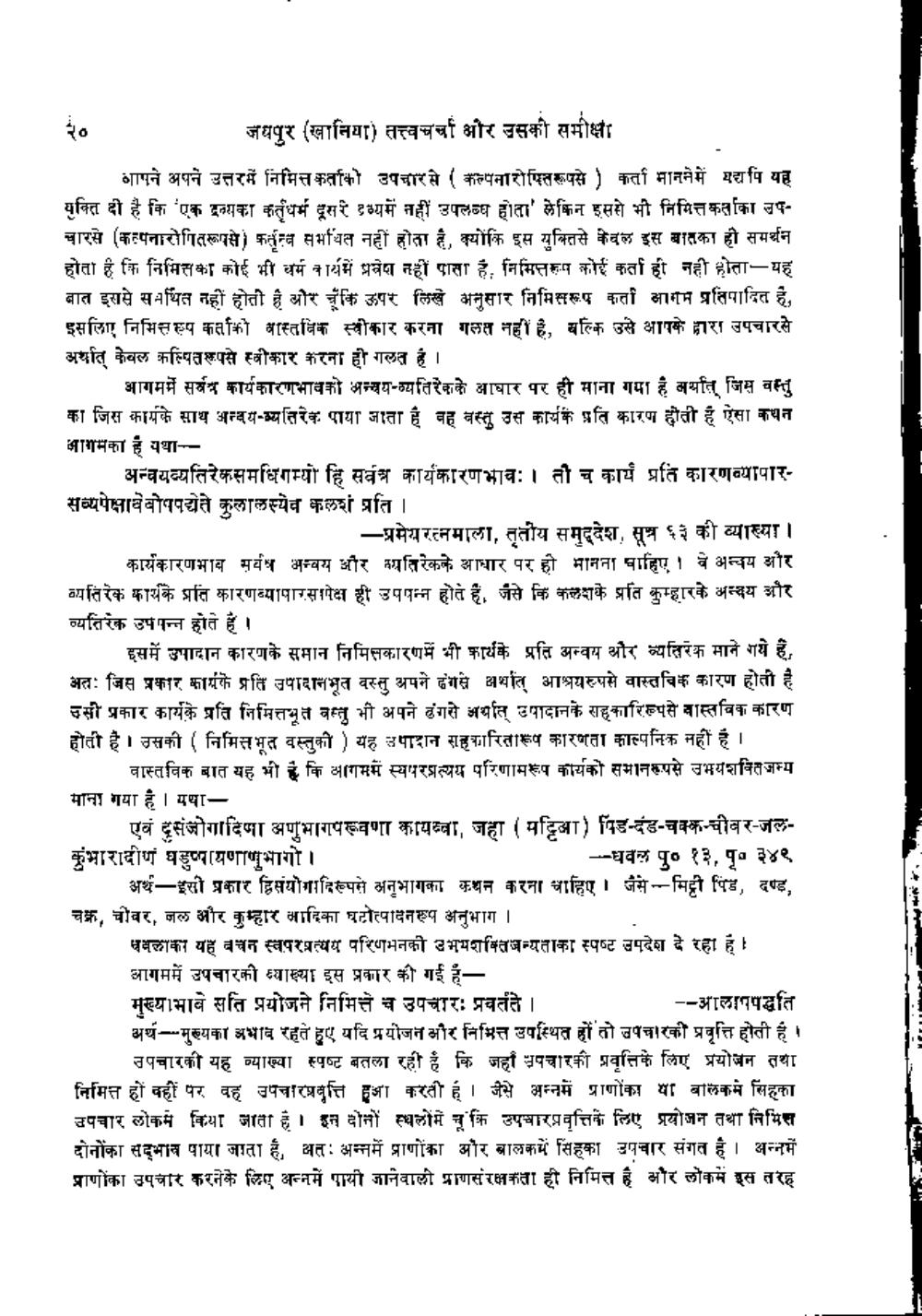________________
जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा
मापने अपने उत्तरमें निमित्त कर्ताको उपचार से ( कल्पनारोपितरूपसे ) कर्ता मानने में यद्यपि यह युक्ति दी है कि एक इन्यका कर्तृधर्म दूसरे ४ध्यमें नहीं उपलब्ध होता' लेकिन इससे भी निमित्त कर्ताका उपचारसे (कल्पनारोगितरूपसे) कर्तृत्व सथित नहीं होता है, क्योंकि इस युक्तिसे केवल इस बातका ही समर्थन होता है कि निमित्तका कोई भी धर्म वायमें प्रवेश नहीं पाता है. निमित्तरूप कोई कर्ता ही नहीं होता-यह बात इससे समर्थित नहीं होती है और कि ऊपर लिखे अनुसार निमिसरूप कर्ता आगम प्रतिपादित है, इसलिए निमित्स रूप कर्ताको वास्तविक स्वीकार करना गलत नहीं है, बल्कि उसे आपके द्वारा उपचारसे अर्थात् केवल कल्पितरूपसे स्वीकार करना ही गलत है।
आगममें सर्वत्र कार्यकारणभावको अन्यय-व्यतिरेक के आधार पर ही माना गया है अर्थात् जिस वस्तु का जिस कार्यके साथ अन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है वह वस्तु उस कार्य के प्रति कारण होती है ऐसा कथन आगमका है यथा
अन्वयन्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभावः । ती च कार्य प्रति कारणव्यापारसध्यपेक्षावेवोपपद्यते कुलालस्येव कलशं प्रति ।
-प्रमेयरत्नमाला, तृतीय समुदेश, सूत्र ६३ की व्याख्या । कार्यकारणभाव सर्वध अन्वय और व्यतिरेकके आधार पर ही मानना चाहिए। वे अन्चय और व्यतिरेक कार्य के प्रति कारणब्यापारसापेक्ष ही उपपन्न होते हैं, जैसे कि कलशके प्रति कुम्हारके अन्वय और व्यतिरेक उपपन्न होते है।
___ इसमें उपादान कारणके समान निमिसकारणमें भी कार्य के प्रति अन्वय और व्यतिरेक माने गये हैं, अत: जिस प्रकार कार्यके प्रति उपादानभूत वस्तु अपने द्वेगसे अर्थात् आश्रयरूपसे वास्तविक कारण होती है उसी प्रकार कार्यके प्रति निमित्तभत वस्तु भी अपने ढंगसे अर्थात उपादानके सहकारिरूपसे वास्तविक कारण होती है। उसकी ( निमित्तभूत वस्तुकी ) यह उपादान सहकारितारूप कारणता काल्पनिक नहीं है ।
वास्तविक बात यह भी है कि आगममें स्यपरप्रत्यय परिणामरूप कार्यको समानरूपसे उभयशक्तिजन्य माना गया है । यथा
एवं दुसंजोगादिणा अणुभागपरूवणा कायम्बा, जहा ( मट्टिआ) पिंड-दंड-चक्क-चीवर-जलकुंभारादीणं धडप्पायणाणुभागो।
---धवल पु० १३, पृ० ३४९ अर्थ-इसी प्रकार हिसंयोगादिरूपसे अनुभागका कथन करना चाहिए । जैसे-मिट्टी पिड, दण्ड, चक्र, चीवर, जल और कुम्हार आदिका घटोत्पादनरूप अनुभाग ।
धवलाका यह वचन स्वपरप्रत्यय परिणभनकी उभयक्तिजन्यताका स्पष्ट उपदेश दे रहा है। आगममें उपचारकी व्याख्या इस प्रकार की गई हैमुख्याभाबे सति प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रवर्तते ।
--आलापपद्धति अर्थ--मुख्यका अभाव रहते हुए यदि प्रयोजन और निमित्त उपस्थित हों तो उपचारकी प्रवृत्ति होती है।
उपचारकी यह व्याख्या स्पष्ट बतला रही है कि जहाँ अपचारकी प्रवृत्तिके लिए प्रयोजन तथा निमित्त हों वहीं पर वह उपचारप्रवृत्ति हुआ करती है। जैसे अन्नमें प्राणोंका या बालकम सिंहका उपचार लोकम किया जाता है। इन दोनों स्थलोंमें चूकि उपचारप्रवृत्ति के लिए प्रयोजन तथा निमित्त दोनोंका सद्भाव पाया जाता है, अतः अन्नमें प्राणोंका और बालकमें सिंहका उपचार संगत है। अन्नमें प्राणोंका उपचार करने के लिए अन्नमें पायी जानेवाली प्राणसंरक्षकता ही निमित्त है और लोकमें इस तरह