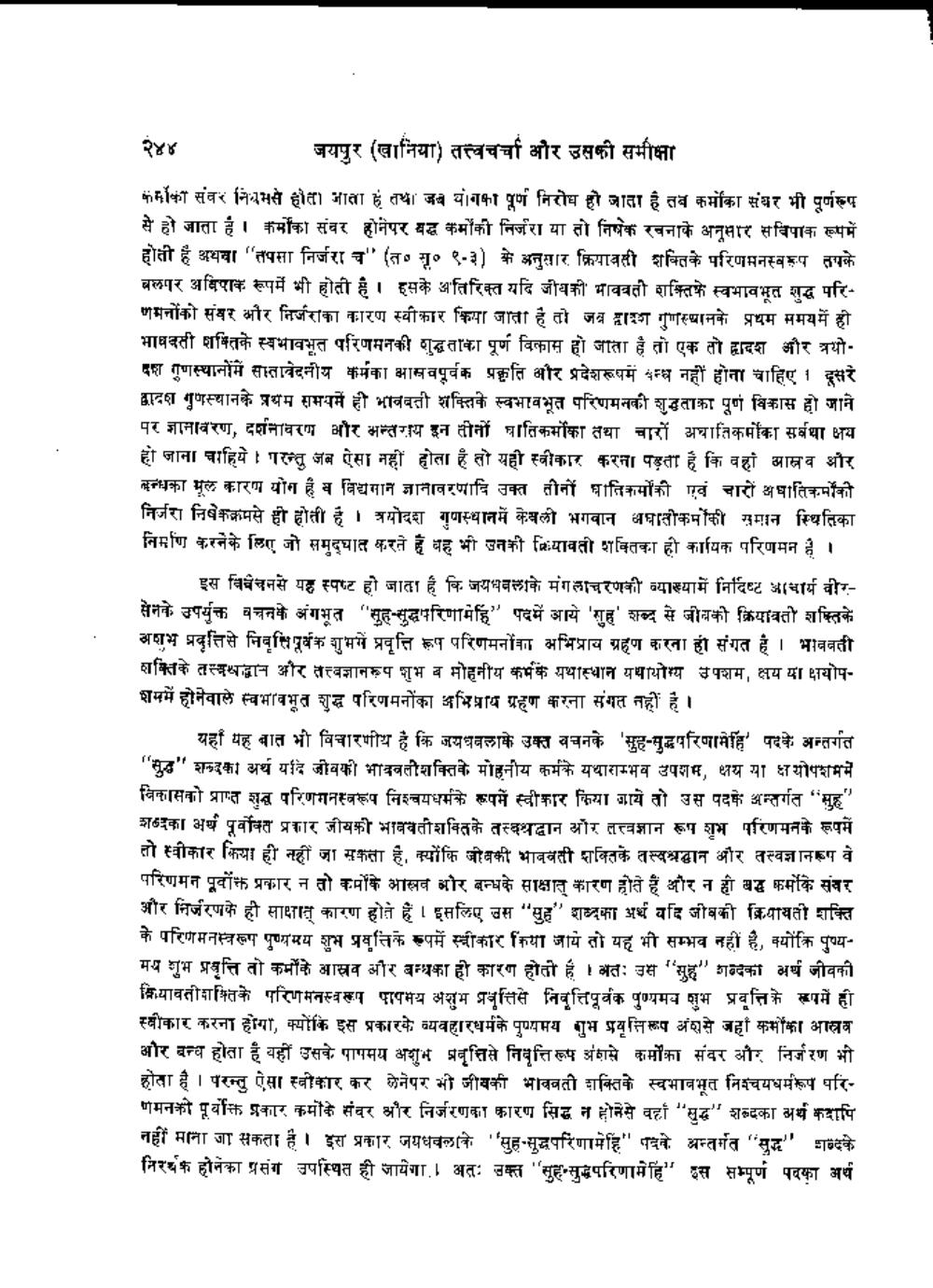________________
२४४
जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा
काका संवर नियमसे होता जाता है तथा जब योगका पूर्ण निरोध हो जाता है तब कर्मोंका संघर भी पूर्णरूप से हो जाता है। कर्मोका संबर होनेपर बद्ध कर्मोंकी निर्जरा या तो निषेक रचनाके अनुसार सविपाक रूपमें होती है अथवा "तपसा निर्जरा च" (त गृ० ९.३) के अनुसार क्रियावसी शक्तिके परिणमनस्वरूप तपके बलपर अविपाक रूपमें भी होती है। इसके अतिरिक्त यदि जीयकी भाववती शक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमनोंको संवर और निर्जराका कारण स्वीकार किया जाता है तो जब द्वादश गुणस्थानके प्रथम ममय में ही भाषवती शक्तिके स्वभावभूत परिणमनकी शुद्धताका पूर्ण विकास हो जाता है तो एक तो द्वादश और त्रयोदश गुणस्थानोंमें सातावेदनीय कर्मका आसवपूर्वक प्रकृति और प्रदेशरूपम बन्ध नहीं होना चाहिए 1 दूसरे द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें ही भाववती शक्तिके स्वभावभूत परिणमनकी शुद्धताका पूर्ण विकास हो जाने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिकर्मोका तथा चारों अघातिकर्मोका सर्वथा अय हो जाना चाहिये । परन्तु जब ऐसा नहीं होता है तो यही स्वीकार करना पड़ता है कि वहां आस्रव और बन्धका मूल कारण योग है व विद्यमान ज्ञानावरणादि उक्त तीनों घातिकर्मोंकी एवं चारों अघातिकर्मीको निर्जरा निषेकक्रमसे ही होती है । त्रयोदश गणस्थानमें केवली भगवान अघातीकोकी समान स्थितिका निर्माण करने के लिए जो समुद्घात करते हैं वह भी उनकी कियावती शक्तिका ही कायिक परिणमन है ।
___इस विवचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जयधवलाके मंगलाचरणकी व्याख्यामें निर्दिष्ट आचार्य वीरसेनके उपर्युक्त वचन के अंगभूत "सुह-सुद्धपरिणामहि" पदमें आये 'गुह' शब्द से जीनको क्रियावती शक्तिके अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्तिपूर्वक शुभगे प्रवृत्ति रूप परिणमनोंका अभिप्राय ग्रहण करना ही संगत है । भाववती शक्तिके तत्ववद्वान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ ब मोहनीय कर्मक यथास्थान यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाले स्वभावभूत शुद्ध परिणमनोंका अभिप्राय ग्रहण करना संगत नहीं है।
___ यहाँ यह बात भी विचारणीय है कि जयधवलाके उक्त वचनके 'सुह-सुद्धपरिणामेहि' पदके अन्तर्गत "सुद्ध" शब्दका अर्थ यदि जीवको भाववलीशक्तिके मोहनीय कर्मके यथाराम्भव उपशम, क्षय या क्षयोपशम में
को प्राप्त शत परिणगनस्वरूप निश्चयधर्मके रूपमें स्वीकार किया जाये तो उस पदके अन्तर्गत "सह" शब्दका अर्थ पूर्वोक्त प्रकार जीयको भाववतीशक्तिके तस्वयद्वान और लत्त्वज्ञान रूप शुभ परिणमनके रूपमें तो स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जीवकी भाववती शक्तिके तस्वश्रद्वान और तत्वज्ञानरूप वे परिणमन पूर्वोक्त प्रकार न तो कोंके आस्त्रव और बन्धके साक्षात कारण होते हैं और न ही बद्ध कर्मोक संवर और निर्जरणके ही साक्षात् कारण होते हैं। इसलिए उस "सुह' शब्दका अर्थ यदि जीवकी क्रियायती शक्ति के परिणमनस्वरूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिकै रूपमें स्वीकार किया जाये तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति तो कमोंके आस्रव और बन्धका ही कारण होती है । अतः उस "सुह" शब्दका अर्थ जीवकी कियावतीयाक्तिके परिणमनस्वरूप पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति के रूपमें ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस प्रकारके व्यवहारधर्मके पुण्यमय गुभ प्रवृत्तिरूप अंशसे जहाँ कर्मोका आस्रव
और बन्य होता है वहीं उसके पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्ति रूप अंशसे कर्मोका संवर और निर्जरण भी होता है । परन्तु ऐसा स्वीकार कर लेनेपर भी जीवकी भाववती शक्तिके स्वभावभत निश्चयधर्मरूप परि
मनको पूर्वोक्त प्रकार कमौके संवर और निर्जरणका कारण सिद्ध न होनेसे वहाँ "सुद्ध" शब्दका अर्थ कदापि नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार जयधवलाके ''सुह-सुद्धपरिणामेहि" पदवे. अन्तर्गत "सुद्ध" शब्दके निरर्थक होने का प्रसंग उपस्थित ही जायेगा । अतः उक्त "सुह-सुद्धपरिणामेहि" इस सम्पूर्ण पदका अर्थ