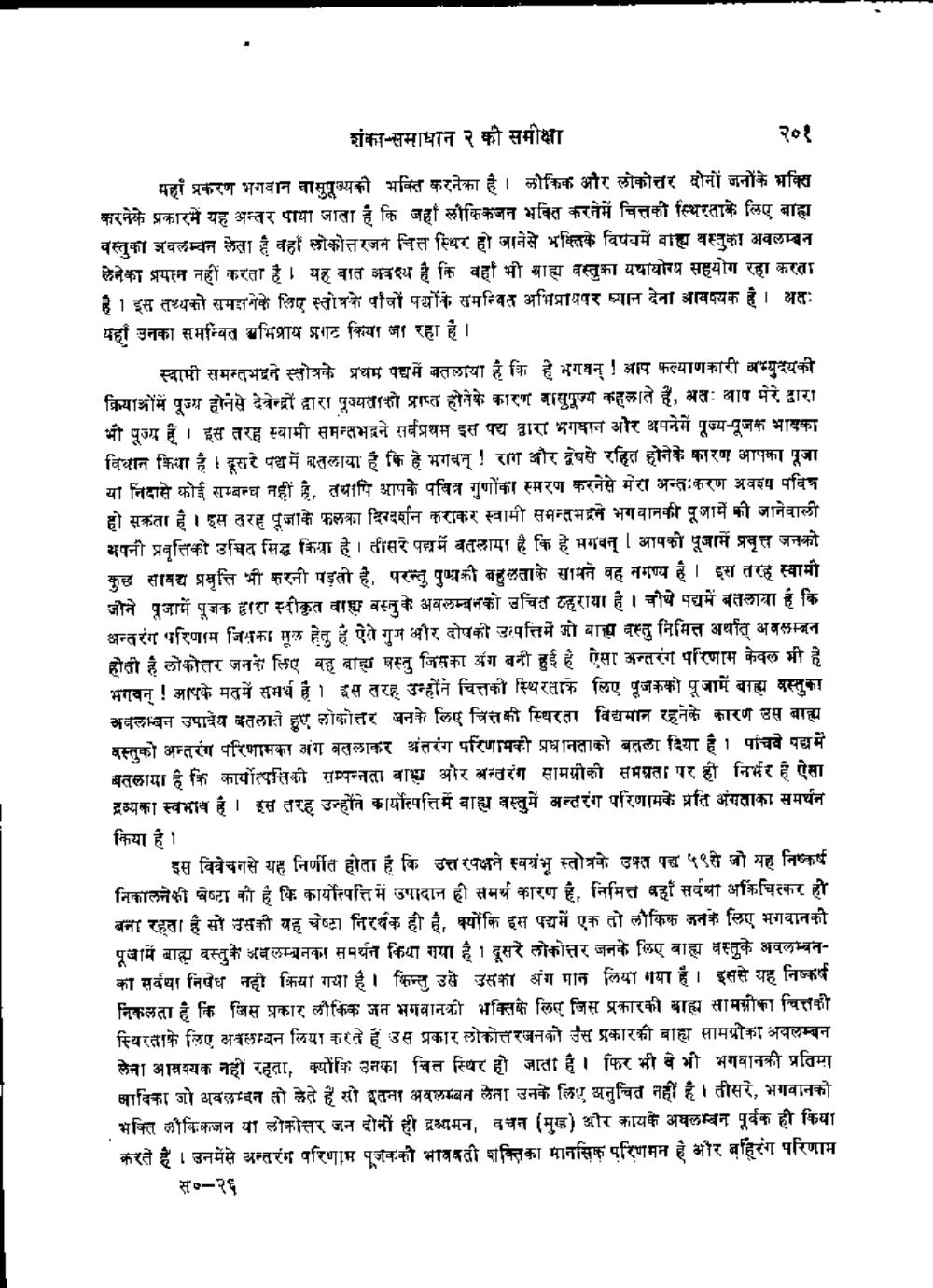________________
शंका-समाधान २ की समीक्षा
२०१
महाँ प्रकरण भगवान वासुपूज्यकी भक्ति करनेका है। लौकिक और लोकोत्तर दोनों जनोंके भक्ति करनेके प्रकारमें यह अन्तर पाया जाता है कि जहाँ लौकिकजन भक्ति करनेमें चित्तकी स्थिरताके लिए बाह्य वस्तुका अवलम्बन लेता है वहाँ लोकोत्तरजन चित्त स्थिर हो जानेसे भक्तिके विषय में बाह्य वस्तुका अवलम्बन लेनेका प्रयत्न नहीं करता है। यह बात अवश्य है कि वहाँ भी बाह्य वस्तुका यथायोग्य सहयोग रहा करता है । इस तथ्यको समझने के लिए स्तोत्रके पांचों पद्योंके समन्वित अभिप्रायपर ध्यान देना आवश्यक है। अतः यहाँ उनका समन्वित अभिप्राय प्रगट किया जा रहा है ।
स्वामी समन्तभदने स्तोत्रके प्रथम पद्य में बतलाया है कि हे भगवन् ! आप कल्याणकारी अभ्युदयकी क्रियाओंम पूज्य होनसे देवेन्द्रों द्वारा पूज्यताको प्राप्त होने के कारण वासुपूज्य कहलाते हैं, अतः आप मेरे द्वारा भी पूज्य है। इस तरह स्वामी समन्तभद्रने सर्वप्रथम इस पद्य वारा भगवान ओर अपनेमें पूज्य-पूजक भावका विधान किया है। दूसरे पक्ष में बतलाया है कि हे भगवन् ! राग और द्वेषसे रहित होने के कारण आपका पूजा या निदासे कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि आपके पवित्र गुणोंका स्मरण करनेसे मेरा अन्तःकरण अवश्य पवित्र हो सकता है । इस तरह पूजाके फलका दिग्दर्शन कराकर स्वामी समन्तभद्रने भगवान की पूजामें की जानेवाली अपनी प्रवृत्तिको उचित सिद्ध किया है। तीसरे पद्ममें बतलाया है कि हे भगवन् । आपकी पूजामें प्रवृत्त जनको कुछ सायद्य प्रवृत्ति भी करनी पड़ती है, परन्तु पुण्यकी बहुलताके सामने वह नगण्य है। इस तरह स्वामी जीने प्रजामें पुजक द्वारा स्वीकृत वा वस्तु के अवलम्बनको उचित ठहराया है। चौथे पद्यमें बतलाया है कि अन्तरंग परिणाम जिसका मूल हेतु है ऐरो गुम और दोषको उत्पत्तिमें जो बाह्य वस्तु निमित्त अर्थात् अवलम्बन होती है लोकोत्तर जनके लिए वह बाह्य पस्तु जिसका अंग बनी हुई है ऐसा अन्तरंग परिणाम केवल भी है भगवन् ! आपके मतमें समर्थ है। इस तरह उन्होंने चित्तको स्थिरताके लिए पूजकको पुजामें बाह्य वस्तुका अवलम्बन उपादेय बतलाते हुए लोकोत्तर जनके लिए चित्त की स्थिरता विद्यमान रहने के कारण उस बाह्य वस्तुको अन्तरंग परिणामका अंग बतलाकर अंतरंग परिणामकी प्रधानताको बतला दिया है। पांचवे पद्यमें बतलाया है कि कार्योत्पत्तिको सम्पन्नता बाच और अन्तरंग सामग्रीको समग्नता पर ही निर्भर है ऐसा द्रव्यका स्वभाव है। इस तरह उन्होंने कार्योत्पत्ति में बाह्य वस्तुमें अन्तरंग परिणामके प्रति अंगताका समर्थन किया है।
इस विवेचगसे यह निर्णीत होता है कि उत्तरपक्षने स्वयंभू स्तोत्रके उक्त पद्य ५९से जो यह निष्कर्ष निकालने की बेष्टा की है कि कार्योत्पत्ति में उपादान ही समर्थ कारण है, निमित्त वहाँ सर्वथा अकिंचित्कर ही बना रहता है सो उसकी यह चेष्टा निरर्थक ही है, क्योंकि इस पद्यमें एक तो लौकिक जनके लिए भगवानको पूजामें बाह्म वस्तु के अवलम्बनका समर्थन किया गया है । दूसरे लोकोत्तर जनके लिए बाह्य वस्तुके अवलम्बनका सर्वथा निषेध नही किया गया है। किन्तु उसे उसका अंग मान लिया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार लौकिक जन भगवानकी भक्ति के लिए जिस प्रकारकी बाह्य सामग्रीका चित्तकी स्थिरताके लिए अवलम्बन लिया करते हैं उस प्रकार लोकोत्तरजनको स प्रकारको बाह्य सामग्रीका अवलम्बन लेना आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि उनका चित स्थिर हो जाता है। फिर भी वे भी भगवानकी प्रतिमा मादिका जो अवलम्बन तो लेते हैं सो इतना अवलम्बन लेना उनके लिए अनुचित नहीं है। तीसरे, भगवानको भक्ति लौकिकजन या लोकोत्तर जन दोनों ही द्रश्यमन, वचन (मुख) और कायके अवलम्बन पूर्वक ही किया करते है । उनमेंसे अन्तरंग परिणाम पूजकको भाववती शक्ति का मानसिक परिणमन है और बहिरंग परिणाम
स०-२६