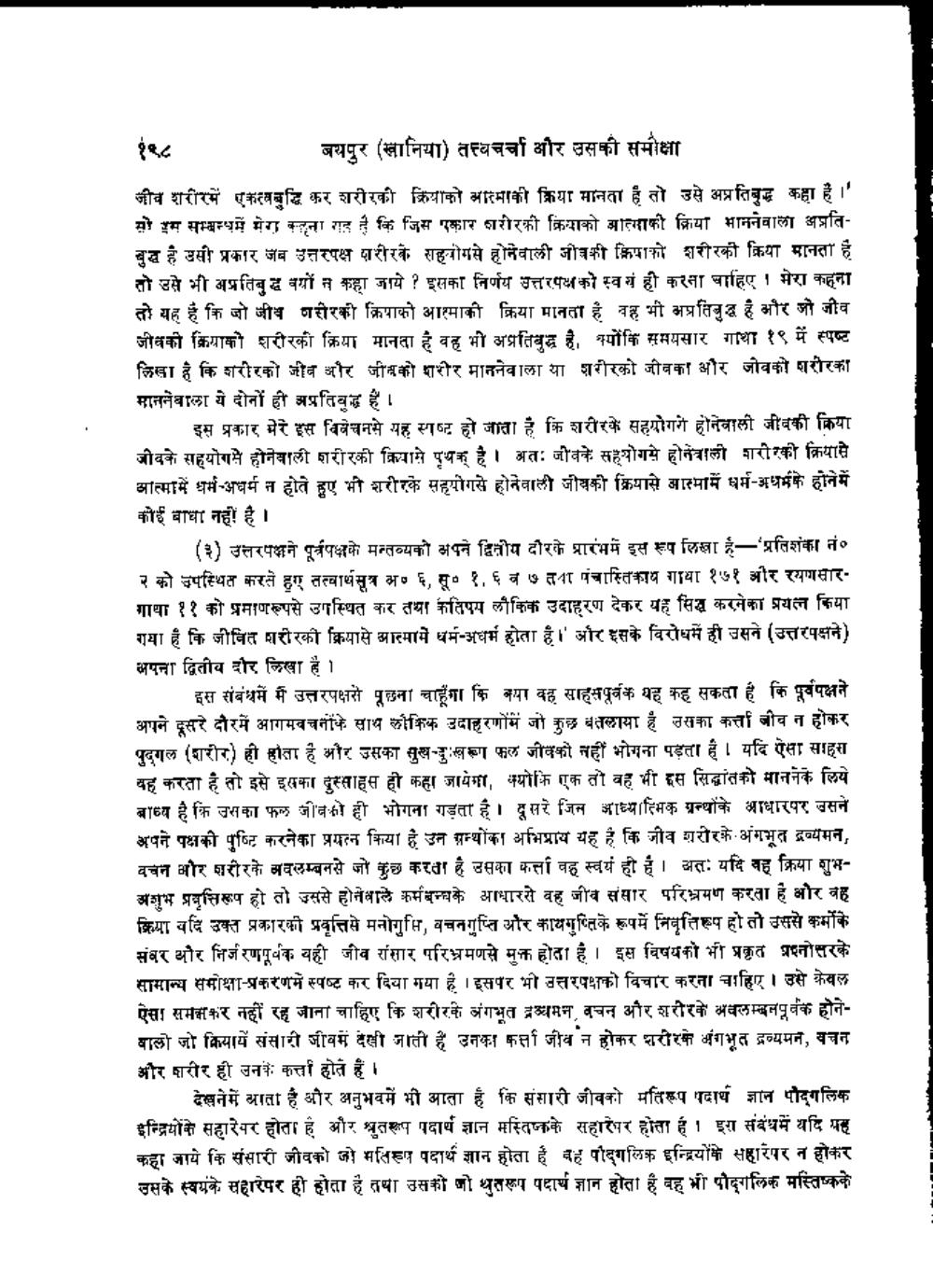________________
१९८
बयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा
जीव शरीरमें एकरवबुद्धि कर शरीरकी क्रियाको आत्माकी क्रिया मानता है तो उसे अप्रतिबुद्ध कहा है।' सो म सम्बन्धमें मेग कलना राह है कि जिस प्रकार शरीरकी क्रियाको आत्माकी क्रिया भामनेवाला अप्रतिबुद्ध है उसी प्रकार जब उत्तरपक्ष शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियाको शरीरकी क्रिया मानता है तो उसे भी अप्रतिबुद्ध क्यों न कहा जाये ? इसका निर्णय उत्तरपक्षको स्वयं ही करना चाहिए । मेरा कहना तो यह है कि जो जीव गरीरकी क्रियाको आश्माकी क्रिया मानता है वह भी अप्रतिजुद्ध है और जो जीव जीवकी क्रियाको शरीरकी क्रिया मानता है वह भी अप्रतिबद्ध है, क्योंकि समयसार गाथा १९ में स्पष्ट लिखा है कि शरीरको जीव और जीवको शरीर माननेवाला या शरीरको जीवका और जीवको शरीरका माननेवाला ये दोनों ही अप्रतिवृद्ध है।
इस प्रकार मेरे इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरके सहयोगगे होनेवाली जीवकी क्रिया जीवके सहयोग से होनेवाली शरीरकी क्रियामे पथक है। अतः जीवके सहयोगसे होनेवाली शारीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म-अधर्म न होते हुए भी शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियासे आस्मामें धर्म-अधर्मके होने में कोई बाधा नहीं है।
(३) उत्तरपक्षने पूर्वपक्षके मन्तव्यको अपने द्वितीय दौरके प्रारंभमें इस रूप लिखा है-'प्रतिशंका नं० २ को उपस्थित करते हए तत्वार्थसूत्र म०६, सू० १, ६ व ७ तवा पंचास्तिकाय गाथा १७१ और रयणसारगाथा ११ को प्रमाणरूपसे उपस्थित कर तथा कतिपय लौकिक उदाहरण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयल किया गया है कि जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म-अधर्म होता है। और इसके विरोध ही उसने (उत्तरपक्षने) अपना द्वितीव दौर लिखा है।
इस संबंध में उत्तरपक्षसे पूछना चाहूँगा कि क्या वह साहसपूर्वक यह कह सकता है कि पूर्वपक्षने अपने दूसरे दौरमें आगमवचनोंके साथ लौकिक उदाहरणोंमें जो कुछ बतलाया है उसका कर्ता जीव न होकर पुद्गल (शरीर) ही होता है और उसका सुख-दुःस्वरूप फल जीवको नहीं भोगना पड़ता है। यदि ऐसा साहस यह करता है तो इसे इसका दुस्साहस ही कहा जायेगा, क्योकि एक तो वह भी इस सिद्धांतको माननेके लिये बाध्य है कि उसका फल जीवको ही भोगना गड़ता है। दूसरे जिन आध्यात्मिक ग्रन्थोंके आधारपर उसने अपने पक्षकी पुष्टि करनेका प्रयत्न किया है उन ग्रन्थोंका अभिप्राय यह है कि जीव शरीरके अंगभूत द्रव्यमन, वचन और शरीरके अवलम्बनसे जो कुछ करता है उसका कर्ता वह स्वयं ही है। अतः यदि वह क्रिया शुभअशुभ प्रवृत्तिरूप हो तो उससे होनेवाले कर्मबन्धके आधारसे वह जीव संसार परिभ्रमण करता है और वह क्रिया यदि उक्त प्रकारको प्रवृत्तिसे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिके रूप निवृत्तिरूप हो तो उससे कर्मोके संबर और निर्जरणपूर्वक यही जीव रासार परिभ्रमणसे मुक्त होता है। इस विषयको भी प्रकृत प्रश्नोसरके सामान्य समोक्षा-प्रकरणमें स्पष्ट कर दिया गया है । इसपर भी उत्तरपक्षको विचार करना चाहिए। उसे केवल ऐसा समझकर नहीं रह जाना चाहिए कि शरीर के अंगभूत द्रवमन, वचन और शरीरके अवलम्बनपूर्वक होनेवालो जो क्रियायें संसारी जीवमं देखी जाती है उनका कर्ता जीव न होकर शरीरके अंगभूत द्रव्यमन, वचन और शारीर ही उनके कर्ता होते हैं।
देखने में आता है और अनभवमें भी आता है कि संसारी जीवको मतिरूप पदार्थ ज्ञान पोदगलिक इन्द्रियों के सहारेपर होता है और श्रुतरूप पदार्थ ज्ञान मस्तिष्कके सहारेपर होता है । इस संबंध यदि यह कहा जाये कि संसारी जीवको जो मतिरूप पदार्थ ज्ञान होता है वह पौदगलिक इन्द्रियोंके सहारपर न होकर उसके स्वयंके सहारेपर ही होता है तथा उसको जो थुतरूप पदार्थ ज्ञान होता है वह भी पौद्गलिक मस्तिष्कके